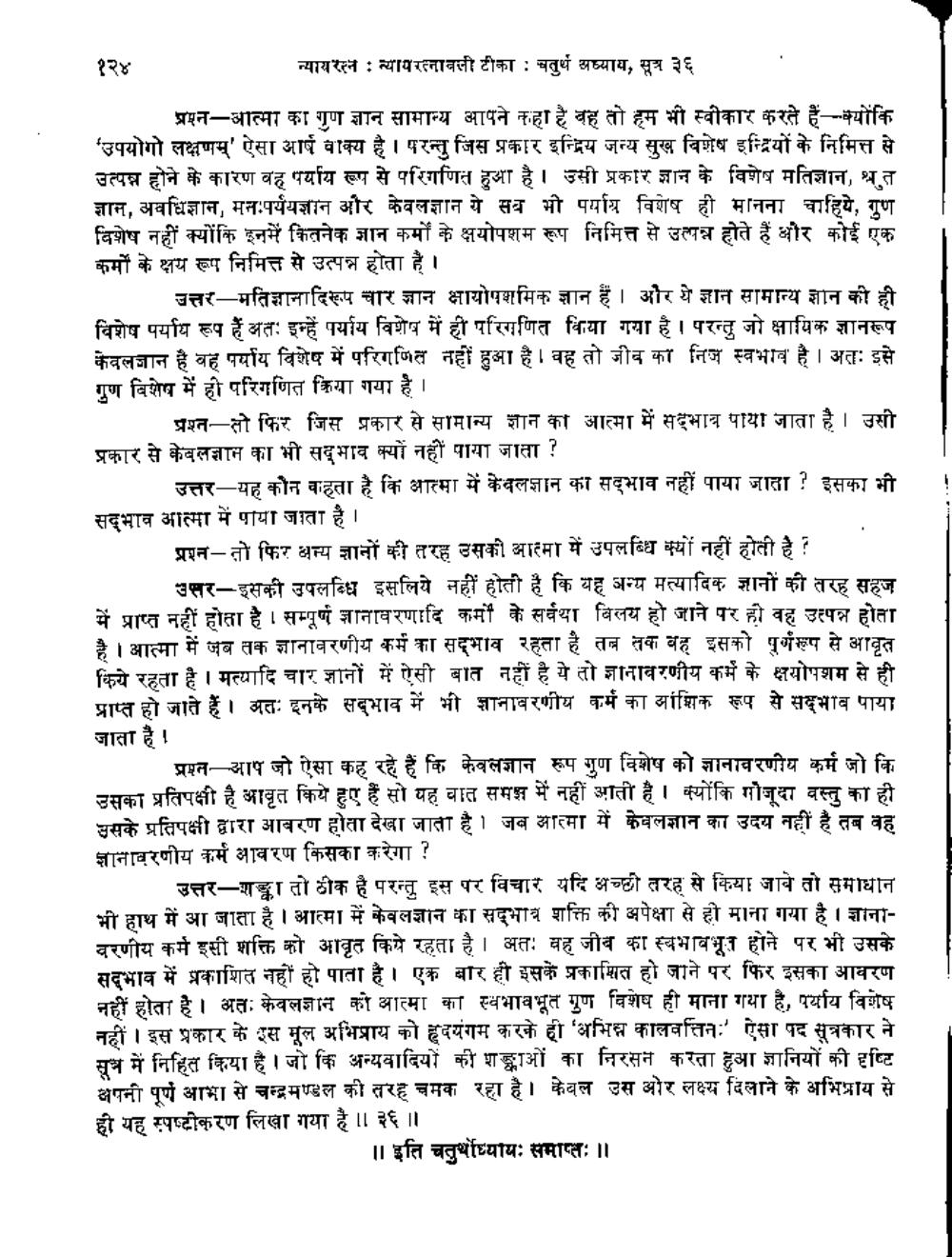________________
१२४
न्यायरत्न :न्यायरत्नावली टीका : चतुर्थ अध्याय, सूत्र ३६
प्रश्न-आत्मा का गुण ज्ञान सामान्य आपने कहा है वह तो हम भी स्वीकार करते हैं क्योंकि 'उपयोगो लक्षणम्' ऐसा आर्ष वाक्य है । परन्तु जिस प्रकार इन्द्रिय जन्य सुख विशेष इन्द्रियों के निमित्त से उत्पन्न होने के कारण वह पर्याय रूप से परिगणित हुआ है। उसी प्रकार ज्ञान के विशेष मतिज्ञान, श्रत ज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान ये सब भी पर्याय विशेष ही मानना चाहिये, गुण विशेष नहीं क्योंकि इनमें कितनेक ज्ञान कर्मों के क्षयोपशम रूप निमित्त से उत्पन्न होते हैं और कोई एक कर्मों के क्षय रूप निमित्त से उत्पन्न होता है।
उत्तर–मतिज्ञानादिरूप चार ज्ञान क्षायोपशामिक ज्ञान हैं। और ये ज्ञान सामान्य ज्ञान की ही विशेष पर्याय रूप हैं अतः इन्हें पर्याय विशेष में ही परिगणित दिया गया है । परन्तु जो क्षायिक ज्ञानरूप केवलज्ञान है वह पर्याय विशेष में परिगणित नहीं हुआ है । वह तो जीव का निज स्वभाव है । अतः इसे गुण विशेष में ही परिगणित किया गया है।
प्रश्न-तो फिर जिस प्रकार से सामान्य ज्ञान का आत्मा में सदभाब पाया जाता है। उसी प्रकार से केवलज्ञान का भी सद्भाव क्यों नहीं पाया जाता ?
उत्तर-यह कौन वाहता है कि आत्मा में केवलज्ञान का सद्भाव नहीं पाया जाता? इसका भी सद्भाव आत्मा में पाया जाता है
प्रश्न- तो फिर अन्य ज्ञानों की तरह उसको आत्मा में उपलब्धि क्यों नहीं होती है ?
उसर-इसकी उपलब्धि इसलिये नहीं होती है कि यह अन्य मत्यादिक ज्ञानों की तरह सहज में प्राप्त नहीं होता है । सम्पूर्ण ज्ञानावरणादि कर्मों के सर्वथा बिलय हो जाने पर ही वह उत्पन्न होता है । आत्मा में जब तक ज्ञानावरणीय कर्म का सद्भाव रहता है तब तक वह इसको पुर्णरूप से आवृत किये रहता है । मत्यादि चार ज्ञानों में ऐसी बात नहीं है ये तो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः इनके सद्भाव में भी ज्ञानावरणीय कर्म का आंशिक रूप से सद्भाब पाया जाता है।
प्रश्न—आप जो ऐसा कह रहे हैं कि केवलज्ञान रूप गुण विशेष को ज्ञानावरणीय कर्म जो कि उसका प्रतिपक्षी है आवृत किये हुए हैं सो यह बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि मौजूदा वस्तु का ही उसके प्रतिपक्षी द्वारा आवरण होता देखा जाता है। जब आत्मा में केवलज्ञान का उदय नहीं है तब वह ज्ञानावरणीय कर्म आवरण किसका करेगा?
उत्तर-शङ्का तो ठीक है परन्तु इस पर विचार यदि अच्छी तरह से किया जाये तो समाधान भी हाथ में आ जाता है । आत्मा में केवलज्ञान का सद्भाव शक्ति की अपेक्षा से ही माना गया है । ज्ञानावरणीय कर्म इसी शक्ति को आवृत किये रहता है। अतः वह जीव का स्वभावभूत होने पर भी उसके सद्भाव में प्रकाशित नहीं हो पाता है। एक बार ही इसके प्रकाशित हो जाने पर फिर इसका आवरण नहीं होता है। अतः केवलज्ञान को आत्मा का स्वभावभूत गुण विशेष ही माना गया है, पर्याय विशेष नहीं । इस प्रकार के इस मूल अभिप्राय को हृदयंगम करके ही 'अभिन्न कालवत्तिनः' ऐसा पद सूत्रकार ने सूत्र में निहित किया है । जो कि अन्यवादियों की शङ्काओं का निरसन करता हुआ ज्ञानियों की दृष्टि अपनी पूर्ण आभा से चन्द्रमण्डल की तरह चमक रहा है। केवल उस ओर लक्ष्य दिलाने के अभिप्राय से ही यह स्पष्टीकरण लिखा गया है ।। ३६ ।।।
॥ इति चतुर्योध्यायः समाप्तः ॥