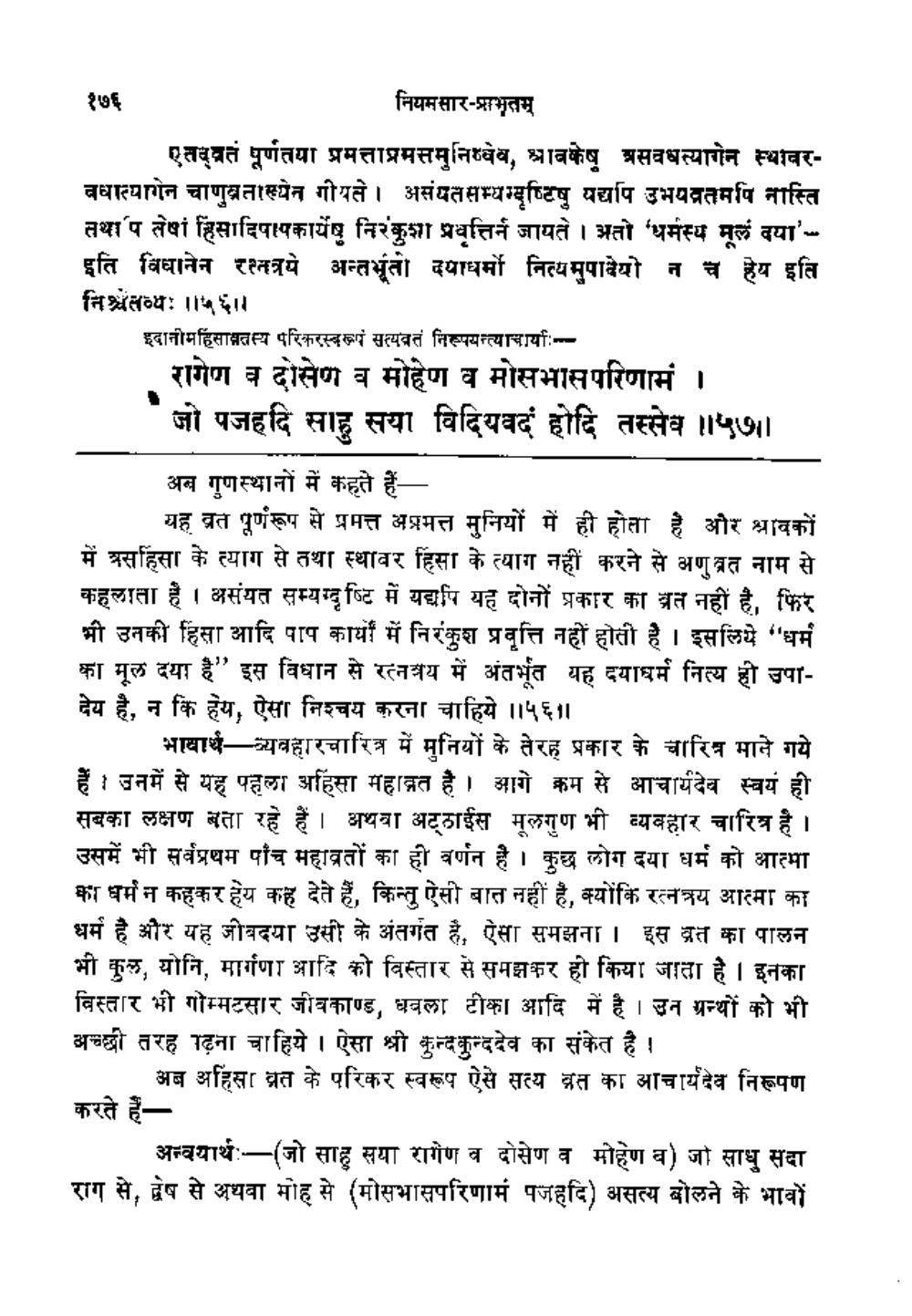________________
१७६
नियमसार-प्राभृतम् एतव्रतं पूर्णतया प्रमत्ताप्रमसमुनिश्वेव, श्रावकेषु प्रसवधत्यागेन स्थावरवधात्यागेन चाणुव्रतास्येन गीयते। असंयतसम्यग्दृष्टिषु यद्यपि उभयव्रतमपि नास्ति तथा प तेषां हिंसादिपापकार्येषु निरंकुशा प्रवत्तिर्न जायते । अतो 'धर्मस्य मूलं वया'-- इति विधानेन रत्नत्रये अन्तर्भूती दयाधर्मो नित्यमुपादेयो न च हेय इति निश्वेतव्यः ।।५।।
इदानीमहिंसानतस्य परिकरस्वरूप सत्यवतं निरूपयन्त्याचार्या:-- रागेण व दोसेण व मोहेण व मोसभासपरिणामं । जो पजहदि साहु सया विदियवदं होदि तस्सेव ॥५७।।
अब गुणस्थानों में कहते हैं
यह व्रत पूर्ण रूप से प्रमत्त अप्रमत्त मुनियों में ही होता है और श्रावकों में असहिंसा के त्याग से तथा स्थावर हिंसा के त्याग नहीं करने से अणुव्रत नाम से कहलाता है । असंयत सम्यग्दृष्टि में यद्यपि यह दोनों प्रकार का व्रत नहीं है, फिर भी उनकी हिंसा आदि पाप कार्यों में निरंकुश प्रवृत्ति नहीं होती है । इसलिये "धर्म का मूल दया है" इस विधान से रत्नत्रय में अंतर्भूत यह दयाधर्म नित्य ही उपादेय है, न कि हेय, ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥५६॥
भावार्थ-व्यवहारचारित्र में मुनियों के तेरह प्रकार के चारित्र माने गये हैं। उनमें से यह पहला अहिंसा महावत है। आगे क्रम से आचार्यदेव स्वयं ही सबका लक्षण बता रहे हैं। अथवा अट्ठाईस मूलगुण भी व्यवहार चारित्र है । उसमें भी सर्वप्रथम पाँच महाव्रतों का ही वर्णन है। कुछ लोग दया धर्म को आत्मा का धर्म न कहकर हेय कह देते हैं, किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रत्नत्रय आत्मा का धर्म है और यह जीवदया उसी के अंतर्गत है, ऐसा समझना। इस व्रत का पालन भी कुल, योनि, मार्गणा आदि को विस्तार से समझकर ही किया जाता है | इनका विस्तार भी गोम्मटसार जीवकाण्ड, धवला टीका आदि में है । उन ग्रन्थों को भी अच्छी तरह पढ़ना चाहिये । ऐसा श्री कुन्दकुन्ददेव का संकेत है।
अब अहिंसा व्रत के परिकर स्वरूप ऐसे सत्य व्रत का आचार्य देव निरूपण करते हैं
अन्वयार्थः-(जो साहु सया रागेण व दोसेण व मोहेण ब) जो साधु सदा राग से, द्वेष से अथवा मोह से (मोसभासपरिणामं पजहदि) असत्य बोलने के भावों