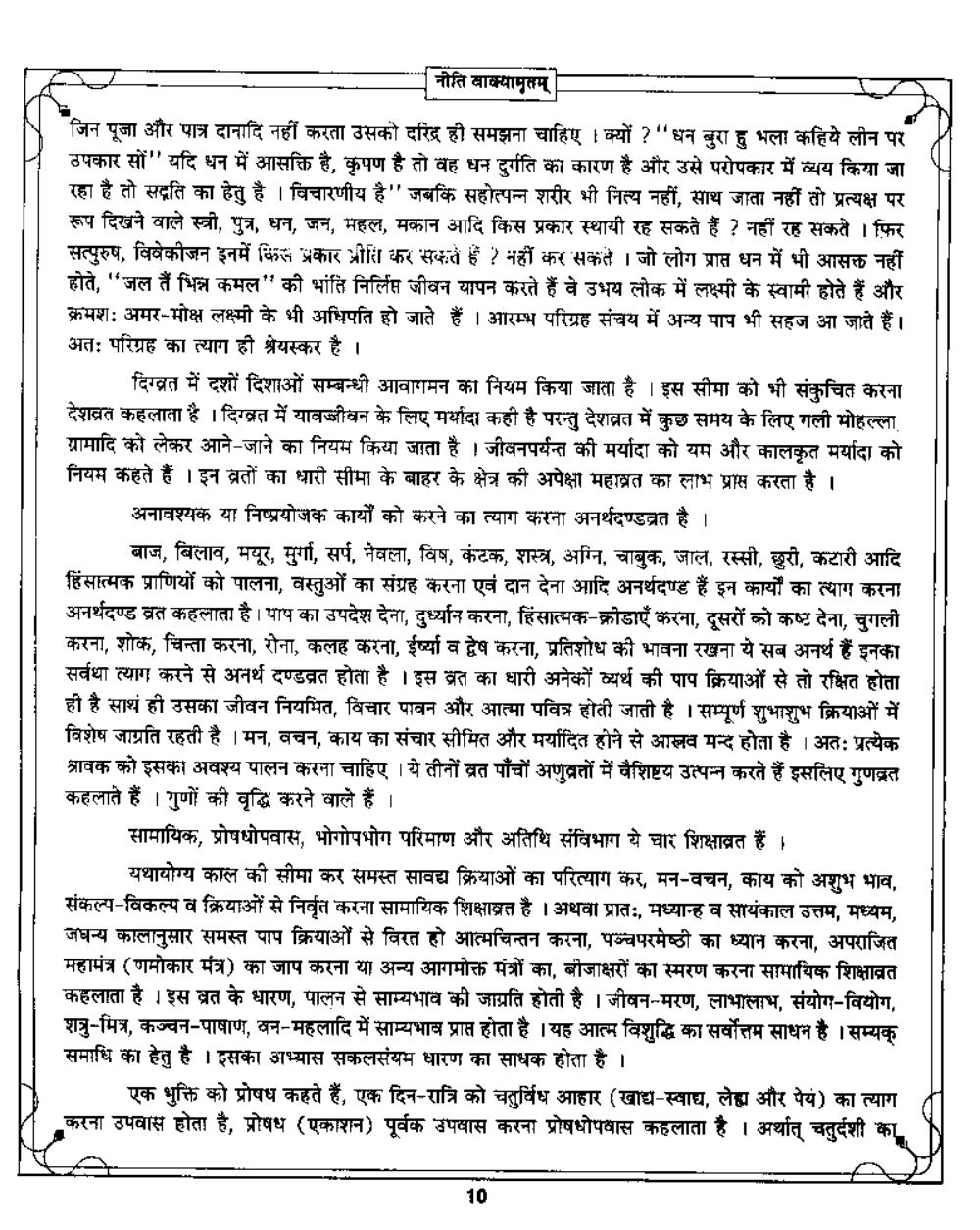________________
नीति वाक्यामृतम् जिन पूजा और पात्र दानादि नहीं करता उसको दरिद्र ही समझना चाहिए । क्यों ? "धन बुरा हु भला कहिये लीन पर उपकार सों" यदि धन में आसक्ति है, कृपण है तो वह धन दर्गति का कारण है और उसे परोपकार में व्यय किया जा रहा है तो सदति का हेतु है । विचारणीय है" जबकि सहोत्पन्न शरीर भी नित्य नहीं, साथ जाता नहीं तो प्रत्यक्ष पर रूप दिखने वाले स्त्री, पुत्र, धन, जन, महल, मकान आदि किस प्रकार स्थायी रह सकते हैं ? नहीं रह सकते । फिर सत्पुरुष, विवेकीजन इनमें किस प्रकार प्रीति कर सकते हैं? नहीं कर सकते । जो लोग प्राप्त धन में भी आसक्त नहीं होते, "जल रौं भिन्न कमल" की भांति निर्लिप्त जीवन यापन करते हैं वे उभय लोक में लक्ष्मी के स्वामी होते हैं और क्रमशः अमर-मोक्ष लक्ष्मी के भी अधिपति हो जाते हैं । आरम्भ परिग्रह संचय में अन्य पाप भी सहज आ जाते हैं। अतः परिग्रह का त्याग ही श्रेयस्कर है ।
दिग्वत में दशों दिशाओं सम्बन्धी आवागमन का नियम किया जाता है । इस सीमा को भी संकुचित करना देशव्रत कहलाता है । दिग्व्रत में यावज्जीवन के लिए मर्यादा कही है परन्तु देशव्रत में कुछ समय के लिए गली मोहल्ला ग्रामादि को लेकर आने-जाने का नियम किया जाता है। जीवनपर्यन्त की मर्यादा को यम और काल नियम कहते हैं । इन व्रतों का धारी सीमा के बाहर के क्षेत्र की अपेक्षा महाव्रत का लाभ प्राप्त करता है ।
अनावश्यक या निष्प्रयोजक कार्यों को करने का त्याग करना अनर्थदण्डव्रत है ।
बाज, बिलाव, मयूर, मुर्गा, सर्प, नेवला, विष, कंटक, शस्त्र, अग्नि, चाबुक, जाल, रस्सी, छुरी, कटारी आदि हिंसात्मक प्राणियों को पालना, वस्तुओं का संग्रह करना एवं दान देना आदि अनर्थदण्ड हैं इन कार्यों का त्याग करना अनर्थदण्ड व्रत कहलाता है। पाप का उपदेश देना, दुर्ध्यान करना, हिंसात्मक-क्रीडाएँ करना, दूसरों को कष्ट देना, चुगली करना, शोक, चिन्ता करना, रोना, कलह करना, ईर्ष्या व द्वेष करना, प्रतिशोध की भावना रखना ये सब अनर्थ हैं इनका सर्वथा त्याग करने से अनर्थ दण्डव्रत होता है । इस व्रत का धारी अनेकों व्यर्थ की पाप क्रियाओं से तो रक्षित होता ही है साथ ही उसका जीवन नियमित, विचार पावन और आत्मा पवित्र होती जाती है । सम्पूर्ण शुभाशुभ क्रियाओं में विशेष जाग्रति रहती है । मन, वचन, काय का संचार सीमित और मर्यादित होने से आसव मन्द होता है । अत: प्रत्येक श्रावक को इसका अवश्य पालन करना चाहिए । ये तीनों व्रत पाँचों अणुव्रतों में वैशिष्टय उत्पन्न करते हैं इसलिए गुणव्रत कहलाते हैं । गुणों की वृद्धि करने वाले हैं ।
सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग ये चार शिक्षाव्रत हैं ।
यथायोग्य काल की सीमा कर समस्त सावध क्रियाओं का परित्याग कर, मन-वचन, काय को अशुभ भाव, संकल्प-विकल्प व क्रियाओं से निर्वत करना सामायिक शिक्षाप्रत है । अथवा प्रातः, मध्यान्ह व सायंकाल उत्तम, मध्यम, जघन्य कालानुसार समस्त पाप क्रियाओं से विरत हो आत्मचिन्तन करना, पञ्चपरमेष्ठी का ध्यान करना, अपराजित महामंत्र (णमोकार मंत्र) का जाप करना या अन्य आगमोक्त मंत्रों का, बीजाक्षरों का स्मरण करना सामायिक शिक्षाव्रत कहलाता है । इस व्रत के धारण, पालन से साम्यभाव की जाग्रति होती है । जीवन-मरण, लाभालाभ, संयोग-वियोग, शत्रु-मित्र, कञ्चन-पाषाण, वन-महलादि में साम्यभाव प्राप्त होता है । यह आत्म विशद्धि का सर्वोत्तम साधन है।सम्यक समाधि का हेतु है । इसका अभ्यास सकलसंयम धारण का साधक होता है ।
एक भुक्ति को प्रोषध कहते हैं, एक दिन-रात्रि को चतुर्विध आहार (खाध-स्वाध, लेह्य और पेय) का त्याग करना उपवास होता है, प्रोषध (एकाशन) पूर्वक उपवास करना प्रोषधोपवास कहलाता है । अर्थात् चतुर्दशी का
10