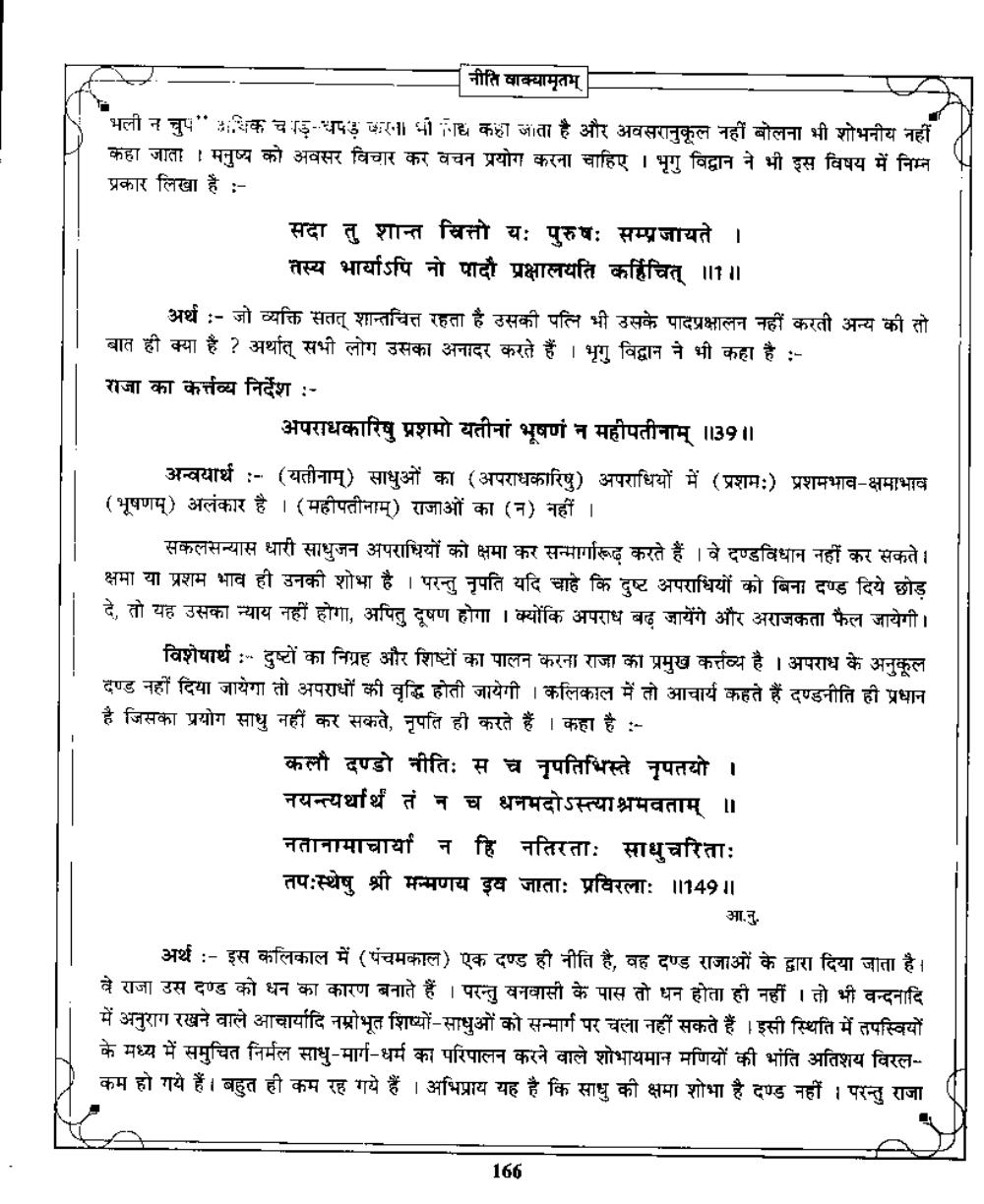________________
नीति वाक्यामृतम्
भली न चुप" अधिक चाप करना भी न कहा जाता है और अवसरानुकूल नहीं बोलना भी शोभनीय नहीं कहा जाता । मनुष्य को अवसर विचार कर वचन प्रयोग करना चाहिए । भृगु विद्वान ने भी इस विषय में निम्न प्रकार लिखा है :
सदा तु शान्त वित्तो यः पुरुषः सम्प्रजायते । तस्य भार्याऽपि नो पादौ प्रक्षालयति कर्हिचित् ॥ ॥
अर्थ :- जो व्यक्ति सतत् शान्तचित्त रहता है उसकी पत्नि भी उसके पादप्रक्षालन नहीं करती अन्य की तो बात ही क्या है ? अर्थात् सभी लोग उसका अनादर करते हैं । भृगु विद्वान ने भी कहा है :राजा का कर्त्तव्य निर्देश :
अपराधकारिषु प्रशमो यतीनां भूषणं न महीपतीनाम् ॥39॥
अन्वयार्थ :- ( यतीनाम् ) साधुओं का ( अपराधकारिषु) अपराधियों में (प्रशम : ) प्रशमभाव - क्षमाभाव (भूषणम्) अलंकार । (महीपतीनाम्) राजाओं का (न) नहीं ।
सकलसन्यास धारी साधुजन अपराधियों को क्षमा कर सन्मार्गारूढ़ करते हैं । वे दण्डविधान नहीं कर सकते। क्षमा या प्रशम भाव ही उनकी शोभा है । परन्तु नृपति यदि चाहे कि दुष्ट अपराधियों को बिना दण्ड दिये छोड़ दे, तो यह उसका न्याय नहीं होगा, अपितु दूषण होगा । क्योंकि अपराध बढ़ जायेंगे और अराजकता फैल जायेगी ।
विशेषार्थ : दुष्टों का निग्रह और शिष्टों का पालन करना राजा का प्रमुख कर्त्तव्य है । अपराध के अनुकूल दण्ड नहीं दिया जायेगा तो अपराधों की वृद्धि होती जायेगी । कलिकाल में तो आचार्य कहते हैं दण्डनीति ही प्रधान है जिसका प्रयोग साधु नहीं कर सकते, नृपति ही करते हैं । कहा है :
कलौ दण्डो नीतिः स च नृपतिभिस्ते नृपतयो । नयन्त्यर्थार्थं तं न च धनमदोऽस्त्याश्रमवताम् ॥ नतानामाचार्या न हि नतिरताः साधुचरिता: तपःस्थेषु श्री ममय इव जाताः प्रविरलाः ॥149 ॥
आ.नु.
में
अर्थ :- इस कलिकाल में (पंचमकाल ) एक दण्ड ही नीति है, वह दण्ड राजाओं के द्वारा दिया जाता है। वे राजा उस दण्ड को धन का कारण बनाते हैं। परन्तु वनवासी के पास तो धन होता ही नहीं । तो भी वन्दनादि अनुराग रखने वाले आचार्यादि नम्रोभूत शिष्यों साधुओं को सन्मार्ग पर चला नहीं सकते हैं। इसी स्थिति में तपस्वियों के मध्य में समुचित निर्मल साधु-मार्ग धर्म का परिपालन करने वाले शोभायमान मणियों की भांति अतिशय विरलकम हो गये हैं। बहुत ही कम रह गये हैं । अभिप्राय यह है कि साधु की क्षमा शोभा है दण्ड नहीं । परन्तु राजा
166