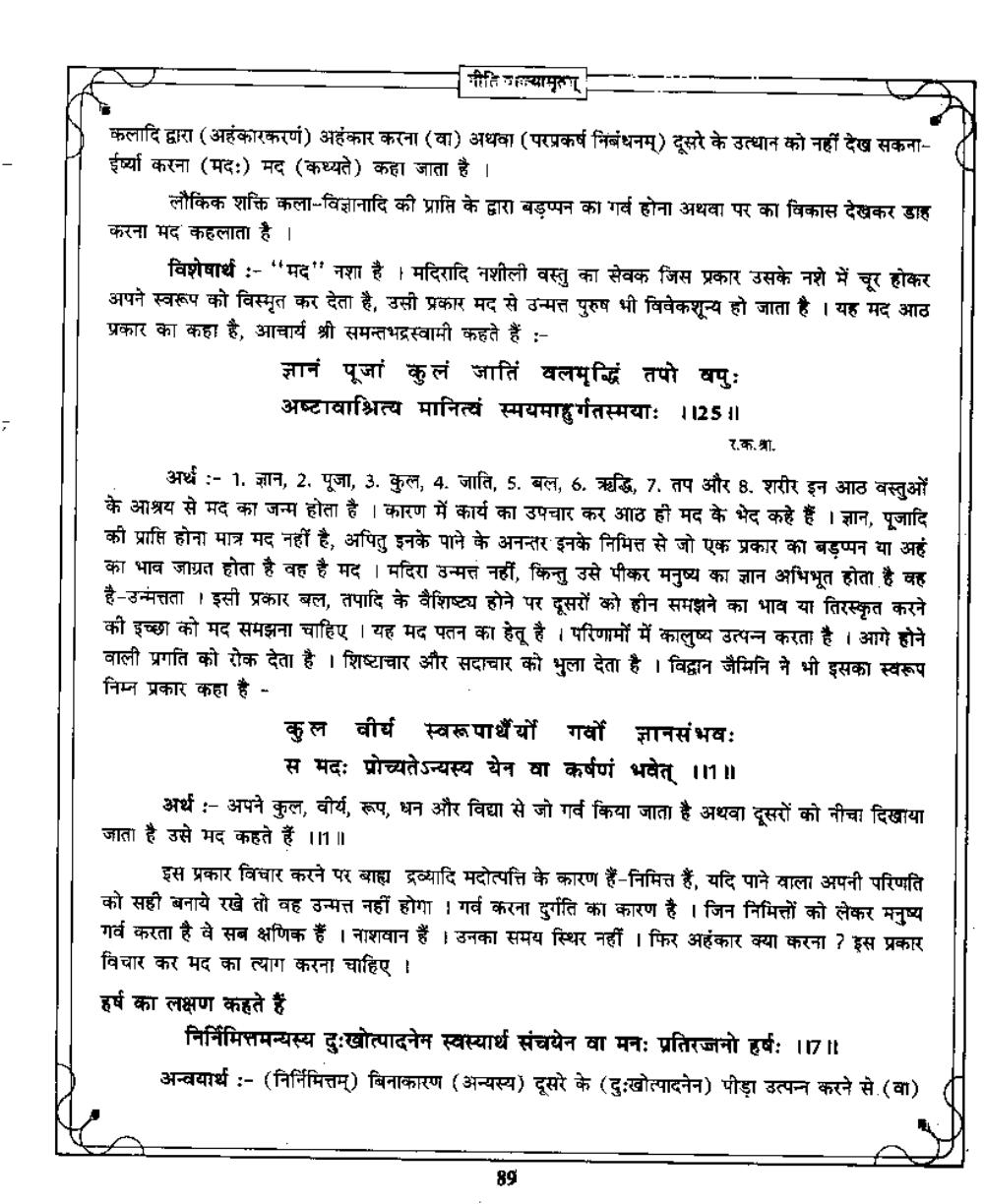________________
गीति यामृतम्
कलादि द्वारा (अहंकारकरणं) अहंकार करना (वा) अथवा (परप्रकर्ष निबंधनम् ) दूसरे के उत्थान को नहीं देख सकनाईर्ष्या करना (मदः) मद (कथ्यते) कहा जाता है ।
लौकिक शक्ति कला - विज्ञानादि की प्राप्ति के द्वारा बड़प्पन का गर्व होना अथवा पर का विकास देखकर डाह करना मद कहलाता है ।
विशेषार्थ :- " मद" नशा है । मदिरादि नशीली वस्तु का सेवक जिस प्रकार उसके नशे में चूर होकर अपने स्वरूप को विस्मृत कर देता है, उसी प्रकार मद से उन्मत्त पुरुष भी विवेकशून्य हो जाता है । यह मद आठ प्रकार का कहा है, आचार्य श्री समन्तभद्रस्वामी कहते हैं :
ज्ञानं पूजां कुलं जातिं वलमृद्धिं तपो वपुः अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयाः 1125 1
र. क. श्री.
अर्थ :- 1. ज्ञान, 2. पूजा, 3. कुल, 4 जाति, 5. बल, 6. ऋद्धि, 7. तप और 8. शरीर इन आठ वस्तुओं के आश्रय से मद का जन्म होता है । कारण में कार्य का उपचार कर आठ ही मद के भेद कहे हैं । ज्ञान, पूजादि की प्राप्ति होना मात्र मद नहीं है, अपितु इनके पाने के अनन्तर इनके निमित्त से जो एक प्रकार का बड़प्पन या अहं का भाव जाग्रत होता है वह है मद । मदिरा उन्मत नहीं, किन्तु उसे पीकर मनुष्य का ज्ञान अभिभूत होता है वह है - उन्मत्तता । इसी प्रकार बल, तपादि के वैशिष्ट्य होने पर दूसरों को हीन समझने का भाव या तिरस्कृत करने की इच्छा को मद समझना चाहिए। यह मद पतन का हेतू है। परिणामों में कालुष्य उत्पन्न करता है । आगे होने वाली प्रगति को रोक देता है । शिष्टाचार और सदाचार को भुला देता है । विद्वान जैमिनि ने भी इसका स्वरूप निम्न प्रकार कहा है
कुल वीर्य स्वरूपार्थे य गर्यो ज्ञानसंभवः स मदः प्रोच्यतेऽन्यस्य येन वा कर्षणं भवेत् ॥11॥
-
अर्थ अपने कुल, वीर्य, रूप, धन और विद्या से जो गर्व किया जाता है अथवा दूसरों को नीचा दिखाया जाता है उसे भद कहते हैं ।।1 ॥
इस प्रकार विचार करने पर बाह्य द्रव्यादि मदोत्पत्ति के कारण हैं-निमित्त हैं, यदि पाने वाला अपनी परिणति को सही बनाये रखे तो वह उन्मत्त नहीं होगा । गर्व करना दुर्गति का कारण है । जिन निमित्तों को लेकर मनुष्य गर्व करता है वे सब क्षणिक हैं । नाशवान हैं। उनका समय स्थिर नहीं । फिर अहंकार क्या करना ? इस प्रकार विचार कर मद का त्याग करना चाहिए ।
हर्ष का लक्षण कहते हैं
निर्निमित्तमन्यस्य दुःखोत्पादनेन स्वस्यार्थ संचयेन वा मनः प्रतिरज्जनो हर्षः ॥ 17 ॥ (निर्निमित्तम्) बिनाकारण (अन्यस्य) दूसरे के (दुःखोत्पादनेन) पीड़ा उत्पन्न करने से (वा)
अन्वयार्थ :
89