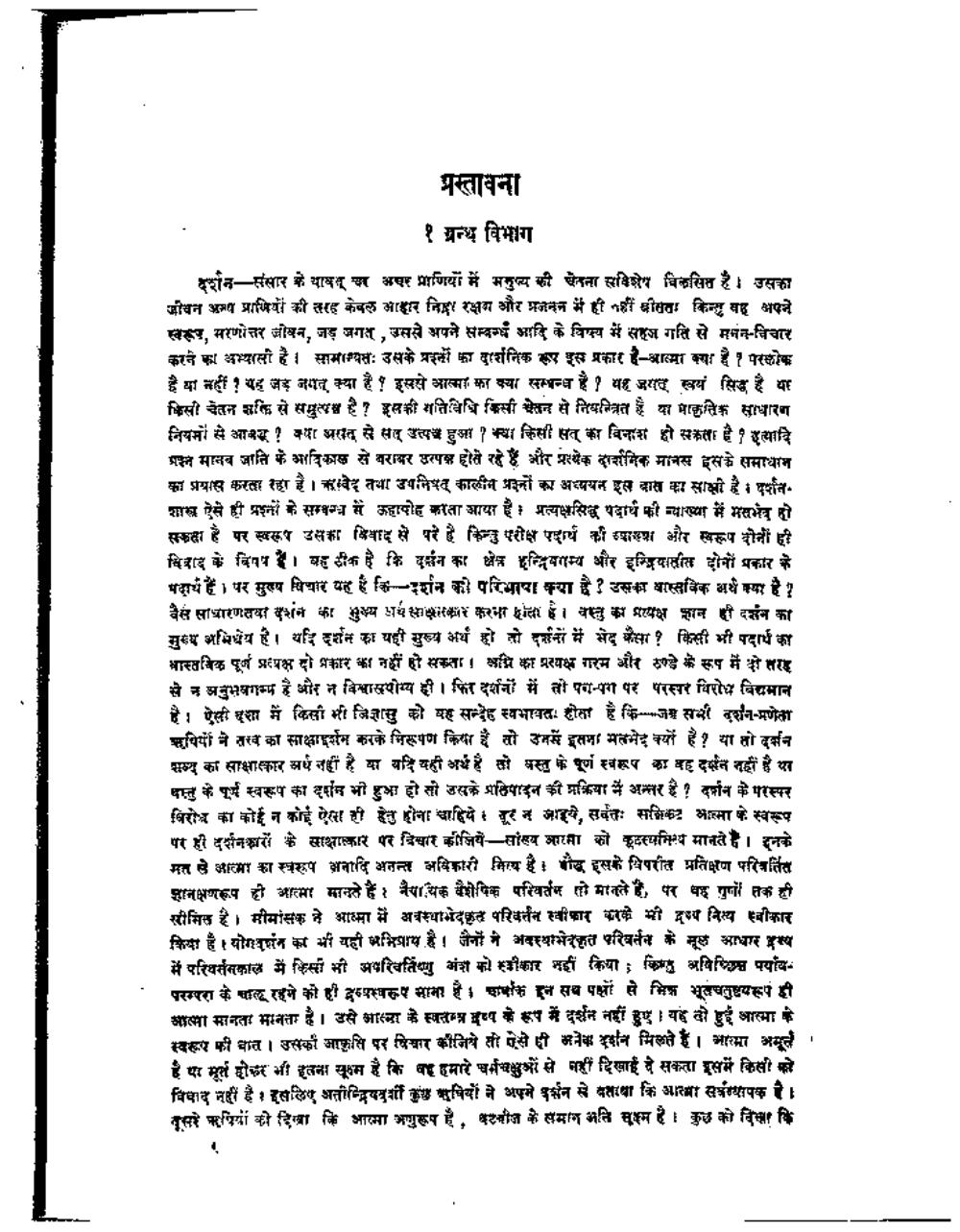________________
प्रस्तावना
१ ग्रन्थ विभाग
दर्शन-संसार के यावत् । अपर प्राणियों में मनुष्य की चेतना सविशेष बिन्द्रसित है। उसका जीवन अन्य प्राणियों की तरह केवल आहार निया रक्षा और प्रजनन में ही नहीं बीसता किन्तु वह अपने स्वरूप, मरणोत्तर जोक्न, जड़ जगत , उससे अपने सम्बन्ध आदि के विषय में सहज गति से मनन-विचार करने का अभ्यासी है। सामान्यतः उसके प्रश्नों का दार्शनिक रूप इस प्रकार है-श्रामा क्या है? परलोक है या नहीं? यह जड़ जगत् क्या है। इससे आत्मा का क्या सम्पन्ध है। यह जपत् वयं सिद्ध है या किसी चेतन शक्ति से समुत्पन है। इसकी गतिविधि किसी शेतन से नियन्त्रित है या माकृतिक साधारण नियमो से आरयू? क्या भरात से सत् उत्पन हुआ? क्या किसी सत् का विनाश हो सकता है इत्यादि प्रश्न मानव जाति के आदिकाल से बराबर उत्पन्न होते रहे हैं और प्रत्येक दार्शनिक मानस इसके समाधान का प्रयास करता रहा है। राम्वेद तथा उपनिषत् कालीन प्रश्नों का अध्ययन इस बात का साक्षी है। दर्शनशास्त्र ऐसे ही प्रश्नों के सम्बन्ध में ऊहापोह करता आया है। प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थ की म्यास्या में मसभेव हो सकता है पर स्वरूप उसका विवाद से परे है किन्तु परोक्ष पदार्थ की पारा और स्वरूप दोनों ही विवाद के विषय है। यह लीक है कि दर्शन का क्षेत्र इन्दियगम्य और इन्द्रियाप्तीस दोनों प्रकार के पदार्थ हैपर मुख्य विचार यह है कि दर्शन को परिभाषा क्या है? उसका वास्तविक अर्थ क्या है? वैस साधारणतया दर्शन का मुख्य अर्थाNRI करना है। वस्तु का पक्ष ज्ञान ही दर्शन का मुख्य अभिधेय है। यदि दर्शन का यही मुख्य अर्थ हो तो दर्शनों में भेद कैसा? किसी भी पदार्थ का भास्तविक पूर्ण प्रत्प्रक्ष दो प्रकार का नहीं हो सकता। अग्नि का प्रत्यक्ष गरम और टण्डे के रूप में दो तरह से न अनुभवाम्म है और न विभासयोग्य ही। फिर दर्शनों में तो पग-पग पर परसर विरोध विद्यमान है। ऐसी दशा में किसी भी जिज्ञासु को यह सन्देह स्वभावतः होता है कि सभी दर्शन-प्रणेता ऋषियों ने तस्व का साक्षादर्शन करके निरूपण किया है तो उनसे इसमा मतभेद क्यों है? या तो दर्शन समय का साक्षात्कार अर्थ नहीं है या यदि यही अर्थ है सो पस्त के पूर्ण स्वरूप का यह दर्शन नहीं है या पास्तु के पूर्ण स्वरूप का दाम भी हुआ हो सो उसके प्रतिपादन की प्रक्रिया में अन्तर है? दर्शन के परस्पर विरोध का कोई न कोई ऐसा ही हेनु होना चाहिये। पूरन आइये, सर्वतः समिकर आत्मा के स्वरूप पर ही दर्शनकारों के साक्षात्कार पर विचार कीजिये-सांख्य आरमा को कूटस्पनिय मानते है। इनके मत से आत्मा का स्वरूप अनादि अनन्त अविकारी सिाय है। चौर इसके विपरीत प्रतिक्षण परिवर्तित झानक्षणरूप ही आत्मा मानते हैं। नैया या वैशेषिक परिवर्तन हो मानते है, पर यह पुर्ण तक ही सीमित है। मीमांसको आत्मा मैं अवस्थाभेदकृत परिवर्तन स्वीकार करके भी दूध्य निस्य स्वीकार किया है। योगवन का भी यही अभिप्राय है। जैनों ने अवस्थामेरकृत परिवर्तन के मूल आधार स्य में परिवर्समकाल में किसी भी अपरिवर्तिणु अंश को स्वीकार नहीं किया कि अविछिन पयांवपरम्परा के चालू रहने को ही स्पस्वरूप माना है। शांक इन सब पक्षों से मिक भूतपतुष्टयरूप ही आला मानता मानता है। उसे आत्मा के स्वतन्त्र इष्प के रूप में दर्शन नहीं हुए। यह वो हारमा स्वरूप की बात । उसकी आकृति पर विचार कीजिये तो ऐसे ही अनेक दर्शन मिलते हैं। भारमा अमः । है या मुर्त होकर भी इतना सूक्ष्म है कि वह हमारे धर्मचक्षुओं से नहीं दिखाई दे सकता इसमें किसी को विवाद नहीं है। इसलिए अतीन्द्रियी कुछ अषियों ने अपने पर्शन से बताया कि मा सग्यापक। दूसरे पियों को दिखा कि आत्मा अगुरूप है . टीज के समान अति सक्ष्म है। कुछ को दिशा कि