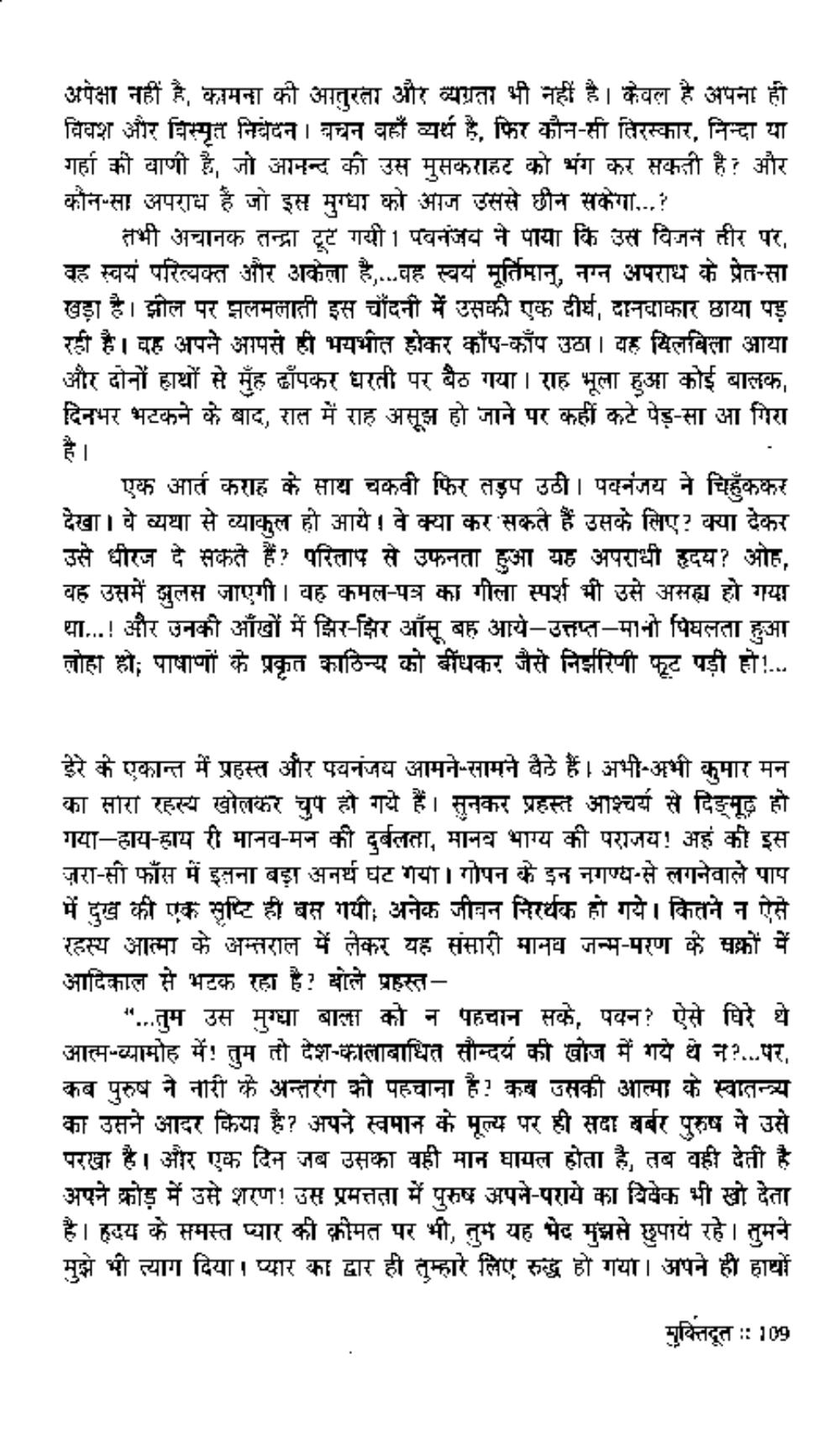________________
अपेक्षा नहीं है, कामना की आतुरता और व्यग्रता भी नहीं है। केवल है अपना ही विवश और विस्मृत निवेदन । बचन वहाँ व्यर्थ है, फिर कौन-सी तिरस्कार, निन्दा या गर्हा की वाणी है, जो आनन्द की उस मुसकराहट को भंग कर सकती है? और कौन-सा अपराध हैं जो इस मुग्धा को आज उससे छीन सकेगा...?
तभी अचानक तन्द्रा टूट गयी। पवनंजय ने पाया कि उस विजन तीर पर, वह स्वयं परित्यक्त और अकेला है... वह स्वयं मूर्तिमान्, नग्न अपराध के प्रेत-सा खड़ा है। झील पर झलमलाती इस चाँदनी में उसकी एक दीर्घ, दानवाकार छाया पड़ रही है। वह अपने आपसे ही भयभीत होकर काँप-काँप उठा। वह बिलबिला आया और दोनों हाथों से मुँह ढाँपकर धरती पर बैठ गया। राह भूला हुआ कोई बालक, दिनभर भटकने के बाद रात में राह असूझ हो जाने पर कहीं कटे पेड़-सा आ गिरा है ।
एक आर्त कराह के साथ चकवी फिर तड़प उठी। पवनंजय ने चिहुँककर देखा । वे व्यथा से व्याकुल ही आये। वे क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्या देकर उसे धीरज दे सकते हैं? परिताप से उफनता हुआ यह अपराधी हृदय ? ओह, वह उसमें झुलस जाएगी। वह कमल -पत्र का गीला स्पर्श भी उसे असह्य हो गया था....! और उनकी आँखों में झिरझिर आँसू बह आये उत्तप्त- मानो पिघलता हुआ लोहा हो; पाषाणों के प्रकृत काठिन्य को बींधकर जैसे निर्झरिणी फूट पड़ी हो !...
-
डेरे के एकान्त में प्रहस्त और पवनंजय आमने-सामने बैठे हैं। अभी-अभी कुमार मन का सारा रहस्य खोलकर चुप हो गये हैं। सुनकर प्रहस्त आश्चर्य से दिङ्मूढ़ हो गया - हाय-हाय री मानव मन की दुर्बलता, मानव भाग्य की पराजय ! अहं की इस ज़रा-सी फाँस में इतना बड़ा अनर्थ घट गया । गोपन के इन नगण्य से लगनेवाले पाप में दुख की एक सृष्टि ही बस गयी अनेक जीवन निरर्थक हो गये। कितने न ऐसे रहस्य आत्मा के अन्तराल में लेकर यह संसारी मानव जन्म-मरण के चक्रों में आदिकाल से भटक रहा है? बोले प्रहस्त
"... तुम उस मुग्धा बाला को न पहचान सके, पवन? ऐसे घिरे थे आत्म-व्यामोह में! तुम तो देश-कालाबाधित सौन्दर्य की खोज में गये थे न... पर. कब पुरुष ने नारी के अन्तरंग को पहचाना है? कब उसकी आत्मा के स्वातन्त्र्य का उसने आदर किया है? अपने स्वमान के मूल्य पर ही सदा बर्बर पुरुष ने उसे परखा है। और एक दिन जब उसका वही मान घायल होता है, तब वही देती है -अपने क्रोड़ में उसे शरण ! उस प्रमत्तता में पुरुष अपने-पराये का विवेक भी खो देता है। हृदय के समस्त प्यार की कीमत पर भी, तुम यह भेद मुझसे छुपाये रहे । तुमने मुझे भी त्याग दिया। प्यार का द्वार ही तुम्हारे लिए रुद्ध हो गया। अपने ही हाथों
मुक्तिदूत :: 109