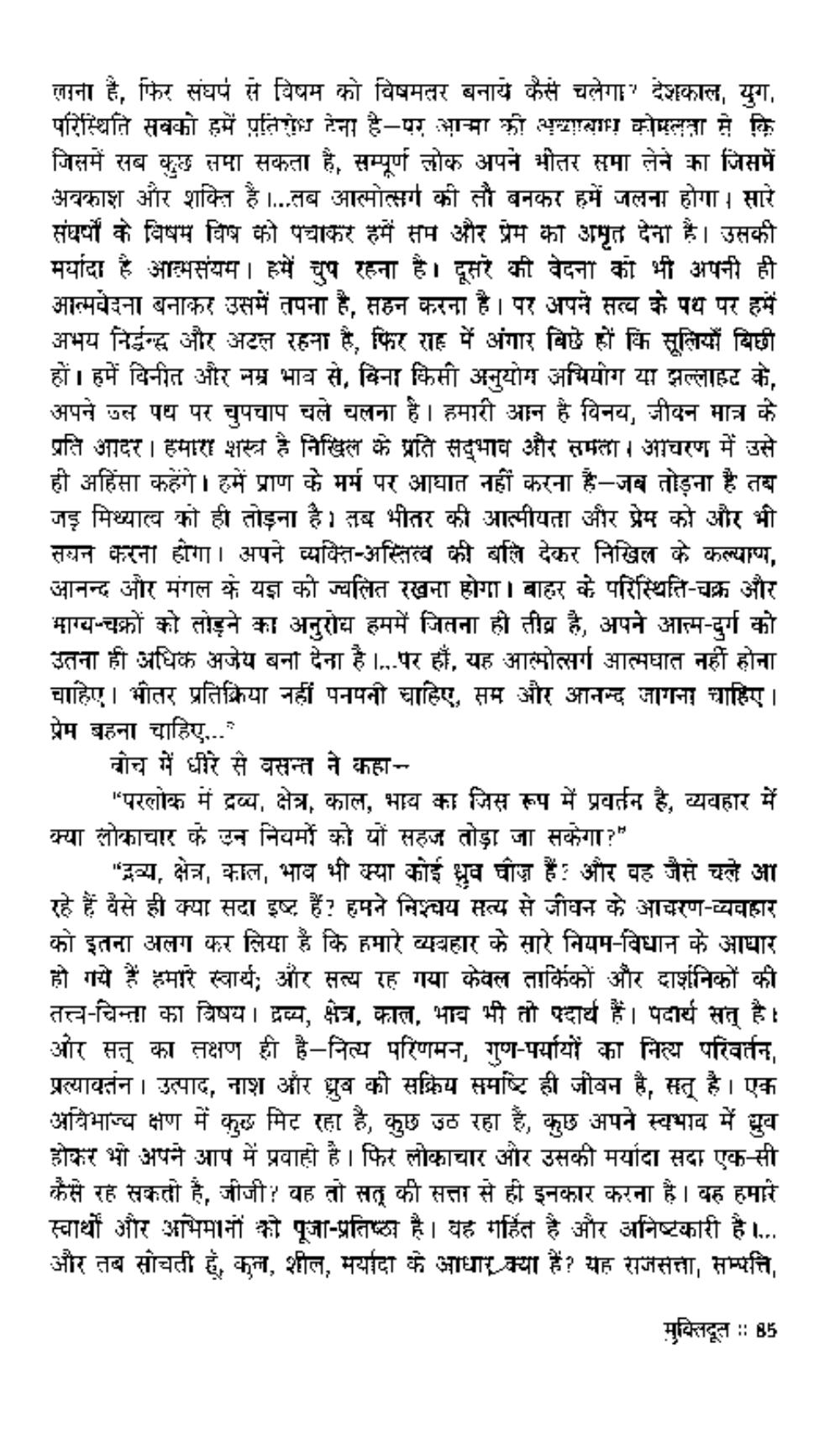________________
लाना है, फिर संघर्प से विषम को विषमतर बनाये कैसे चलेगा। देशकाल, युग, परिस्थिति सवको हमें प्रतिरोध देना है-पर आमा की भावना कोमलता से कि जिसमें सब कुछ समा सकता है, सम्पूर्ण लोक अपने भीतर समा लेने का जिसमें अवकाश और शक्ति हैं।...तब आत्मोत्सग की तौ बनकर हमें जलना होगा। सारे संघर्षों के विषम विष को पचाकर हमें सम और प्रेम का अमृत देना है। उसकी मर्यादा है आत्मसंयम। हमें चुप रहना है। दूसरे की वेदना को भी अपनी ही आत्मवेदना बनाकर उसमें तपना है, सहन करना है। पर अपने सत्य के पथ पर हमें अभय निर्द्धन्द्ध और अटल रहना है, फिर राह में अंगार बिछे हो कि सूलियों बिछी हों। हमें विनीत और नम्र भाव से, बिना किसी अनुयोग अभियोग या झल्लाहट के, अपने उस पथ पर चुपचाप चले चलना है। हमारी आन है विनय, जीवन मात्र के प्रति आदर । हमारा शस्त्र है निखिल के प्रति सद्भाव और समता । आचरण में उसे ही अहिंसा कहेंगे। हमें प्राण के मर्म पर आघात नहीं करना है-जब तोड़ना है तब जड़ मिथ्याल्व को ही तोड़ना है। सब भीतर की आत्मीयता और प्रेम को और भी सयन करना होगा। अपने व्यक्ति-अस्तित्व की बलि देकर निखिल के कल्याण, आनन्द और मंगल के यज्ञ को ज्वलित रखना होगा। बाहर के परिस्थिति-चक्र और माग्य-चक्रों को तोड़ने का अनुरोध हममें जितना ही तीव्र है, अपने आत्म-दर्ग को उतना ही अधिक अजेय बना देना है।...पर हाँ, यह आत्मोत्सर्ग आत्मघात नहीं होना चाहिए। भीतर प्रतिक्रिया नहीं पनपनी चाहिए, सम और आनन्द जागना चाहिए। प्रेम बहना चाहिए....
बोच में धीरे से वसन्त ने कहा
"परलोक में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का जिस रूप में प्रवर्तन है, व्यवहार में क्या लोकाचार के इन नियमों को यों सहज तोड़ा जा सकेगा?"
___ "व्य, क्षेत्र, काल, भाव भी क्या कोई ध्रुव चीज़ हैं: और वह जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही क्या सदा इष्ट हैं? हमने निश्चय सत्य से जीवन के आचरण-व्यवहार को इतना अलग कर लिया है कि हमारे व्यवहार के सारे नियम-विधान के आधार हो गये हैं हमारे स्वार्थ और सत्य रह गया केवल ताकिकों और दार्शनिकों की तत्त्व-चिन्ता का विषय। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाब भी तो पदार्थ हैं। पदार्थ सत है।
और सत् का सक्षण ही है-नित्य परिणमन, गुण-पर्यायों का नित्य परिवर्तन, प्रत्यावर्तन। उत्पाद, नाश और ध्रुब की सक्रिय समष्टि ही जीवन है, सत् है। एक अविभाज्य क्षण में कुछ मिट रहा है, कुछ उठ रहा हैं, कुछ अपने स्वभाव में ध्रुव होकर भी अपने आप में प्रवाही है। फिर लोकाचार और उसकी मर्यादा सदा एक-सी कैसे रह सकती हैं, जीजी! वह तो सत की सत्ता से ही इनकार करना है। वह हमारे स्वार्थों और आभमानों को पूजा-प्रतिष्ठा है। वह गहित है और अनिष्टकारी है।... और तब सोचती हूं, कुल, शील, मर्यादा के आधार क्या हैं? यह राजसत्ता, सम्पत्ति,
मुक्लिदूत :: 85