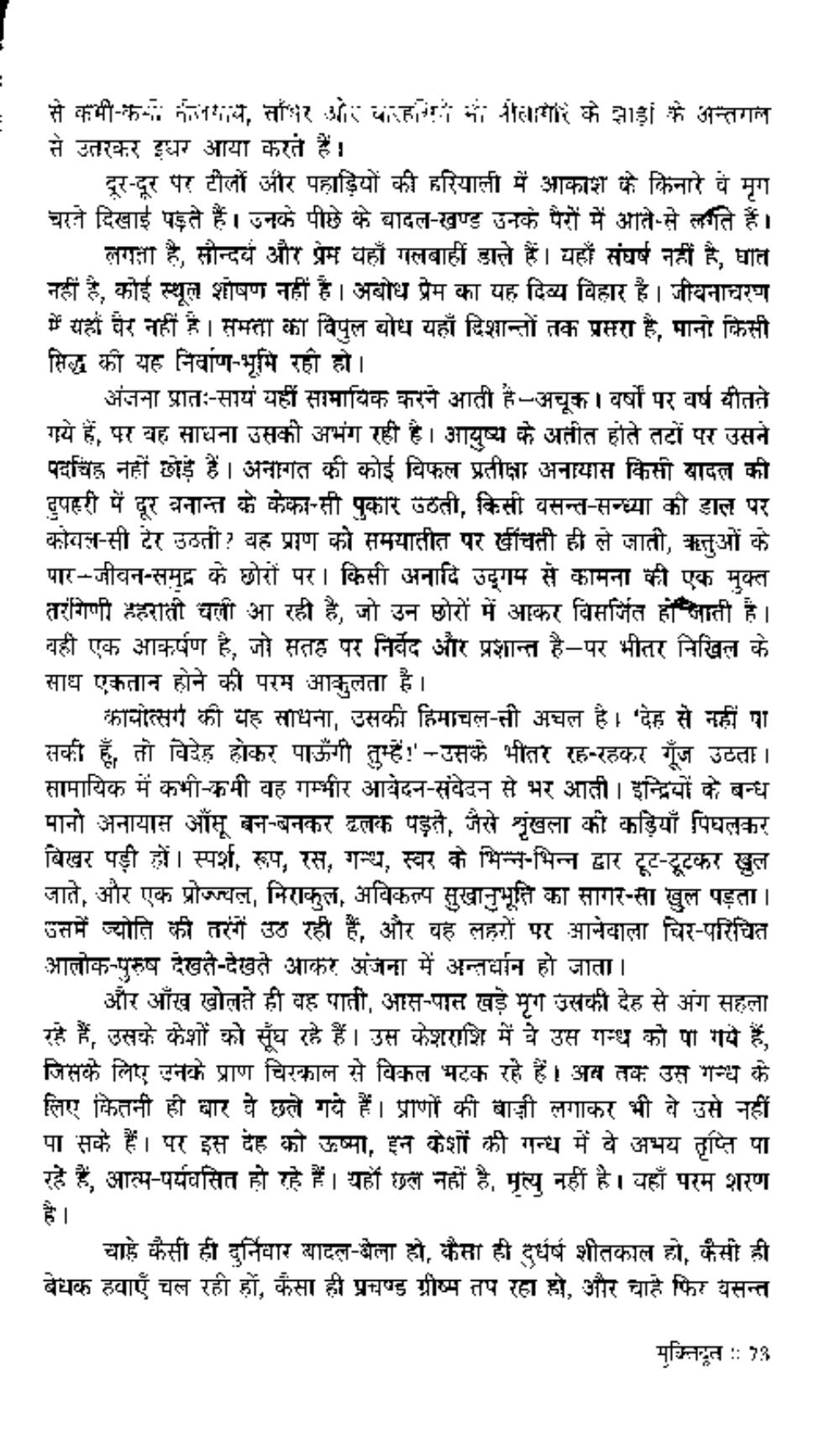________________
से कमी-कम मनाल, तांभर और बाहर भी नौलागार के झाड़ा के अन्तगल से उत्तरकर इधर आया करते हैं।
दूर-दूर पर टीलों और पहाड़ियों की हरियाली में आकाश के किनारे वे मृग चरते दिखाई पड़ते हैं। उनके पीछे के बादल-खण्ट उनके पैरों में आते-से लगते हैं।
लगता है, सौन्दर्य और प्रेम यहाँ गलबाहीं डाले हैं। यहाँ संघर्ष नहीं है, घात नहीं है, कोई स्थूल शोषण नहीं हैं। अबोध प्रेम का यह दिव्य विहार है। जीवनाचरण में यहीं वैर नहीं हैं। समता का विपुल बोध यहाँ दिशान्तों तक प्रसरा है, मानो किसी सिद्ध की यह निर्माण-भूमि रही हो।
अंजना प्रातः-सायं यहीं सामायिक करने आती है-अचूक। वर्षों पर वर्ष बीतते गये हैं, पर वह साधना उसकी अभंग रही है। आयुष्य के अतीत होते तटों पर उसने पदचिह्न नहीं छोड़े हैं। अनागत की कोई विफल प्रतीक्षा अनायास किसी यादल की दुपहरी में दूर बनान्त के केका-सी पुकार उठती, किसी वसन्त-सन्ध्या की डाल पर कोवल-सी टेर उठती? यह प्राण को समयातीत पर खींचती ही ले जाती, ऋतुओं के पार-जीवन-समुद्र के छोरों पर। किसी अनादि उद्गम से कामना की एक मुक्त तरंगिणी हहराती चली आ रही है, जो उन छोरों में आकर विसर्जित हो जाती हैं। वहीं एक आकर्षण है, जो सतह पर निर्वेद और प्रशान्त है-पर भीतर निखिल के साध एकतान होने की परम आकुलता हैं।
काचोत्सग की यह साधना, उसकी हिमाचल-सी अचल है। 'देह से नहीं पा सकी हूँ, तो विदेह होकर पाऊँगी तुम्हें!' --उसके भीतर रह-रहकर गूंज उठता। सामायिक में कभी-कमी वह गम्भीर आवेदन-संवेदन से भर आती। इन्द्रियों के बन्ध पानो अनायास आँसू बन-बनकर ढलक पड़ते, जैसे शृंखला की कड़ियाँ पिघलकर बिखर पड़ी हो। स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, स्वर के भिन्न-भिन्न द्वार टूट-टूटकर खुल जाते, और एक प्रोज्वल, निराकुल, अविकल्प सुखानुभूति का सागर-सा खुल पड़ता। उसमें ज्योति की तरंगें उठ रही हैं, और वह लहरों पर आनेवाला चिर-परिचित आलोक-पुरुष देखते-देखते आकर अंजना में अन्तर्धान हो जाता।
और आँख खोलते ही वह पाती, आस-पास खड़े मृग उसकी देह से अंग सहला रहे हैं, उसके केशों को सूंघ रहे हैं। उस केशराशि में वे उस गन्ध को पा गये हैं, जिसके लिए उनके प्राण चिरकाल से विकल भटक रहे हैं। अब तक उस गन्ध के लिए कितनी ही बार चे छते गये हैं। प्राणों की बाजी लगाकर भी वे उसे नहीं पा सके हैं। पर इस देह को ऊष्मा, इन केशों की गन्ध में वे अभय तृप्ति पा रहे हैं, आत्म-पर्यवसित हो रहे हैं। यहाँ छल नहीं है, मृत्यु नहीं है। वहाँ परम शरण
चाहे कैसी ही दुर्निवार त्यादल-बेला हो, कैसा ही दुर्धर्ष शीतकाल हो, कैसी ही बेधक हवाएँ चल रही हों, कैसा ही प्रचण्ड ग्रीष्म तप रहा हो, और चाहे फिर बसन्त
मस्तिदूत :: 78