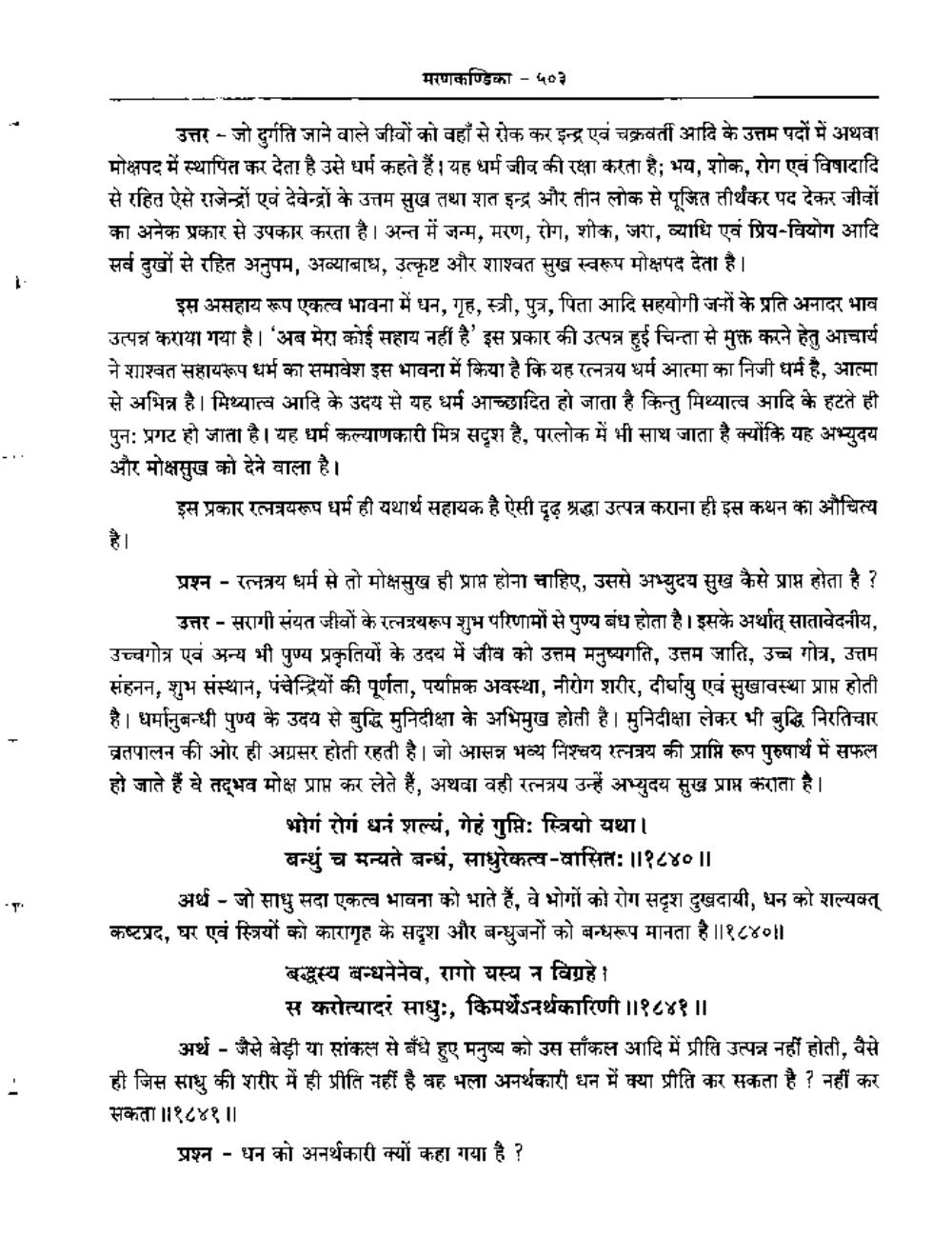________________
मरणकण्डिका - ५०३
उत्तर - जो दुर्गति जाने वाले जीवों को वहाँ से रोक कर इन्द्र एवं चक्रवर्ती आदि के उत्तम पदों में अथवा मोक्षपद में स्थापित कर देता है उसे धर्म कहते हैं। यह धर्म जीव की रक्षा करता है; भय, शोक, रोग एवं विषादादि से रहित ऐसे राजेन्द्रों एवं देवेन्द्रों के उत्तम सुख तथा शत इन्द्र और तीन लोक से पूजित तीर्थकर पद देकर जीवों का अनेक प्रकार से उपकार करता है। अन्त में जन्म, मरण, रोग, शोक, जरा, व्याधि एवं प्रिय-वियोग आदि सर्व दुखों से रहित अनुपम, अव्याबाध, उत्कृष्ट और शाश्वत सुख स्वरूप मोक्षपद देता है।
इस असहाय रूप एकत्व भावना में धन, गृह, स्त्री, पुत्र, पिता आदि सहयोगी जनों के प्रति अनादर भाव उत्पन्न कराया गया है। अब मेरा कोई सहाय नहीं है' इस प्रकार की उत्पन्न हुई चिन्ता से मुक्त करने हेतु आचार्य ने शाश्वत सहायरूप धर्म का समावेश इस भावना में किया है कि यह रत्नत्रय धर्म आत्मा का निजी धर्म है, आत्मा से अभिन्न है। मिथ्यात्व आदि के उदय से यह धर्म आच्छादित हो जाता है किन्तु मिथ्यात्व आदि के हटते ही पुन: प्रगट हो जाता है। यह धर्म कल्याणकारी मित्र सदृश है, परलोक में भी साथ जाता है क्योंकि यह अभ्युदय और मोक्षसुख को देने वाला है।
इस प्रकार रत्नत्रयरूप धर्म ही यथार्थ सहायक है ऐसी दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कराना ही इस कथन का औचित्य
प्रश्न - रत्नत्रय धर्म से तो मोक्षसुख ही प्राप्त होना चाहिए, उससे अभ्युदय सुख कैसे प्राप्त होता है ?
उत्तर - सरागी संयत जीवों के रत्नत्रयरूप शुभ परिणामों से पुण्य बंध होता है। इसके अर्थात् सातावेदनीय, उच्चगोत्र एवं अन्य भी पुण्य प्रकृतियों के उदय में जीव को उत्तम मनुष्यगति, उत्तम जाति, उच्च गोत्र, उत्तम संहनन, शुभ संस्थान, पंचेन्द्रियों की पूर्णता, पर्याप्तक अवस्था, नीरोग शरीर, दीर्घायु एवं सुखावस्था प्राप्त होती है। धर्मानुबन्धी पुण्य के उदय से बुद्धि मुनिदीक्षा के अभिमुख होती है। मुनिदीक्षा लेकर भी बुद्धि निरतिचार व्रतपालन की ओर ही अग्रसर होती रहती है। जो आसन्न भव्य निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ में सफल हो जाते हैं वे तद्भव मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, अथवा वही रत्नत्रय उन्हें अभ्युदय सुख प्राप्त कराता है।
भोगं रोगं धनं शल्यं, गेहं गुप्तिः स्त्रियो यथा।
बन्धुं च मन्यते बन्धं, साधुरेकत्व-वासितः॥१८४० ।। अर्थ - जो साधु सदा एकत्व भावना को भाते हैं, वे भोगों को रोग सदृश दुखदायी, धन को शल्यक्त् कष्टप्रद, घर एवं स्त्रियों को कारागृह के सदृश और बन्धुजनों को बन्धरूप मानता है ।।१८४०।।
बद्धस्य बन्धनेनेव, रागो यस्य न विग्रहे।
स करोत्यादरं साधुः, किमर्थेऽनर्थकारिणी ॥१८४१ ।। अर्थ - जैसे बेड़ी या सांकल से बँधे हुए मनुष्य को उस साँकल आदि में प्रीति उत्पन्न नहीं होती, वैसे ही जिस साधु की शरीर में ही प्रीति नहीं है वह भला अनर्थकारी धन में क्या प्रीति कर सकता है ? नहीं कर सकता॥१८४१।।
प्रश्न - धन को अनर्थकारी क्यों कहा गया है ?