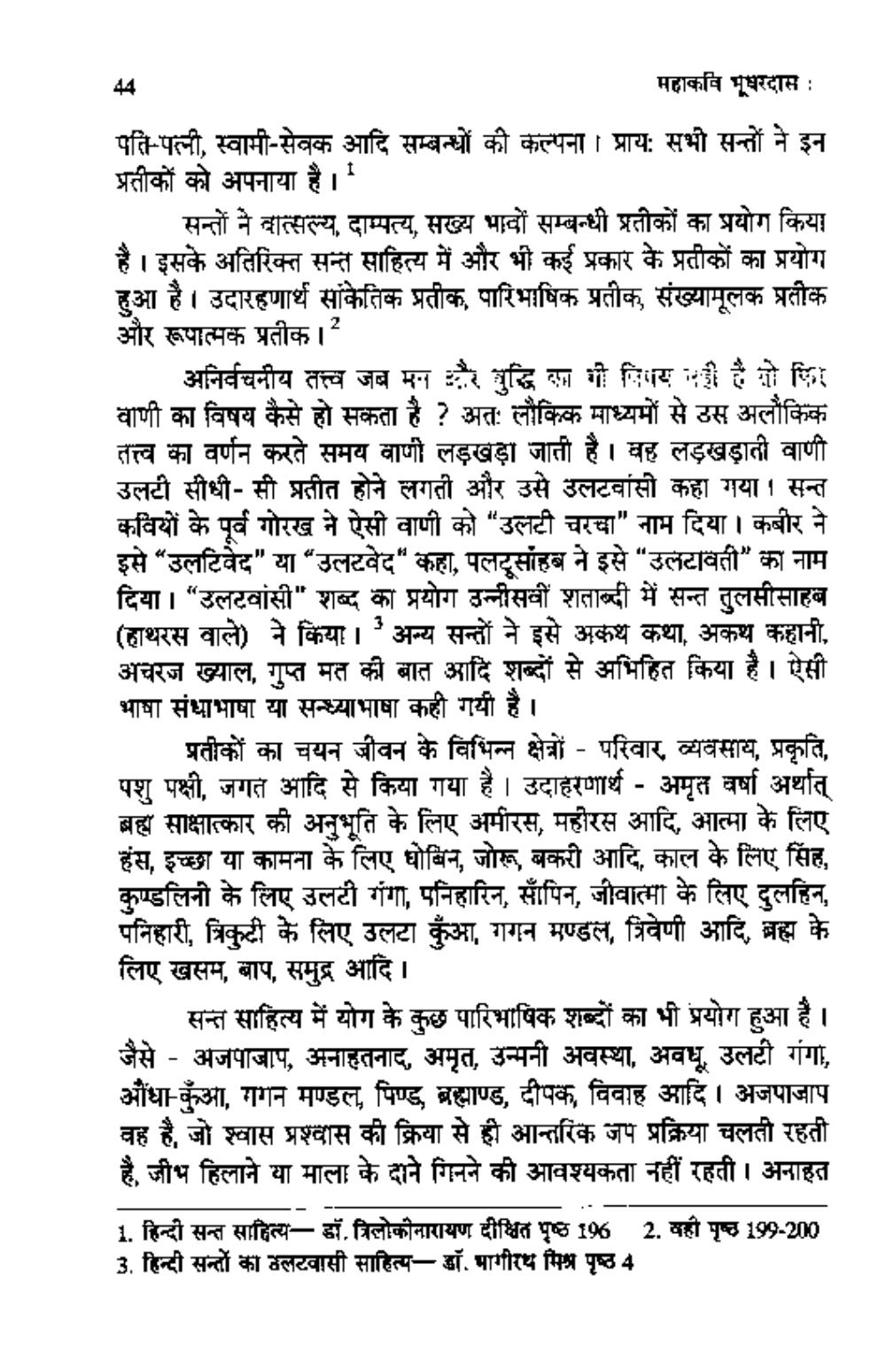________________
महाकवि भूधरदास : पति-पत्नी, स्वामी-सेवक आदि सम्बन्धों की कल्पना । प्राय: सभी सन्तों ने इन प्रतीकों को अपनाया है।
सन्तों ने वात्सल्य, दाम्पत्य, सख्य भावों सम्बन्धी प्रतीकों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त सन्त साहित्य में और भी कई प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। उदारहणार्थ सांकेतिक प्रतीक, पारिभाषिक प्रतीक, संख्यामूलक प्रतीक और रूपात्मक प्रतीक ।
अनिर्वचनीय तत्त्व जब मन और बुद्धि का गी निगाय ही है तो फिर वाणी का विषय कैसे हो सकता है ? अत: लौकिक माध्यमों से उस अलौकिक तत्त्व का वर्णन करते समय वाणी लड़खड़ा जाती है । वह लड़खड़ाती वाणी उलटी सीधी-सी प्रतीत होने लगती और उसे उलटवांसी कहा गया । सन्त कवियों के पूर्व गोरख ने ऐसी वाणी को "उलटी चरचा" नाम दिया। कबीर ने इसे “उलटिवेद" या "उलटवेद" कहा, पलटूसाहब ने इसे "उलटावती" का नाम दिया। “उलटवांसी" शब्द का प्रयोग उन्नीसवीं शताब्दी में सन्त तुलसीसाहब (हाथरस वाले) ने किया।' अन्य सन्तों ने इसे अकथ कथा, अकथ कहानी, अचरज ख्याल, गुप्त मत की बात आदि शब्दों से अभिहित किया है । ऐसी भाषा संधाभाषा या सन्ध्याभाषा कही गयी है ।
__ प्रतीकों का चयन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों - परिवार, व्यवसाय, प्रकृति, पशु पक्षी, जगत आदि से किया गया है। उदाहरणार्थ - अमृत वर्षा अर्थात् ब्रह्म साक्षात्कार की अनुभूति के लिए अमीरस, महीरस आदि, आत्मा के लिए हंस, इच्छा या कामना के लिए धोबिन, जोरू, बकरी आदि, काल के लिए सिंह, कुण्डलिनी के लिए उलटी गंगा, पनिहारिन, सॉपिन, जीवात्मा के लिए दुलहिन, पनिहारी, त्रिकुटी के लिए उलटा कुंआ, गगन मण्डल, त्रिवेणी आदि, ब्रह्म के लिए खसम, बाप, समुद्र आदि।
सन्त साहित्य में योग के कुछ पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । जैसे - अजपाजाप, अनाहतनाद, अमृत, उन्मनी अवस्था, अवधू, उलटी गंगा, औंधा कुंआ, गगन मण्डल, पिण्ड, ब्रह्माण्ड, दीपक, विवाह आदि । अजपाजाप वह है, जो श्वास प्रश्वास की क्रिया से ही आन्तरिक जप प्रक्रिया चलती रहती है, जीभ हिलाने या माला के दाने गिनने की आवश्यकता नहीं रहती। अनाहत 1. हिन्दी सन्त साहित्य- डॉ. त्रिलोकीनारायण दीक्षित पृष्ठ 19 2. वही पृष्ठ 199-200 3. हिन्दी सन्तों का उलटवासी साहित्य-डॉ.भागीरथ मिश्र पृष्ठ 4