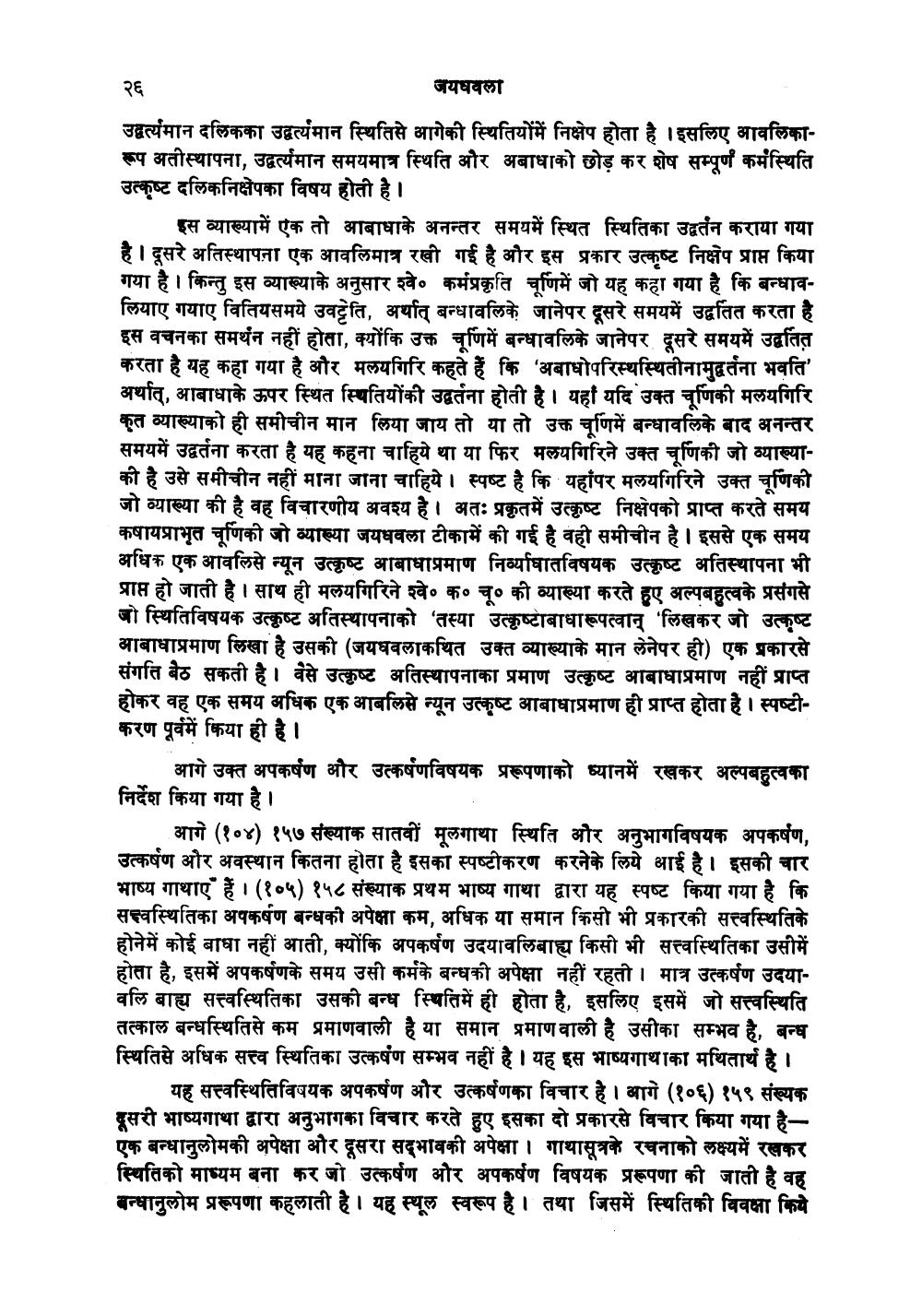________________
२६
जयधवला
उद्वर्त्यमान दलिकका उद्वय॑मान स्थितिसे आगेकी स्थितियोंमें निक्षेप होता है । इसलिए आवलिकारूप अतीस्थापना, उद्वर्त्यमान समयमात्र स्थिति और अबाधाको छोड़ कर शेष सम्पूर्ण कर्मस्थिति उत्कृष्ट दलिकनिक्षेपका विषय होती है।
इस व्याख्यामें एक तो आबाधाके अनन्तर समयमें स्थित स्थितिका उद्वर्तन कराया गया है। दूसरे अतिस्थापना एक आवलिमात्र रखी गई है और इस प्रकार उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त किया गया है। किन्तु इस व्याख्याके अनुसार श्वे० कर्मप्रकृति चूणिमें जो यह कहा गया है कि बन्धावलियाए गयाए वितियसमये उवट्टेति, अर्थात् बन्धावलिके जानेपर दूसरे समयमें उर्तित करता है इस वचनका समर्थन नहीं होता, क्योंकि उक्त चूर्णिमें बन्धावलिके जानेपर दूसरे समयमें उर्तित करता है यह कहा गया है और मलयगिरि कहते हैं कि 'अबाधोपरिस्थस्थितीनामुद्वर्तना भवति' अर्थात्, आबाधाके ऊपर स्थित स्थितियोंकी उद्वर्तना होती है। यहां यदि उक्त चूर्णिकी मलयगिरि कृत व्याख्याको ही समीचीन मान लिया जाय तो या तो उक्त चूणिमें बन्धावलिके बाद अनन्तर समयमें उद्वर्तना करता है यह कहना चाहिये था या फिर मलयगिरिने उक्त चूर्णिकी जो व्याख्याकी है उसे समीचीन नहीं माना जाना चाहिये। स्पष्ट है कि यहाँपर मलयगिरिने उक्त चूर्णिको जो व्याख्या की है वह विचारणीय अवश्य है। अतः प्रकृतमें उत्कृष्ट निक्षेपको प्राप्त करते समय कषायप्राभूत चूर्णिको जो व्याख्या जयधवला टीकामें की गई है वही समीचीन है । इससे एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण निर्व्याघातविषयक उत्कृष्ट अतिस्थापना भी प्राप्त हो जाती है । साथ ही मलयगिरिने श्वे. क. चू० की व्याख्या करते हुए अल्पबहुत्वके प्रसंगसे जो स्थितिविषयक उत्कृष्ट अतिस्थापनाको 'तस्या उत्कृष्टाबाधारूपत्वान् 'लिखकर जो उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण लिखा है उसकी (जयधवलाकथित उक्त व्याख्याके मान लेनेपर ही) एक प्रकारसे संगति बैठ सकती है। वैसे उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण नहीं प्राप्त होकर वह एक समय अधिक एक आबलिसे न्यून उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण ही प्राप्त होता है । स्पष्टीकरण पूर्वमें किया ही है।
_आगे उक्त अपकर्षण और उत्कर्षणविषयक प्ररूपणाको ध्यानमें रखकर अल्पबहुत्वका निर्देश किया गया है।
__आगे (१०४) १५७ संख्याक सातवीं मूलगाथा स्थिति और अनुभागविषयक अपकर्षण, उत्कर्षण और अवस्थान कितना होता है इसका स्पष्टीकरण करनेके लिये आई है। इसकी चार भाष्य गाथाएं हैं । (१०५) १५८ संख्याक प्रथम भाष्य गाथा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सत्त्वस्थितिका अपकर्षण बन्धकी अपेक्षा कम, अधिक या समान किसी भी प्रकारकी सत्त्वस्थितिके होनेमें कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि अपकर्षण उदयावलिबाह्य किसी भी सत्त्वस्थितिका उसीमें होता है, इसमें अपकर्षणके समय उसी कर्मके बन्धकी अपेक्षा नहीं रहती। मात्र उत्कर्षण उदयावलि बाह्य सत्त्वस्थितिका उसकी बन्ध स्थितिमें ही होता है, इसलिए इसमें जो सत्त्वस्थिति तत्काल बन्धस्थितिसे कम प्रमाणवाली है या समान प्रमाण वाली है उसीका सम्भव है, बन्ध स्थितिसे अधिक सत्त्व स्थितिका उत्कर्षण सम्भव नहीं है । यह इस भाष्यगाथाका मथितार्थ है।
यह सत्त्वस्थितिविषयक अपकर्षण और उत्कर्षणका विचार है । आगे (१०६) १५९ संख्यक दूसरी भाष्यगाथा द्वारा अनुभागका विचार करते हुए इसका दो प्रकारसे विचार किया गया हैएक बन्धानुलोमकी अपेक्षा और दूसरा सद्भावकी अपेक्षा। गाथासूत्रके रचनाको लक्ष्यमें रखकर स्थितिको माध्यम बना कर जो उत्कर्षण और अपकर्षण विषयक प्ररूपणा की जाती है वह बन्धानुलोम प्ररूपणा कहलाती है। यह स्थूल स्वरूप है। तथा जिसमें स्थितिको विवक्षा किये