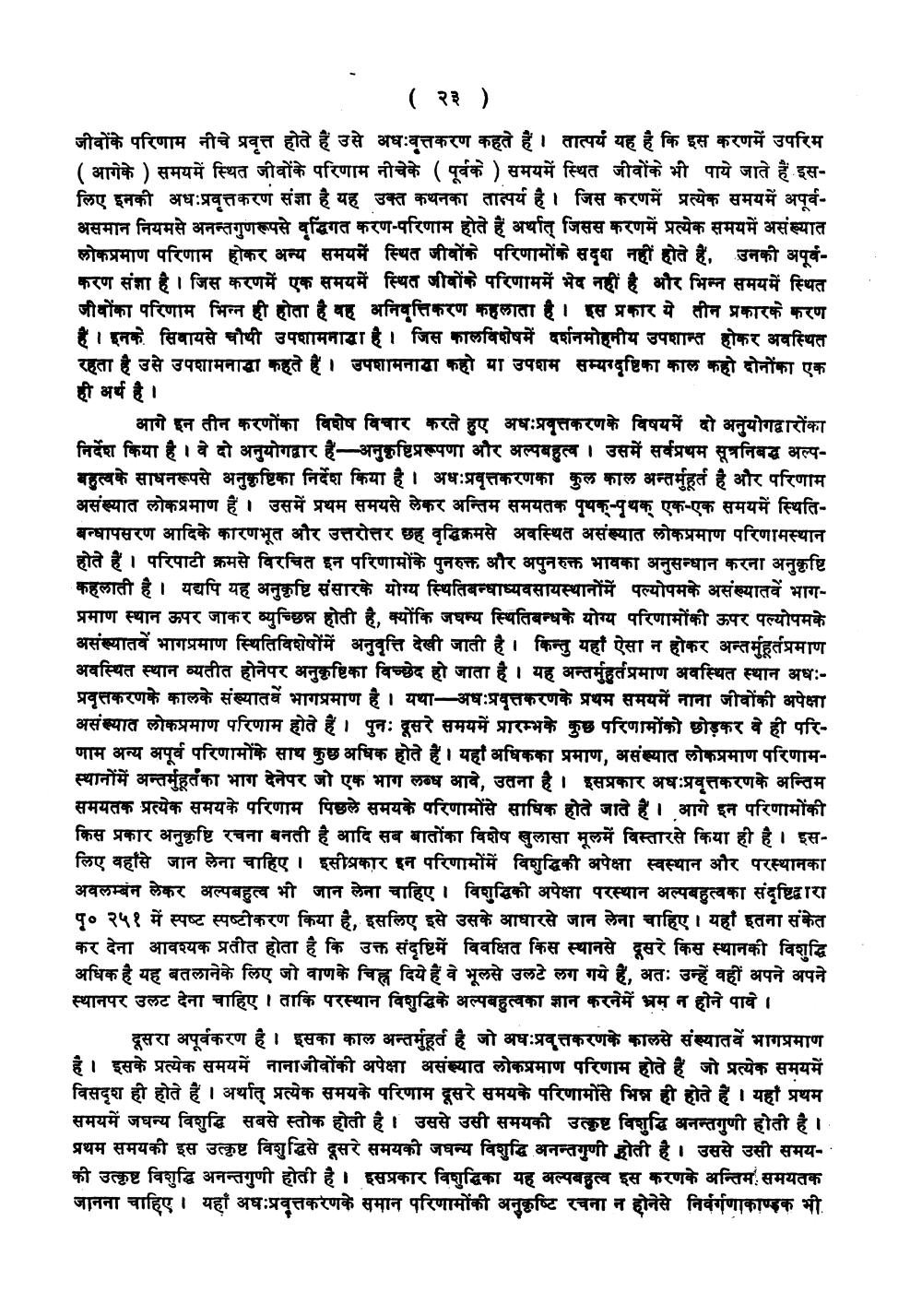________________
( २३ ) जीवोंके परिणाम नीचे प्रवृत्त होते हैं उसे अधःवृत्तकरण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि इस करणमें उपरिम ( आगे ) समयमें स्थित जीवोंके परिणाम नीचेके ( पूर्वके ) समयमें स्थित जीवोंके भी पाये जाते हैं इसलिए इनकी अधःप्रवृत्तकरण संज्ञा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। जिस करणमें प्रत्येक समयमें अपूर्वअसमान नियमसे अनन्तगुणरूपसे वृद्धिंगत करण-परिणाम होते हैं अर्थात् जिसस करणमें प्रत्येक समयमें असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम होकर अन्य समयमें स्थित जीवोंके परिणामोंके सदृश नहीं होते हैं, उनकी अपूर्वकरण संज्ञा है। जिस करणमें एक समयमें स्थित जीवोंके परिणाममें भेद नहीं है और भिन्न समयमें स्थित जीवोंका परिणाम भिन्न ही होता है वह अनिवृत्तिकरण कहलाता है। इस प्रकार ये तीन प्रकारके फरण है । इनके सिवायसे चौथी उपशामनाता है। जिस कालविशेषमें दर्शनमोहनीय उपशान्त होकर अवस्थित रहता है उसे उपशामनाडा कहते हैं। उपशामनाया कहो या उपशम सम्यग्दृष्टिका काल कहो दोनोंका एक ही अर्थ है।
आगे इन तीन करणोंका विशेष विचार करते हुए अषःप्रवृत्तकरणके विषयमें दो अनुयोगद्वारोंका निज किया दो अनयोगदार है-अनकृष्टिप्ररूपणा और अल्पबहत्व । उसमें सर्वप्रथम बहुत्वके साधनरूपसे अनुकृष्टिका निर्देश किया है। अधःप्रवृत्तकरणका कुल काल अन्तर्मुहूर्त है और परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण है। उसमें प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समयतक पृथक-पृथक् एक-एक समयमें स्थितिबन्धापसरण आदिके कारणभूत और उत्तरोत्तर छह वृद्धिक्रमसे अवस्थित असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं। परिपाटी क्रमसे विरचित इन परिणामोंके पुनरुक्त और अपुनरुक्त भावका अनुसन्धान करना अनुकृष्टि कहलाती है। यद्यपि यह अनुकृष्टि संसारके योग्य स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानोंमें पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान ऊपर जाकर व्युच्छिन्न होती है, क्योंकि जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणामोंकी ऊपर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविशेषोंमें अनुवृत्ति देखी जाती है। किन्तु यहाँ ऐसा न होकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण अवस्थित स्थान व्यतीत होनेपर अनुकृष्टिका विच्छेद हो जाता है। यह अन्तर्मुहुर्तप्रमाण अवस्थित स्थान अध:प्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवें भागप्रमाण है। यथा-अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें नाना जीवोंकी अपेक्षा असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम होते हैं। पुनः दूसरे समयमें प्रारम्भके कुछ परिणामोंको छोड़कर वे ही परिणाम अन्य अपूर्व परिणामोंके साथ कुछ अधिक होते हैं। यहाँ अधिकका प्रमाण, असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थानों में अन्तर्मुहर्तका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे, उतना है। इसप्रकार अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयतक प्रत्येक समयके परिणाम पिछले समयके परिणामोंसे साधिक होते जाते हैं। आगे इन परिणामोंकी किस प्रकार अनुकृष्टि रचना बनती है आदि सब बातोंका विशेष खुलासा मूलमें विस्तारसे किया ही है। इसलिए वहाँसे जान लेना चाहिए। इसीप्रकार इन परिणामोंमें विशुद्धिकी अपेक्षा स्वस्थान और परस्थानका अवलम्बन लेकर अल्पबहत्व भी जान लेना चाहिए। विशद्धिकी अपेक्षा परस्थान अल्पबहत्वका संदष्टिद्वारा पृ० २५१ में स्पष्ट स्पष्टीकरण किया है, इसलिए इसे उसके आधारसे जान लेना चाहिए। यहां इतना संकेत कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त संदृष्टिमें विवक्षित किस स्थानसे दूसरे किस स्थानकी विशद्धि अधिक है यह बतलानेके लिए जो वाणके चिह्न दिये हैं वे भूलसे उलटे लग गये है, अतः उन्हें वहीं अपने अपने स्थानपर उलट देना चाहिए । ताकि परस्थान विशुद्धिके अल्पबहुत्वका ज्ञान करने में भ्रम न होने पाये।
दूसरा अपूर्वकरण है। इसका काल अन्तर्मुहूर्त है जो अधःप्रवृत्तकरणके कालसे संख्यातवें भागप्रमाण है। इसके प्रत्येक समयमें नानाजीवोंकी अपेक्षा असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम होते हैं जो प्रत्येक समयमें विसदृश ही होते हैं । अर्थात् प्रत्येक समयके परिणाम दूसरे समयके परिणामोंसे भिन्न ही होते हैं । यहाँ प्रथम समयमें जघन्य विशुद्धि सबसे स्तोक होती है। उससे उसी समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। प्रथम समयकी इस उत्कृष्ट विशुद्धिसे दूसरे समयको जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। उससे उसी समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। इसप्रकार विशुद्धिका यह अल्पबहुत्व इस करणके अन्तिम समयतक जानना चाहिए। यहाँ अधःप्रवृत्तकरणके समान परिणामोंकी अनुकृष्टि रचना न होनेसे निर्वर्गणाकाण्डक भी.