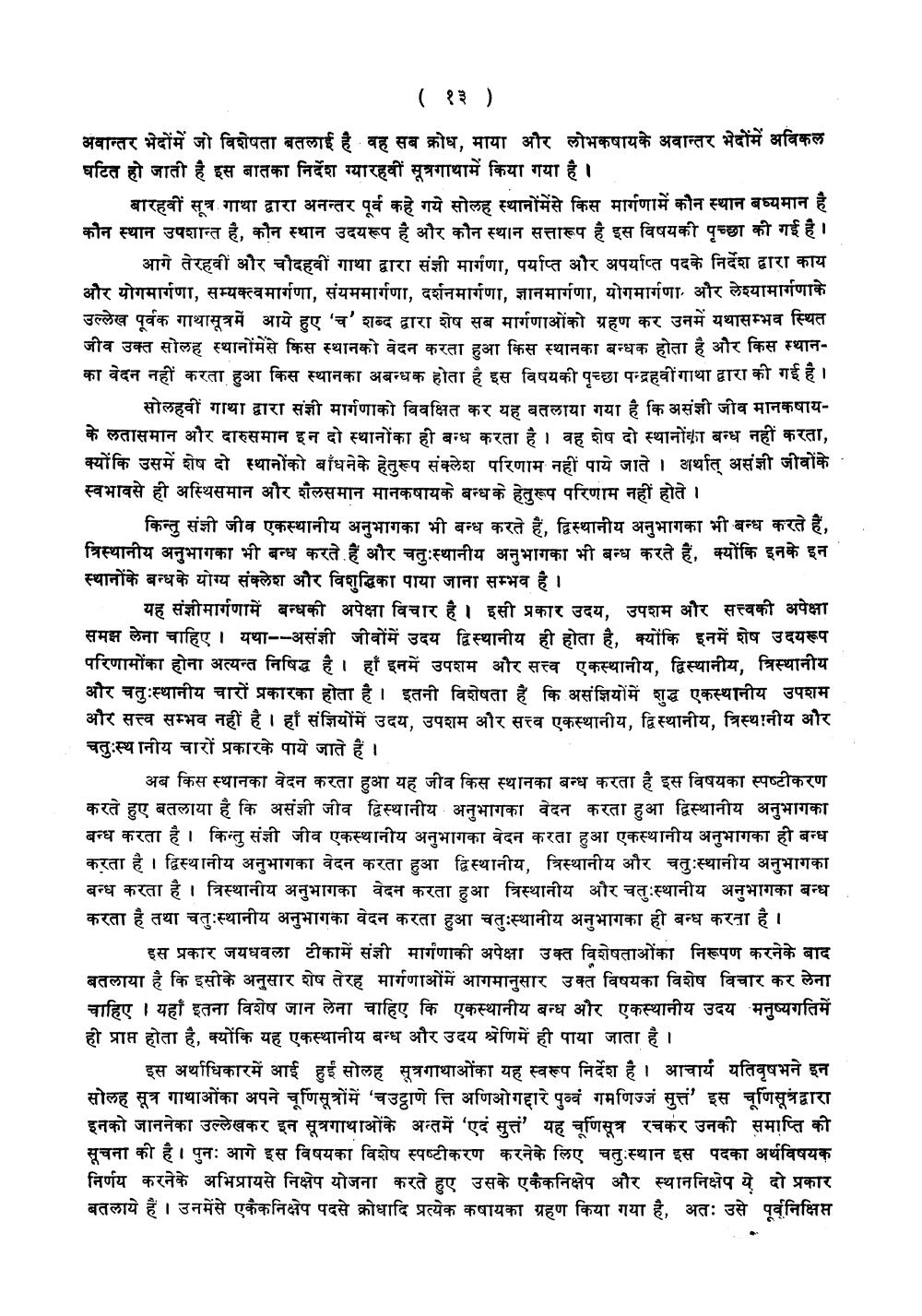________________
अवान्तर भेदोंमें जो विशेषता बतलाई है वह सब क्रोध, माया और लोभकषायके अवान्तर भेदोंमें अविकल घटित हो जाती है इस बातका निर्देश ग्यारहवीं सूत्रगाथामें किया गया है ।
__बारहवीं सूत्र गाथा द्वारा अनन्तर पूर्व कहे गये सोलह स्थानोंमेंसे किस मार्गणामें कौन स्थान बध्यमान है कौन स्थान उपशान्त है, कौन स्थान उदयरूप है और कौन स्थान सत्तारूप है इस विषयकी पृच्छा की गई है।
आगे तेरहवीं और चौदहवीं गाथा द्वारा संज्ञी मार्गणा, पर्याप्त और अपर्याप्त पदके निर्देश द्वारा काय और योगमार्गणा, सम्यक्त्वमार्गणा, संयममार्गणा, दर्शनमार्गणा, ज्ञानमार्गणा, योगमार्गणा. और लेश्यामार्गणाके उल्लेख पूर्वक गाथासूत्र में आये हए 'च' शब्द द्वारा शेष सब मार्गणाओंको ग्रहण कर उनमें यथासम्भव स्थित जीव उक्त सोलह स्थानोंमेंसे किस स्थानको वेदन करता हुआ किस स्थानका बन्धक होता है और किस स्थानका वेदन नहीं करता हुआ किस स्थानका अबन्धक होता है इस विषयकी पृच्छा पन्द्रहवीं गाथा द्वारा की गई है।
सोलहवीं गाथा द्वारा संज्ञी मार्गणाको विवक्षित कर यह बतलाया गया है कि असंज्ञी जीव मानकषायके लतासमान और दारुसमान इन दो स्थानोंका ही बन्ध करता है। वह शेष दो स्थानोंका बन्ध नहीं करता, क्योंकि उसमें शेष दो स्थानोंको बाँधनेके हेतुरूप संक्लेश परिणाम नहीं पाये जाते । अर्थात् असंज्ञी जीवोंके स्वभावसे ही अस्थिसमान और शैलसमान मानकषायके बन्ध के हेतुरूप परिणाम नहीं होते।
किन्तु संज्ञो जीव एकस्थानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं, द्विस्थानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं, त्रिस्थानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं और चतुःस्थानीय अनुभागका भी बन्ध करते हैं, क्योंकि इनके इन स्थानोंके बन्धके योग्य संक्लेश और विशुद्धिका पाया जाना सम्भव है।
यह संज्ञीमार्गणामें बन्धकी अपेक्षा विचार है। इसी प्रकार उदय, उपशम और सत्त्वकी अपेक्षा समझ लेना चाहिए। यथा--असंज्ञी जीवोंमें उदय द्विस्थानीय ही होता है, क्योंकि इनमें शेष उदयरूप परिणामोंका होना अत्यन्त निषिद्ध है। हाँ इनमें उपशम और सत्त्व एकस्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय चारों प्रकारका होता है। इतनी विशेषता है कि असंज्ञियोंमें शुद्ध एकस्थानीय उपशम और सत्त्व सम्भव नहीं है। हाँ संज्ञियोंमें उदय, उपशम और सत्त्व एकस्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय चारों प्रकारके पाये जाते हैं।
अब किस स्थानका वेदन करता हुआ यह जीव किस स्थानका बन्ध करता है इस विषयका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि असंज्ञी जीव द्विस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ द्विस्थानीय अनुभागका बन्ध करता है। किन्तु संज्ञी जीव एकस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ एकस्थानीय अनुभागका ही बन्ध करता है । द्विस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका बन्ध करता है । त्रिस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका बन्ध करता है तथा चतुःस्थानीय अनुभागका वेदन करता हुआ चतुःस्थानीय अनुभागका ही बन्ध करता है ।
इस प्रकार जयधवला टीकामें संज्ञी मागंणाकी अपेक्षा उक्त विशेषताओंका निरूपण करनेके बाद बतलाया है कि इसोके अनुसार शेष तेरह मार्गणाओंमें आगमानुसार उक्त विषयका विशेष विचार कर लेना चाहिए । यहाँ इतना विशेष जान लेना चाहिए कि एकस्थानीय बन्ध और एकस्थानीय उदय मनुष्यगतिमें ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह एकस्थानीय बन्ध और उदय श्रेणिमें ही पाया जाता है।
इस अर्थाधिकारमें आई हुईं सोलह सूत्रगाथाओंका यह स्वरूप निर्देश है। आचार्य यतिवृषभने इन सोलह सूत्र गाथाओंका अपने चूणिसूत्रोंमें 'चउदाणे त्ति अणिओगहारे पुव्वं गमणिज्ज सुत्तं' इस चूणिसूत्रद्वारा इनको जाननेका उल्लेखकर इन सूत्रगाथाओंके अन्तमें 'एदं सुत्तं' यह चूर्णिसूत्र रचकर उनकी समाप्ति की सूचना की है। पुनः आगे इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिए चतुःस्थान इस पदका अर्थविषयक निर्णय करनेके अभिप्रायसे निक्षेप योजना करते हुए उसके एककनिक्षेप और स्थाननिक्षेप ये दो प्रकार बतलाये हैं। उनमेंसे एकैकनिक्षेप पदसे क्रोधादि प्रत्येक कषायका ग्रहण किया गया है, अतः उसे पूर्वनिक्षिप्त