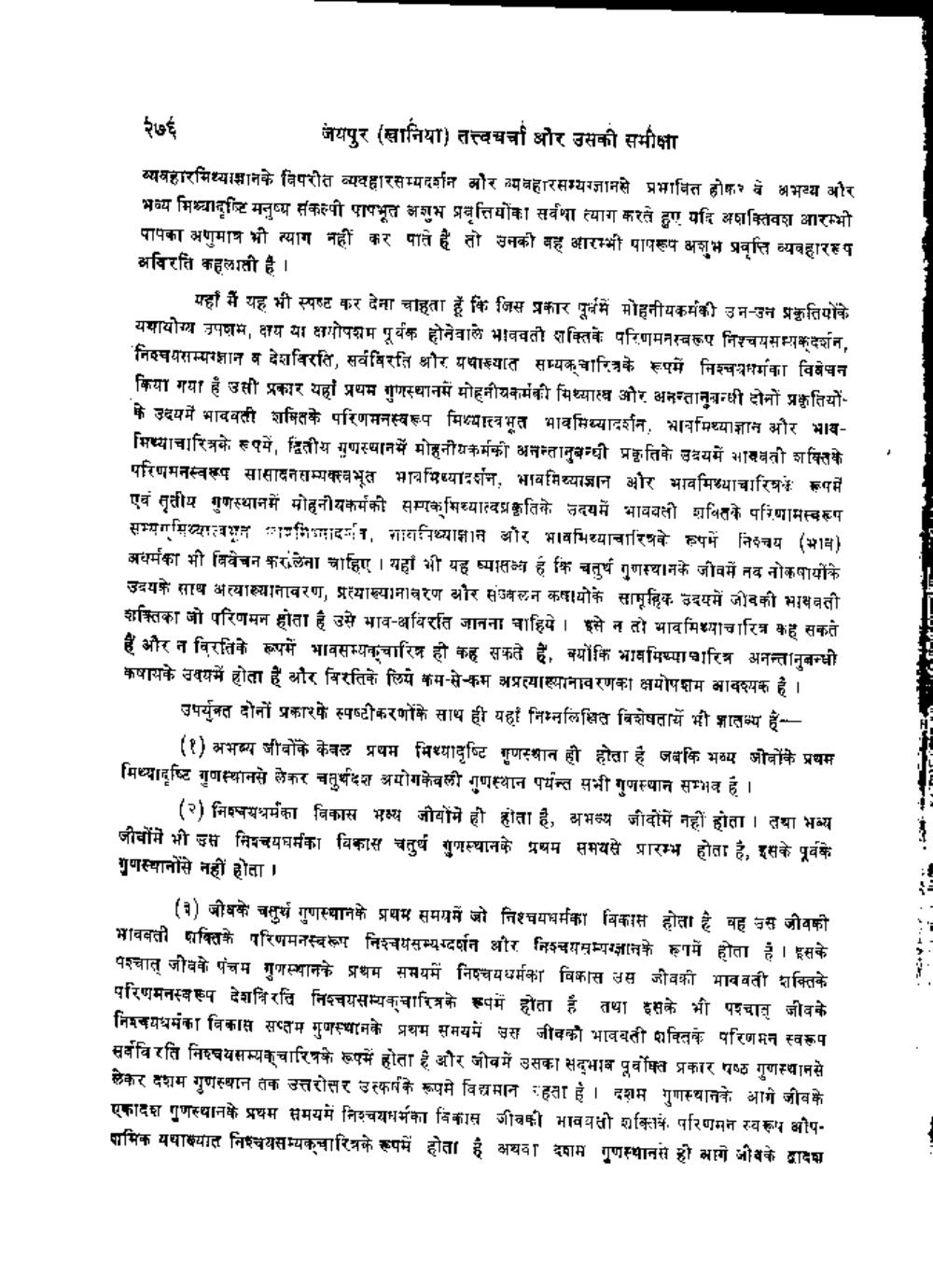________________
२७६
जयपुर (खानिया) तत्त्वचर्चा और उसकी समीक्षा
व्यवहार मिथ्याज्ञानके विपरीत व्यवहारसम्यदर्शन और व्यवहारसम्यग्जान से प्रभावित होकर वे अभय्य और भव्य मिध्यादृष्टि मनुष्य संकल्पी पापभूत अशुभ प्रवृत्तियोंका सर्वथा त्याग करते हुए यदि अस्तिवश आरम्भी पापका अणुमात्र भी त्याग नहीं कर पाते हैं तो उनकी वह आरम्भी पापरूप अशुभ प्रवृत्ति व्यवहाररूप अविरति कहलाती है ।
यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार पूर्व में मोहनीयकर्मकी उन उन प्रकृतियोंके यथायोग्य उपशम, क्षय या क्षयोपशम पूर्वक होनेवाले भाववती शक्ति के परिणमनस्वरूप निश्चयसम्यक्दर्शन, निश्चयसम्यग्ज्ञान व देशविरति सर्वविरति और यथास्यात सम्यक् चारित्र के रूपमें निश्चयधर्मका विवेचन किया गया है उसी प्रकार यहाँ प्रथम गुणस्थानमें मोहनीय कर्मको मिथ्यास्थ और अनन्तानुबन्धी दोनों प्रकृतियोंके उदयमें भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप मिध्यात्वभूत भाव मिथ्यादर्शन, भावमिथ्याज्ञान और भावमिथ्याचारित्रके रूपमें द्वितीय गुणस्थान में मोहनीय कर्मकी अनन्तानुबन्धी प्रकृतिके उदय में भावी शक्तिके परिणमनस्वरूप सासादन सम्पवस्व भूत भावमिध्यादर्शन, भावमिथ्याज्ञान और भावमिथ्याचारित्र के रूप में एवं तृतीय गुणस्थान में मोहनीयकर्म की सम्पक मिध्यात्वप्रकृति के उदय में भाववती शक्तिके परिणामस्वरूप सभ्यमिध्यात्वभूतादर्श सानिध्याज्ञान और भावभिथ्याचारित्र के रूपमें निश्चय (भाव)
धर्मका भी विवेचन करलेना चाहिए । यहाँ भी यह ष्यासभ्य है कि चतुर्थं गुणस्थानके जीव में नव नोकषायके उदयके साथ अत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संवलन कष्टायो के सामूहिक उदयमें जीवकी भागवती शक्तिका जो परिणमन होता है उसे भाव-अविरति जानना चाहिये। इसे न तो भावमिथ्याचारित्र कह सकते हैं और न विरतिके रूपमें भावसम्यक् चारित्र ही कह सकते हैं, क्योंकि भावमिष्पा शरित्र अनन्तानुबन्धी कषायके उदय होता है और विरतिके लिये कम-से-कम अप्रत्याख्यानावरणका क्षयोपशम आवश्यक है ।
उपर्युक्त दोनों प्रकार के स्पष्टीकरणोंके साथ ही यहां निम्नलिखित विशेषतायें भी ज्ञातव्य है(१) अभव्य जीवोंके केवल प्रथम मिध्यादृष्टि गुणस्थान हो होता है जबकि भव्य जीवोंके प्रथम मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर चतुर्थदेश अयोगकेवली गुणस्थान पर्यन्त सभी गुणस्थान सम्भव है ।
(२) निश्वश्रमका विकास भव्य जीयोंमें ही होता है, जीवोंमें भी उस निश्चयधर्मका विकास चतुर्थ गुणस्थान के प्रथम गुणस्थानोंसे नहीं होता ।
अभव्य जीवोंमें नहीं होता । तथा भव्य समय से प्रारम्भ होता है, इसके पूर्वके
(३) जीवके चतुर्थ गुणस्थान के प्रथम समय में जो निश्चयका विकास होता है वह उस जीवकी भाववती शक्ति परिणमनस्वरूप निश्चयसम्यग्दर्शन और निश्चयसम्यग्ज्ञानके रूपमें होता है। इसके पश्चात् जीवके पंचम गुणस्थानके प्रथम समय में निश्चयधर्मका विकास उस जीवको भाववती शक्तिके परिणमनस्वरूप देशविरति निश्चयसम्यक् चारित्रके रूपमें होता है तथा इसके भी पश्चात् जीवके निश्चयधर्मका विकास सप्तम गुणस्थान के प्रथम समय में उस जीवको भाववती शक्ति के परिणमन स्वरूप सर्वविरति निश्वयसम्यक् चारित्रके रूपमें होता है और जीव में उसका सद्भाव पूर्वोक्त प्रकार पष्ठ गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक उत्तरोसर उत्कर्ष के रूपमे विद्यमान रहता है। दशम गुणस्थानके आगे जीव के एकादश गुणस्थानके प्रथम समय में निश्चयधर्मका विकास जीवको भाववती शक्ति परिणमन स्वरूप औपपामिक यथास्यात निश्चयसम्यक्चारित्रके रूपमें होता है अथवा दशम गुणस्थानसे हो भागे जीवके द्वादश