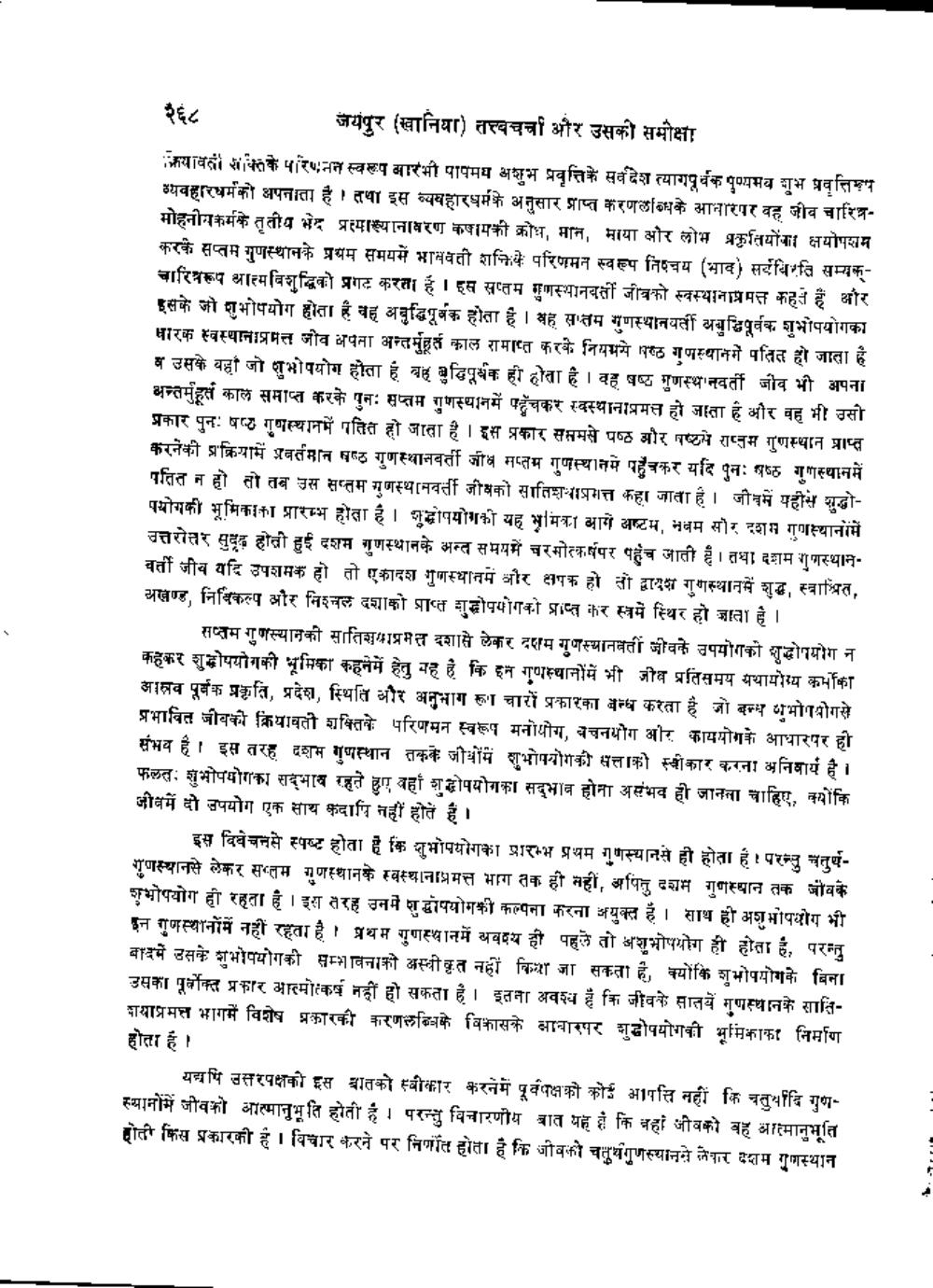________________
३६८
जयपुर (खानिया) तत्वचर्चा और उसकी समीक्षा
क्रियावती शक्तिके परिपनन स्वरूप बारंभी पापमय अशुभ प्रवृत्तिके सर्वदेश त्यागपूर्वक पुण्यभव शुभ प्रवृत्तिप व्यवहारधर्मको अपनाता है। तथा इस व्यवहारधर्मके अनुसार प्राप्त करणलब्धिके आधारपर वह जीव चारित्रमोहनीय कर्मके तृतीय भेद प्रत्याख्यानावरण कषायकी क्रोध, मान, माया और लोभ प्रकृतियोंजार क्षयोपशम करके सप्तम गुणस्थान के प्रथम समय में भाववती शक्ति के परिणमन स्वरूप निश्चय (भाव) सर्वविरति सम्यक्चारित्ररूप आत्मविशुद्धिको प्रगट करता है। इस सप्तम गुणस्थानवर्ती जीवको स्वस्थानाप्रमत्त कहते हैं और इसके जो शुभोपयोग होता है वह अबुद्धिपूर्वक होता है। वह सप्तम गुणस्थानवर्ती अबुद्धिपूर्वक शुभोपयोगका धारक स्वस्थानाप्रमत्त जीव अपना अन्तर्मुहूर्त काल रामाप्त करके नियम पष्ठ गुणस्थान में पतित हो जाता है अ उसके वहाँ जो शुभोपयोग होता है वह बुद्धिपूर्वक ही होता है। वह षष्ठ गुणस्थ' नवर्ती जीव भी अपना अन्तर्मुहूर्त काल समाप्त करके पुनः सप्तम गुणस्थान में पहुँचकर स्वस्थानाप्रमत्त हो जाता। प्रकार पुनः षष्ठ गुणस्थानमें पतित हो जाता है । इस प्रकार सप्तमसे पष्ठ और पष्ट राम गुणस्थान प्राप्त और वह भी उसी करने की प्रक्रियामें प्रवर्तमान षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीव सप्तम गुणस्थानमे पहुँचकर यदि पुनः श्रेष्ठ गुणस्थान में पतित न हो तो तब उस सप्तम गुणस्थानवर्ती जीवको सातिशयाप्रमत्त कहा जाता है। जीव में यहीसे शुद्धोपयोगकी भूमिकाका प्रारम्भ होता है। शुद्धोपयोग की यह भूमिका आगे अष्टम भवम सौर दशम गुणस्थानों में उत्तरोत्तर सुदृढ़ होती हुई दशम गुणस्थानके अन्त समय में चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाती है। तथा दशम गुणस्थानवर्ती जीव यदि उपशमक हो तो एकादश गुणस्थानमें और क्षपक हो तो द्वादश गुणस्थानमें शुद्ध स्वाश्रित, अखण्ड, निर्विकल्प और निश्चल दशाको प्राप्त शुद्धोपयोगको प्राप्त कर स्त्रमें स्थिर हो जाता है ।
सप्तम गुणस्यानकी सातिशयाश्रमत्त दशासे लेकर दशम गुणस्थानवतीं जीवके उपयोगको शुद्धोपयोग न कहकर शुद्धोपयोग की भूमिका कहने में हेतु यह है कि इन गुणस्थानों में भी जीव प्रतिसमय यथायोग्य कर्मका आस्रव पूर्वक प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग रूप चारों प्रकारका बन्ध करता है जो बन्ध भोग प्रभावित जीवको क्रियावती शक्तिके परिणमन स्वरूप मनोयोग, वचनयोग और काययोग के आधारपर संभव है। इस तरह दशम गुणस्थान तकके जीवोंमें शुभपयोगको सत्ताको स्वीकार करना अनिवार्य है । फलतः शुभोपयोगका सद्भाव रहते हुए वहाँ शुद्धोपयोगका सद्भाव होना असंभव ही जानना चाहिए, क्योंकि जीव में दो उपयोग एक साथ कदापि नहीं होते हैं ।
इस विवेचनसे स्पष्ट होता है कि शुभोपयोगका प्रारम्भ प्रथम गुणस्थान से ही होता है। परन्तु चतुर्थगुणस्थानसे लेकर सन्लम गुणस्थानके स्वस्थानाप्रमत्त भाग तक ही नहीं, अपितु दशम गुणस्थान तक जीवके शुभोपयोग ही रहता है । इस तरह उनमें शुद्धोपयोगी कल्पना करना अयुक्त है। साथ ही अनुपयोग भी इन गुणस्थानोंमें नहीं रहता है। प्रथम गुणस्थान में अवश्य ही पहले तो अशुभोपयोग ही होता है, परन्तु बाद उसके शुभपयोगकी सम्भावनाको अस्वीकृत नहीं किया जा सकता उसका पूर्वोक्त प्रकार आत्मोत्कर्ष नहीं हो सकता है। इतना अवश्य है कि जीवके सातवें गुणस्थानके सातिक्योंकि शुभोपयोग के बिना पायाप्रमत्त भागमें विशेष प्रकारको करणलनिके विकासके आवापर शुद्धोपयोग की भूमिकाका निर्माण होता है ।
यद्यपि उतरपक्षको इस बातको स्वीकार करने में पूर्वपक्षको कोई आपत्ति नहीं कि चतुर्यादि गुणस्थानोंमें जीवको आत्मानुभूति होती है । परन्तु विचारणीय बात यह है कि वहाँ जीवको वह आत्मानुभूति होती किस प्रकारकी हुँ । विचार करने पर निशांत होता है कि जीवको चतुर्थगुणस्थानने लेकर दशम गुणस्थान