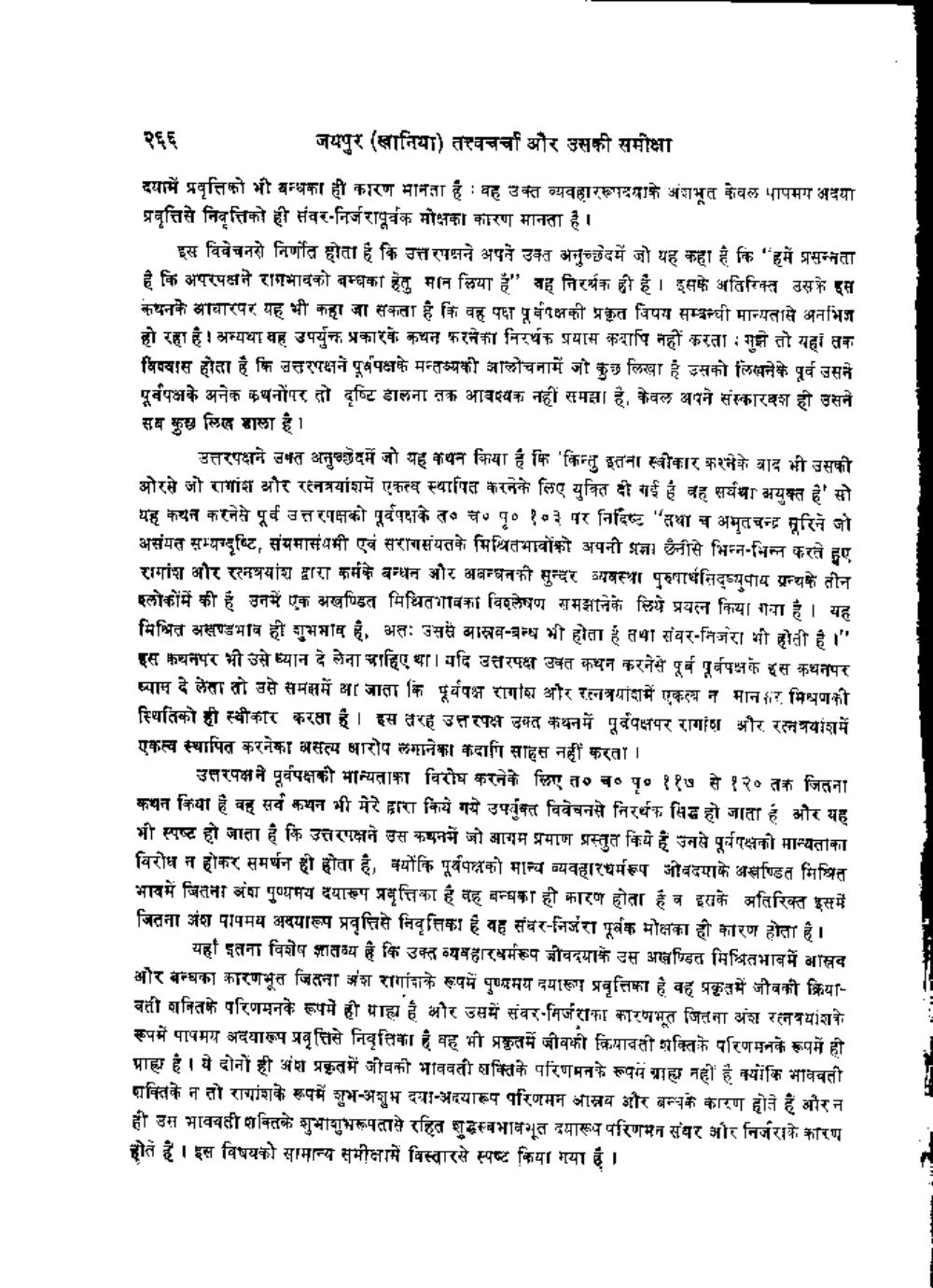________________
२६६
जयपुर (खानिया) तत्वचर्चा और उसकी समीक्षा
दामें प्रवृत्तिको भी बन्धका ही कारण मानता है वह उक्त व्यवहाररूपदा अंशभूत केवल पापमय अदया प्रवृत्ति से निवृत्तिको ही संवर-निर्जरापूर्वक मोक्षका कारण मानता है ।
1
इस विवेचनसे निर्णीत होता है कि उत्तरपक्षने अपने उक्त अनुच्छेद में जो यह कहा है कि हमें प्रसन्नता है कि अपरपक्ष ने रागभावको बम्धका हेतु मान लिया है" वह निरर्थक ही हैं। इसके अतिरिक्त उसके इस कंचनके आधारपर यह भी कहा जा सकता है कि वह पक्ष पूर्वरक्षक प्रकृत विषय सम्बन्धी मान्यता से अनभिज हो रहा है । अभ्यथा वह उपर्युक्त प्रकार के कथन करनेका निरर्थक प्रयास कदापि नहीं करता मुझे तो यहाँ तक विवास होता है कि उत्तरपक्षने पूर्वपक्ष के मन्तव्यकी आलोचनामें जो कुछ लिखा है उसको लिखनेके पूर्व उसने पूर्वपक्ष के अनेक कथनों पर तो दृष्टि डालना तक आवश्यक नहीं समझा है, केवल अपने संस्कारवश ही उसने सब कुछ लिख डाला है ।
उत्तरपक्षने उक्त अनुच्छेद में जो यह कथन किया है कि 'किन्तु इतना स्वीकार करने के बाद भी उसकी ओरसे जो रागांश और रत्नत्रयांशमें एकत्व स्थापित करनेके लिए युक्ति दी गई है वह सर्वथा अयुक्त है' सो यह कथन करने से पूर्व उत्तरपक्षको पूर्वपक्षके त० च० पृ० १०३ पर निर्दिष्ट " तथा च अमृतचन्द्र सूरिने जो असंयत स॒भ्यग्दृष्टि, संयमासंयमी एवं सरागसंयत के मिश्रितभावोंको अपनी अज्ञानीसे भिन्न-भिन्न करते हुए शमांश और रत्नत्रयांश द्वारा कर्मके बन्धन और अवन्धनकी सुन्दर व्यवस्था पुरुषार्थनिष्युपाय प्रत्यके तीन श्लोकों की है उनमें एक अखण्डित मिथितभावका विश्लेषण समझाने के लिये प्रयत्न किया गया है। यह मिश्रित अखण्डभाव ही शुभभाव है, अतः उससे मात्र बन्ध भी होता है तथा संवर- निर्जरा भी होती है।" इस कथनपर भी उसे ध्यान दे लेना चाहिए था। यदि उत्तरपक्ष उक्त कथन करनेसे पूर्व पूर्वपक्ष के इस कथनपर ध्यान दे लेता तो उसे समझ में आ जाता कि पूर्वपक्ष रागोश और रत्नत्रयांमें एकल्य न मानकर मिश्रणकी स्थितिको ही स्वीकार करता है। इस तरह उत्तरपक्ष उक्त कथन में पूर्वपक्षपर रागांश और रत्नत्रयांश में एकस्व स्थापित करनेका असत्य आरोप लगाने का कदापि साहस नहीं करता ।
उतरपक्ष ने पूर्वपक्षको मान्यताका विरोध करने के लिए त० ० पृ० ११७ से १२० तक जितना कथन किया है वह सर्व कथन भी मेरे द्वारा किये गये उपर्युक्त विवेचनसे निरर्थक सिद्ध हो जाता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरपक्षने उस कथन में जो आगम प्रमाण प्रस्तुत किये हैं उनसे पूर्व पक्षको मान्यताका विरोध न होकर समर्थन ही होता है, क्योंकि पूर्वपक्षको मान्य व्यवहारथर्मरूप जीवदया के अखण्डित मिश्रित भाव में जितना अंश पुण्यमय दयारूप प्रवृत्तिका है वह बन्धका ही कारण होता है व इसके अतिरिक्त इसमें जितना अंश पापमय अवयारूप प्रवृत्तिसे निवृत्तिका है वह संचर- निर्जरा पूर्वक मोक्षका ही कारण होता है ।
यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि उक्त व्यवहारधर्मरूप जीवदया उस अखण्डित मिश्रित भाव में आसव और बन्धका कारणभूत जितना अंश गांवाके रूपमें पुण्यमय दयारूप प्रवृत्तिका है वह प्रकृतमें जीवकी क्रियाबत्ती शक्तिके परिणमनके रूपमें ही ग्राह्य है और उसमें संवर मिर्जराका कारणभूत जितना अंश रत्नत्रयांश रूपमें पापमय अदयारूप प्रवृत्तिसे निवृत्तिका है वह भी प्रकृत में जीवक क्रियावती शक्ति के परिणमनके रूपमें हो प्राह्य है । ये दोनों ही अंश प्रकृत में जीवकी भाववती शक्ति के परिणमन के रूपयं ग्राह्य नहीं है क्योंकि भाववती शक्ति न तो रागांश के रूपमें शुभ-अशुभ दया- अदयारूप परिणमन आनाव और बम्बके कारण होते हैं और न ही उस भाववती शक्तिके शुभाशुभरूपता से रहित शुद्धस्वभावभूत दयारूप परिणम संघर और निर्जरा के कारण होते हैं । इस विषयको सामान्य समीक्षामें विस्तार से स्पष्ट किया गया है ।