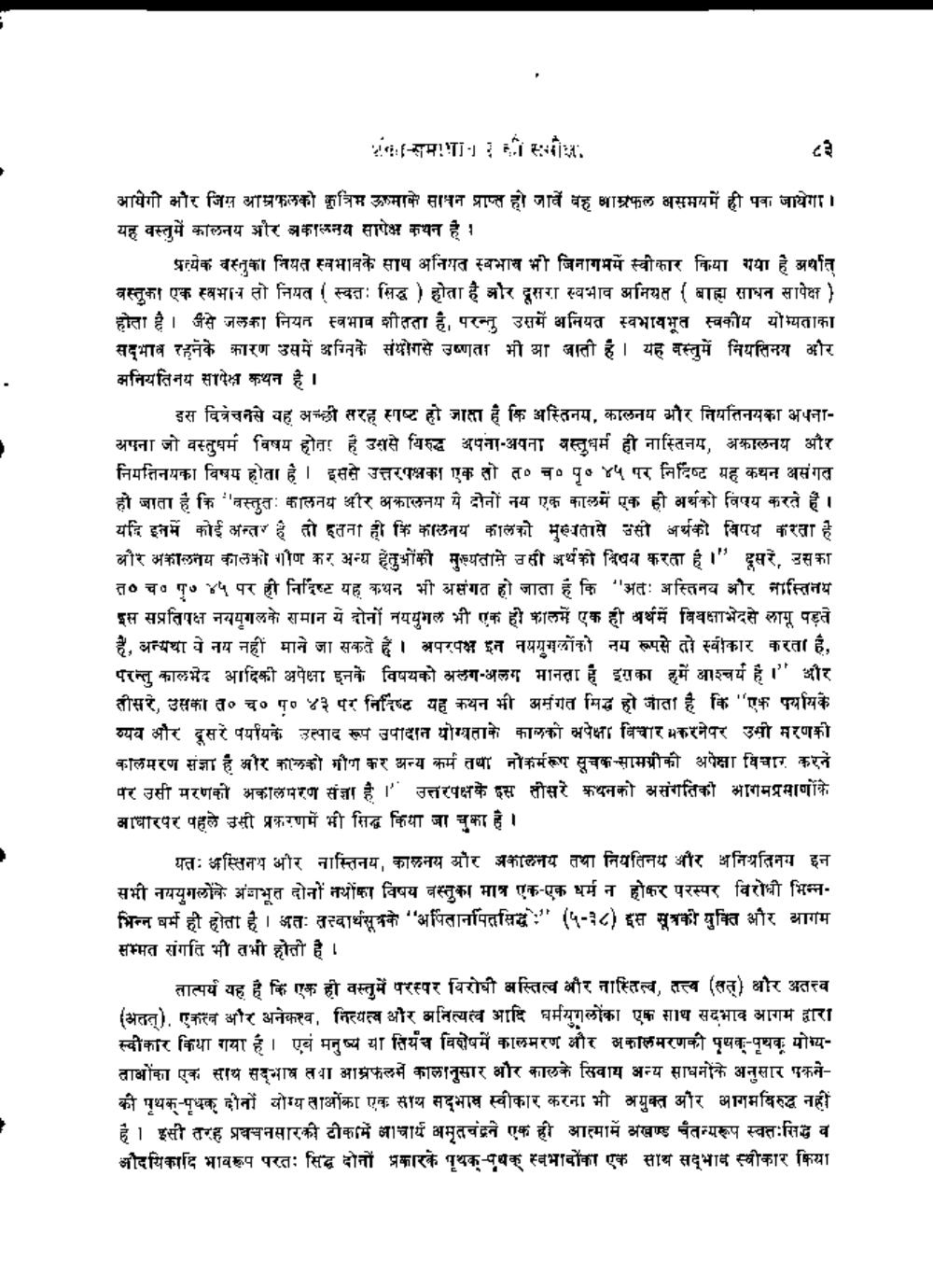________________
-समाभासपीः
आयेगी और जिस आम्रफलको कृत्रिम ऊष्माके साधन प्राप्त हो जावें वह भाम्रफल असमयमें ही पका जायेगा। यह वस्तुमें कालनय और अकालनय सापेक्ष कथन है।
प्रत्येक वस्तुका नियत स्वभावके साथ अनियत स्वभाव भी जिनागममें स्वीकार किया गया है अर्थात् वस्तुका एक स्वभाव तो नियत ( स्वतः सिद्ध होता है और दूसरा स्वभाव अमियप्त (बाह्म साधन सापेक्ष ) होता है। जैसे जलका नियत स्वभाव शीतता है, परन्तु उसमें अनियत स्वभावभूत स्वकीय योग्यताका सदभाव रहनके कारण उसमें अग्नि के संयोगसे उष्णता भी आ जाती है। यह वस्तुमें नियतिमय और अनियतिनय सापेक्ष कथन है।
इस वित्रचनसे वह अच्छी सरह साष्ट हो जाता है कि अस्तिनम, कालनय और नियतिनयका अपनाअपना जो वस्तुधर्म विषय होता है उससे विरुद्ध अपना-अपना यस्तुधर्म ही नास्तिनम, अकालनय और नियत्तिनयका विषय होता है | इससे उत्तरपक्षका एक तो त० च. पृ० ४५ पर निर्दिष्ट यह कथन असंगत हो जाता है कि 'वस्तुतः कालनय और अकालनय ये दोनों नय एक कालमें एक ही अर्थको विषय करते हैं । यदि इनमें कोई अन्तर है तो इतना ही कि कालनय कालको मुख्यतासे उसी अर्थको विषय करता है
और अकालनय कालको गौण कर अन्य हेतुओंको मुल्यतामे उसी अर्थको विषय करता है।" दूसरे, उसका त० च० पु. ४५ पर ही निर्दिष्ट यह कथन भी असंगत हो जाता है कि "अतः अस्तिनव और नास्तिनय इस सप्रतिपक्ष नययुगल के समान ये दोनों नययुगल भी एक ही कालमें एक ही अर्थ में विवक्षाभेदसे लागू पड़ते है, अन्यथा वे नय नहीं माने जा सकते हैं। अपरपक्ष इन नययुगलोंको नय रूपसे तो स्वीकार करता है, परन्तु कालभेद आदिकी अपेक्षा इनके विषयको अलग-अलग मानता है इसका हमें आश्चर्य है।" और तीसरे, उसका त० च० प० ४३ पर निर्दिष्ट यह कथन भी अमंगत सिद्ध हो जाता है कि "एक पर्यायके व्यय और दूसरे पर्यायके उत्पाद रूप उपादान योग्यताके कालको अपेक्षा विचार करनेपर उमी मरणकी कालमरण संज्ञा है और कालको गौण कर अन्य कर्म तथा नोकर्मरूप सूचक सामग्रीकी अपेक्षा विचार करने पर उसी मरणको अकालमरण संज्ञा है। उत्तरपक्षके इस तीसरे कथनको असंगतिको आगमप्रमाणोंके आधारपर पहले उसी प्रकरणमें भी सिद्ध किया जा चुका है।
यतः अस्तिनथ और नास्तिनय, कालनय और अकालनय तथा नियतिनय और अनियतिनय इन सभी नययुगलोंके अंगभूत दोनों नयोंका विषय वस्तुका मात्र एक-एक धर्म न होकर परस्पर विरोधी भिन्नभिन्न धर्म ही होता है । अतः तत्वार्थसूत्रके "अर्पितापितसिद्धः" (५-३८) इस सूत्रकी युक्ति और आगम सम्मत संगति भी तभी होती है।
तात्पर्य यह है कि एक ही वस्तुमें परस्पर विरोधी अस्तित्व और नास्तित्व, तत्त्व (सत्) और अतत्व (अतत). एकरन और अनेकश्व, नित्यत्व और अनित्यत्व आदि धर्मयुगलोंका एक साथ सदभाव आगम द्वारा स्वीकार किया गया है। एवं मनुष्य या तियच विशेषमें कालमरण और अकालमरणकी पृथक-पृथक योग्यताओंका एक साथ सद्भाव तथा आम्रफलमें कालानुसार और कालके सिवाय अन्य साधनोंके अनुसार पकनेकी पृथक्-पृथक दोनों योग्य ताओंका एक साथ सद्भाव स्वीकार करना भी अयुक्त और आगमविरुद्ध नहीं है। इसी तरह प्रवचनसारकी टीकामें आचार्य अमृतचंद्रने एक ही आत्मामें अखण्ड चैतन्यरूप स्वतःसिद्ध व औदयिकादि भावरूप परतः सिद्ध दोनों प्रकारके पृथक्-पृथक् स्वभावोंका एक साथ सद्भाव स्वीकार किया