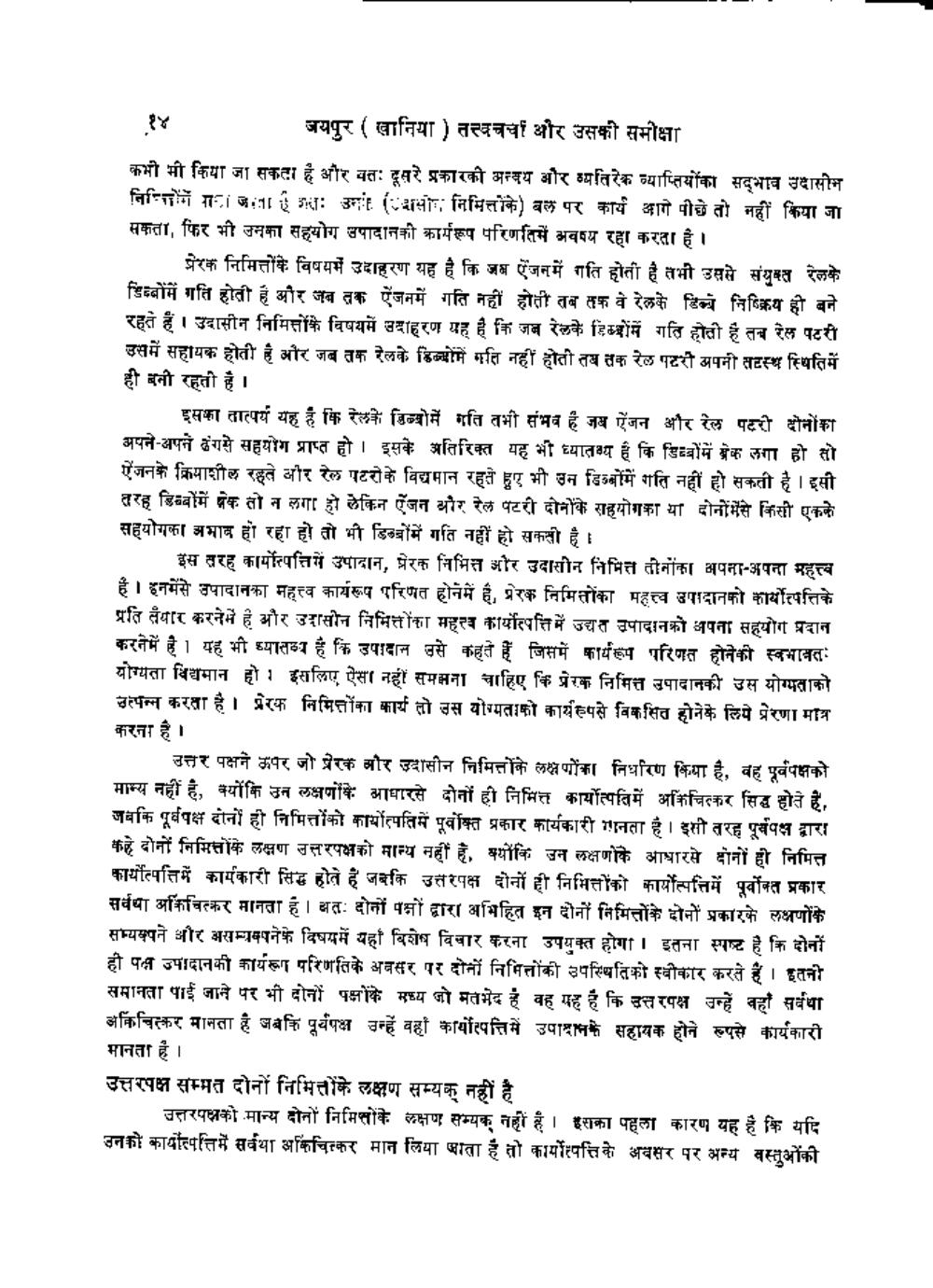________________
जयपुर ( खानिया) तत्वचर्चा और उसकी समीक्षा कभी भी किया जा सकता है और वतः दूसरे प्रकारको अन्क्य और व्यतिरेक व्याप्तियोंका सद्भाव उदासीन निषिोंगें पा जाता है अतः उन असो निमित्तोंके) बल पर कार्य आगे पीछे तो नहीं किया जा सकता, फिर भी उनका सहयोग उपादानको कार्यरूप परिणतिमें अवषय रहा करता है।
प्रेरक निमित्तोंके विषयमें उदाहरण यह है कि जब ऐजनमें गति होती है तभी उससे संयुक्त रेलके खिदबोंमें गति होती है और जब तक ऐंजनमें गति नहीं होती तब तक वे रेलके डिब्बे निष्क्रिय ही बने रहते हैं। उदासीन निमित्तोंके विषयमें उदाहरण यह है कि जब रेलके हिम्छोंमें गति होती है तब रेल पटरी उसमें सहायक होती है और जब तक रेलके डिब्बोंमें मति नहीं होती तब तक रेल पटरी अपनी तटस्थ स्थितिमें ही बनी रहती है।
इसका तात्पर्य यह है कि रेल के डिब्बोमें गति तभी संभव है जब ऐंजन और रेल पटरी दोनोंका अपने-अपने ढंगसे सहयोग प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यातव्य है कि डिब्बोंमें ब्रेक लगा हो सो ऐंजनके क्रियाशील रहते और रेल पटरो के विद्यमान रहते हुए भी उन डिब्बोंमें गति नहीं हो सकती है । इसी तरह डिब्बों में अंक तो न लगा हो लेकिन ऐंजन और रेल पटरी दोनोंके सहयोगका या दोनों से किसी एकके सहयोगका अभाव हो रहा हो तो भी डिब्बोंमें गति नहीं हो सकती है।
इस तरह कार्योत्पत्ति में उपादान, प्रेरक निभित्त और उदासीन निमित्त तीनोंका अपना-अपना महत्त्व हैं। इनमेंसे उपादानका महत्त्व कार्यरूप परिणत होने में है, प्रेरक निमित्तोंका महत्त्व उपादानको कार्योत्पत्तिके प्रति तैयार करने में है और उदासीन निमित्तोंका महत्व कार्योत्पत्ति में उद्यत उपादानको अपना सहयोग प्रदान करने में है। यह भी ध्यातव्य है कि उपादान उसे कहते हैं जिसमें कार्यरूप परिणत होनेकी स्वभावतः योग्यता विद्यमान हो। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रेरक निमित्त उपादानकी उस योग्यताको
न करता है। प्रेरक निमित्तोंका कार्य लो उस योग्यताको कार्यरुपसे विकसित होने के लिये प्रेरणा मात्र करना है।
उत्तर पक्षने ऊपर जो प्रेरक और उदासीन निमित्तोंके लक्षणोंका निर्धारण किया है, वह पूर्वपक्षको मान्य नहीं है, क्योंकि उन लक्षणों के आधारसे दोनों ही निमित्त कार्योत्पतिमें अकिंचित्कर सिद्ध होते है, जबकि पूर्वपक्ष दोनों ही निमित्तोंको कार्योत्पतिमें पूर्वोक्त प्रकार कार्यकारी मानता है। इसी तरह पूर्वपक्ष द्वारा कहे दोनों निमित्तोंके लक्षण उत्तरपक्षको मान्य नहीं है, क्योंकि उन लक्षणोके आधारसे दोनों ही निमित्त कार्योत्पत्ति में कार्यकारी सिद्ध होते हैं जबकि उत्तरपक्ष दोनों ही निमित्तोंको कार्योत्पत्तिमें पूर्वोक्त प्रकार सर्वथा अकिचित्कर मानता है। अतः दोनों पक्षों द्वारा अभिहित इन दोनों निमित्तोंके दोनों प्रकारके लक्षणों के सम्यक्पने और असम्यक्पनेके विषय में यहाँ विशेष विचार करना उपयुक्त होगा। इतना स्पष्ट है कि दोनों ही पक्ष उपादानकी कार्यरूप परिणतिके अवसर पर दोनों निमित्तोंकी उपस्थितिको स्वीकार करते हैं। इतनी समानता पाई जाने पर भी दोनों पक्षोंके मध्य जो मतभेद है वह यह है कि उत्तरपक्ष उन्हें वहाँ सर्वथा अकिंचितर मानता है जबकि पूर्वपक्ष उन्हें वहाँ कार्योत्पत्तिमें उपादानके सहायक होने रूपसे कार्यकारी मानता है। उत्तरपक्ष सम्मत दोनों निमित्तोंके लक्षण सम्यक नहीं है
उत्तरपक्षको मान्य दोनों निमितोंके लक्षण सम्यक नहीं है। इसका पहला कारण यह है कि यदि उनको कार्यात्पत्तिमें सर्वथा अकिचित्कर मान लिया जाता है तो कार्योत्पत्ति के अवसर पर अन्य वस्तुओंकी