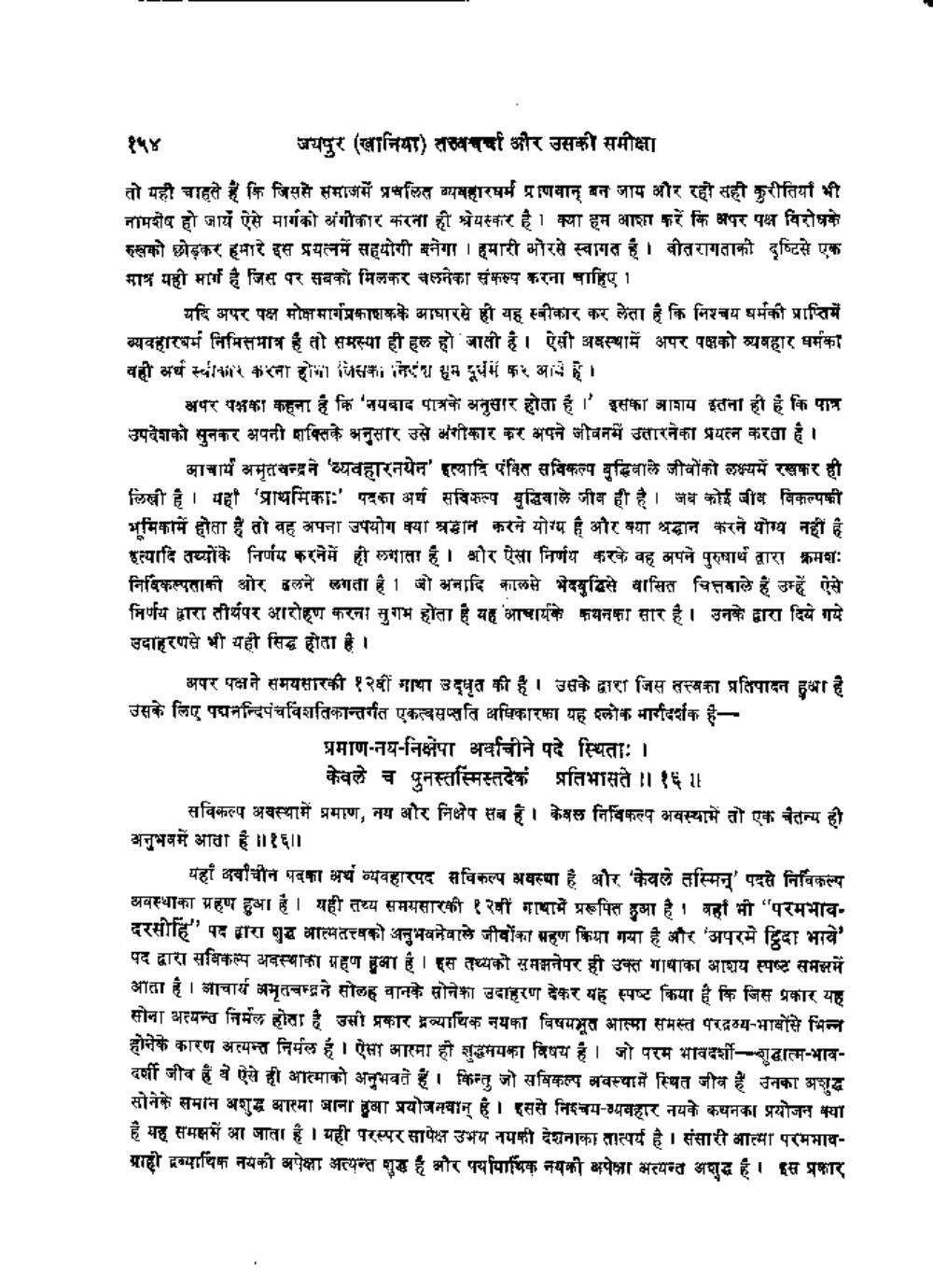________________
१५४
जयपुर (खानिया) तस्वचर्चा और उसकी समीक्षा
तो यही चाहते हैं कि जिससे समाज में प्रचलित व्यवहारधर्म प्राणवान् बन जाय और रहो सही कुरीतियाँ भी नामशेष हो जायें ऐसे मार्गको अंगीकार करना हो श्रेयस्कर है। क्या हम आशा करें कि अपर पक्ष विरोधके रुखको छोड़कर हमारे इस प्रयत्न में सहयोगी बनेगा । हमारी ओरसे स्वागत है । वीतरागताकी दृष्टिसे एक मात्र ही मार्ग है जिस पर सबको मिलकर चलनेका संकरूप करना चाहिए ।
यदि अपर पक्ष मोक्षमार्गप्रकाशक के आधार से ही यह स्वीकार कर लेता हूँ कि निश्चय धर्मकी प्राप्ति में व्यवहारधर्म निमितमात्र है तो समस्या ही हल हो जाती है। ऐसी अवस्थामें अपर पक्षको व्यवहार धर्मका वही अर्थ स्वीकार करना होगा जिसका निदेशक है।
अपर पक्षका कहना है कि 'नयवाद पात्र के अनुसार होता है।' इसका आशय इतना ही हैं कि पात्र सुनकर अपनी शक्तिके अनुसार उसे अंगीकार कर अपने जीवनमें उतारनेका प्रयत्न करता है ।
उपदेशको
आचार्य अमृतचन्द्र ने 'व्यवहारनयेन' इत्यादि पंक्ति सविकल्प बुद्धिवाले जीवोंको लक्ष्यमें रखकर ही लिखी है। यहाँ 'प्राथमिका:' पदका अर्थ सविकल्प बुद्धिवाले जीव ही है। जब कोई जीव विकल्पकी भूमिका होता है तो वह अपना उपयोग क्या श्रद्धान करने योग्य हूँ और क्या श्रद्धान करने योग्य नहीं है इत्यादि तथ्योंके निर्णय करने में हो लगाता है। और ऐसा निर्णय करके वह अपने पुरुषार्थं द्वारा क्रमशः fafeकल्पताnt ओर ढलने लगता है । जो अनादि कालसे भेदबुद्धिसे वासित चित्तवाले हैं उन्हें ऐसे निर्णय द्वारा तीर्थपर आरोहण करना सुगम होता है यह आचार्यके कथनका सार है। उनके द्वारा दिये गये उदाहरण भी यही सिद्ध होता है ।
अपर पक्षने समयसारकी १२वीं गाथा उद्धृत की है। उसके द्वारा जिस तत्त्वका प्रतिपादन हुआ है। उसके लिए पद्मनन्दिपंचविंशतिकान्तर्गत एकत्वसप्तति अधिकारका यह श्लोक मार्गदर्शक हैप्रमाण -नय-निक्षेपा अर्वाचीने पदे स्थिताः ।
केवले च पुनस्तस्मिस्तदेकं प्रतिभासते ॥ १६ ॥
सविकल्प अवस्था में प्रमाण, नय और निक्षेप सब है। केवल निर्विकल्प अवस्थामें तो एक चैतन्य ही अनुभव में आता है ॥ १६॥
यहाँ अचीन पदका अर्थ व्यवहारपद सविकल्प अवस्था है और 'केवले तस्मिन् पदसे निर्विकल्प व्यवस्थाका ग्रहण हुआ है। यही तथ्य समयसारकी १२वीं गाथामें प्ररूपित हुआ है । वहाँ भी "परमभावदरसीहिं" पद द्वारा शुद्ध आत्मतत्त्वको अनुभवनेवाले जीवोंका महण किया गया है और 'अपरमे द्विदा भावे' पद द्वारा सविकल्प अवस्थाका ग्रहण हुआ है। इस तथ्य को समझनेपर ही उक्त गाथाका आशय स्पष्ट समझमें आता है। आचार्य अमृतचन्द्रने सोलह वानके सोनेका उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार यह सोना अत्यन्त निर्मल होता है उसी प्रकार द्रव्याथिक नयका विषयभूत आत्मा समस्त परद्रव्य भावोंसे भिन्न होनेके कारण अत्यन्त निर्मल है। ऐसा आत्मा हो शुद्धका विषय है। जो परम भावदर्शी - शुद्धात्म-भावदर्शी जीव हैं ये ऐसे ही आत्माको अनुभवते हैं । किन्तु जो सविकल्प अवस्था में स्थित जीव हैं उनका अशुद्ध सोने के समान अशुद्ध व्यारमा जाना हुआ प्रयोजनवान् है । इससे निश्चय व्यवहार नयके कथनका प्रयोजन क्या है यह समझ में आ जाता है । यही परस्पर सापेक्ष उभय नमकी देशनाका तात्पर्य है । संसारी आत्मा परमभावग्राही कि नयकी अपेक्षा अत्यन्त शुद्ध है और पर्यायार्थिक नयको अपेक्षा अत्यन्त अशुद्ध है। इस प्रकार