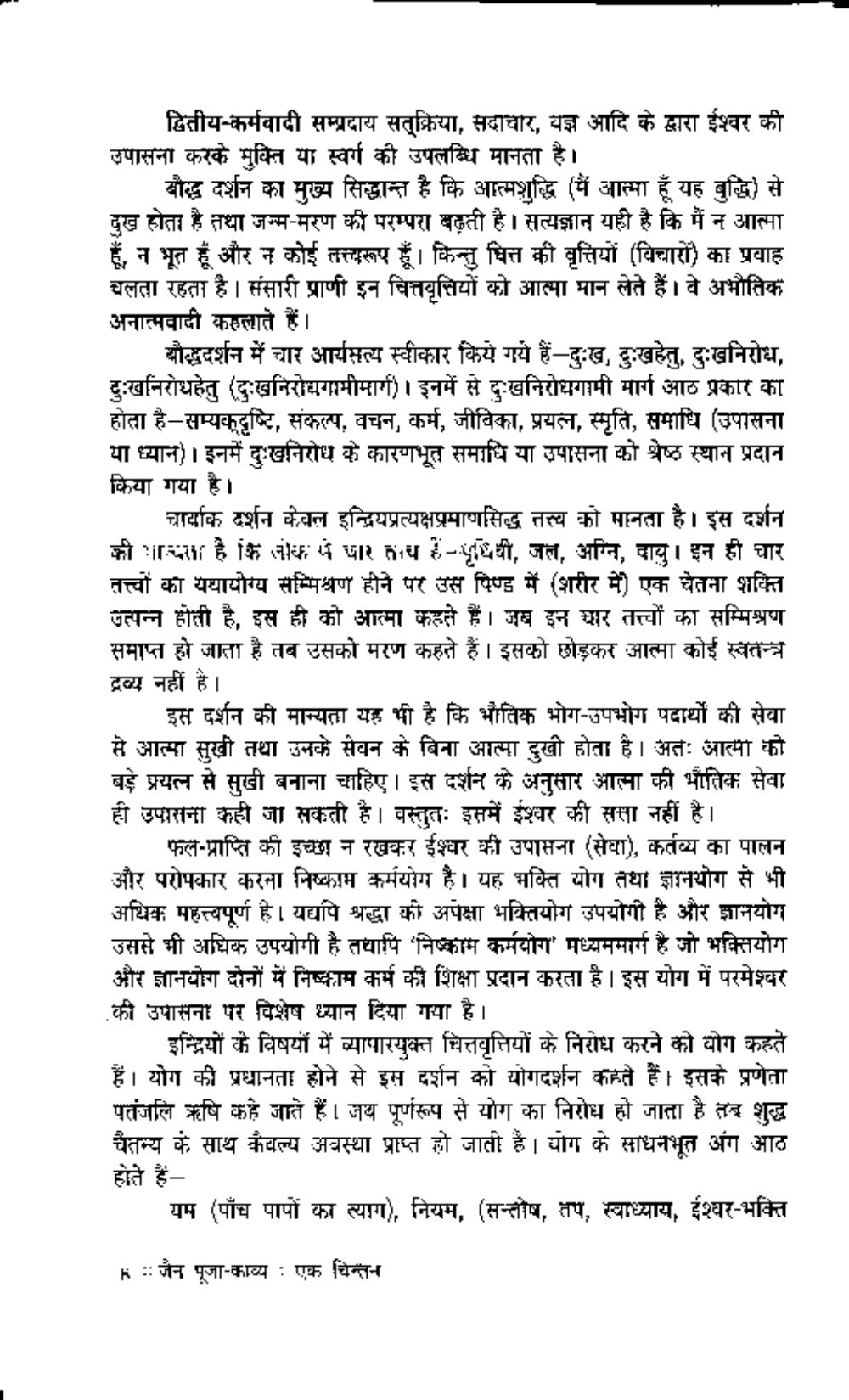________________
द्वितीय- कर्मवादी सम्प्रदाय सत्क्रिया, सदाचार, यज्ञ आदि के द्वारा ईश्वर की उपासना करके मुक्ति या स्वर्ग की उपलब्धि मानता है।
बौद्ध दर्शन का मुख्य सिद्धान्त है कि आत्मशुद्धि (मैं आत्मा हूँ यह बुद्धि) से दुख होता है तथा जन्म-मरण की परम्परा बढ़ती है। सत्यज्ञान यही है कि मैं न आत्मा हूँ, न भूत हूँ और न कोई तस्वरूप हूँ। किन्तु चित्त की वृत्तियों (विचारों) का प्रवाह चलता रहता है । संसारी प्राणी इन चित्तवृत्तियों को आत्मा मान लेते हैं। वे अभौतिक अनात्मवादी कहलाते हैं।
बौद्धदर्शन में चार आर्यसत्य स्वीकार किये गये हैं-दुःख, दुःखहेतु, दुःखनिरोध, दुःखनिरोधहेतु (दुःखनिरोगामीमार्ग) । इनमें से दुःखनिरोधगामी मार्ग आठ प्रकार का होता है - सम्यकदृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, जीविका, प्रयत्न, स्मृति, समाधि (उपासना या ध्यान) । इनमें दुःखनिरोध के कारणभूत समाधि या उपासना को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है।
चार्वाक दर्शन केवल इन्द्रियप्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध तत्त्व को मानता है । इस दर्शन की है कि लोक में चारता है - पृथिवी, जल, अग्नि, वावु । इन ही चार तत्त्वों का यथायोग्य सम्मिश्रण होने पर उस पिण्ड में (शरीर में) एक चेतना शक्ति उत्पन्न होती है, इस ही को आत्मा कहते हैं। जब इन चार तत्त्वों का सम्मिश्रण समाप्त हो जाता है तब उसको मरण कहते हैं। इसको छोड़कर आत्मा कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है।
इस दर्शन की मान्यता यह भी है कि भौतिक भोग-उपभोग पदार्थों की सेवा से आत्मा सुखी तथा उनके सेवन के बिना आत्मा दुखी होता है। अतः आत्मा को बड़े प्रयत्न से सुखी बनाना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार आत्मा की भौतिक सेवा ही उपासना कही जा सकती है। वस्तुतः इसमें ईश्वर की सत्ता नहीं है।
फल प्राप्ति की इच्छा न रखकर ईश्वर की उपासना (सेवा), कर्तव्य का पालन और परोपकार करना निष्काम कर्मयोग है। यह भक्ति योग तथा ज्ञानयोग से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है । यद्यपि श्रद्धा की अपेक्षा भक्तियोग उपयोगी है और ज्ञानयोग उससे भी अधिक उपयोगी है तथापि 'निष्काम कर्मयोग' मध्यममार्ग है जो भक्तियोग और ज्ञानयोग दोनों में निष्काम कर्म की शिक्षा प्रदान करता है । इस योग में परमेश्वर . की उपासना पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इन्द्रियों के विषयों में व्यापारयुक्त चित्तवृत्तियों के निरोध करने को योग कहते हैं। योग की प्रधानता होने से इस दर्शन को योगदर्शन कहते हैं। इसके प्रणेता पतंजलि ऋषि कड़े जाते हैं। जब पूर्णरूप से योग का निरोध हो जाता है तब शुद्ध चैतन्य के साथ कैवल्य अवस्था प्राप्त हो जाती हैं। योग के साधनभूत अंग आठ होते हैं
यम (पाँच पापों का त्याग ), नियम, (सन्तोष, तप, स्वाध्याय,
ईश्वर - भक्ति
K: जैन पूजा-काव्य : एक चिन्तन