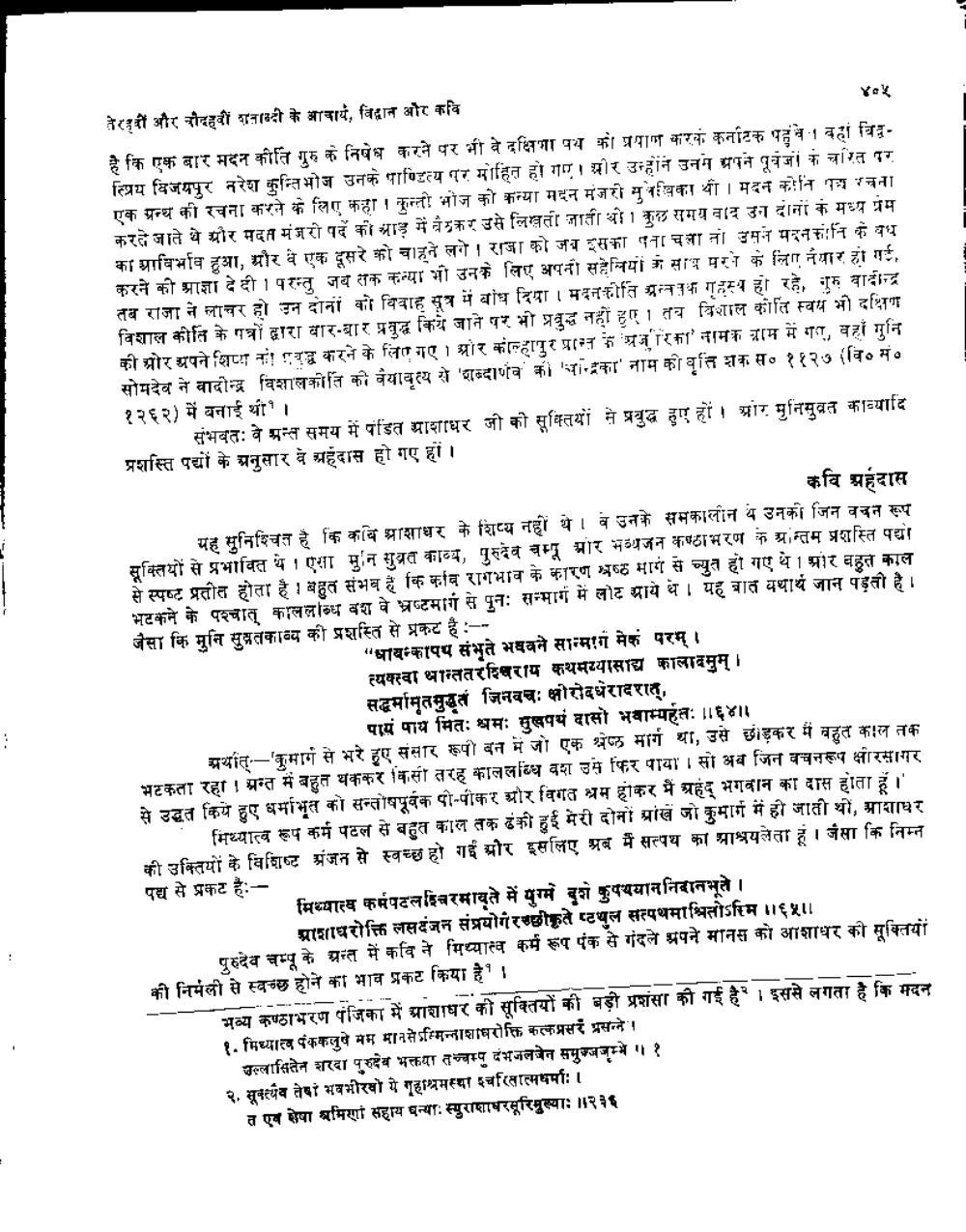________________
तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी के आचार्य, विद्वान और कवि
है कि एक बार मदन कीति गुरु के निषेध करने पर भी वे दक्षिणा पथ को प्रयाण करवं कर्नाटक पहंचे। वहां विद्वस्त्रिय विजयपुर नरेश कुन्तिभोज उनके पाण्डित्य पर मोहित हो गए। ग्रार उन्होंने उनम अपने पूर्वजों के चरित पर एक ग्रन्थ की रचना करने के लिए कहा । कुन्ती भोज को कन्या मदन मंजरी मुखिका थी। मदन कोनि पच रचना करते जाते थे और मदत मंजरी पर्दे की आड़ में बैठकर उसे लिखती जाती थी। कुछ समय बाद उन दोनों के मध्य प्रेम का प्राविर्भाव हुआ, और वे एक दूसरे को चाहने लगे। राजा को जब इसका पता चला तो उसने मदन कोनि के वध करने की आज्ञा दे दी। परन्तु जब तक कन्या भी उनके लिए अपनी सहेलियों के साप परने के लिए तैयार हो गई, तब राजा ने लाचर हो उन दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया । मदन-कीति अलका गहस्य हो रहे, गुरू वादीन्द्र विशाल कीति के पत्रों द्वारा बार-बार प्रतुद्ध किये जाने पर भी प्रवुद्ध नहीं हए। तब विशाल को ति स्वय भी दक्षिण की ओर अपने शिष्य नारद करने के लिए गए। और कोल्हापुर प्रान्त के अजारका' नामक ग्राम में गए, वहाँ मुनि सोमदेव ने वादीन्द्र विशालकोति की वैयावत्य से 'शब्दाव को 'चान्द्रका' नाम की वृत्ति शक स० ११२७ (वि०म० १२६२) में बनाई थी।
संभवतः वे अन्त समय में पंडित पाशाधर जी को सूक्तियों में प्रबुद्ध हुए हों। पर मुनिसुव्रत काव्यादि प्रशस्ति पद्यों के अनुसार वे अहंदास हो गए हो।
कवि अहंदास यह सुनिश्चित है कि कवि माशाधर के शिष्य नहीं थे। व उनके समकालीन थे उनकी जिन वचन रूप सूक्तियों से प्रभावित थे । एसा मुनि सुव्रत काव्य, पुरुदेव चम्पू मार भब्यजन कण्ठाभरण के अन्तिम प्रशस्ति पद्या से स्पष्ट प्रतीत होता है। बहुत संभव है कि कवि रागभाव के कारण श्रष्ठभाग स च्युत हो गए थे। पार बहत काल भटकने के पश्चात् काललब्धि बश वे भ्रष्टमार्ग से पुन: सन्मार्ग में लोट पाये थे। यह बात यथार्थ जान पड़ती है। जैसा कि मुनि सुखतकाव्य की प्रशस्ति से प्रकट है :--
"बायकापप संभृते भवबने सान्माग मेकं परम् । त्यवस्वा थान्ततरश्चिराय कथमय्यासाद्य कालावमुम्। सद्धर्मामृतमुखतं जिनवचः क्षीरोदधेरादरात
पायं पाय मितः श्रमः सुखपयं दासो भवाम्यहतः ।।६४॥ अर्थात-कुमार्ग से भरे हुए संसार रूपी वन में जो एक श्रेष्ठ मार्ग था, उसे छोड़कर में बहुत काल तक भटकता रहा । अन्त में बहुत थककर किसी तरह काललब्धि वश उसे फिर पाया । सो अब जिन वचनरूप क्षीरसागर से उद्धत किये हुए धर्माभूत को सन्तोषपूर्वक पी-पीकर और विगत श्रम होकर मैं अहं भगवान का दास होता है।'
मिथ्यात्व रूप कर्म पटल से बहुत काल तक ढंकी हुई मेरी दोनों प्रांख जो कुमार्ग में हो जाती थी, आशाघर की उक्तियों के विशिष्ट अंजन से स्वच्छ हो गई और इसलिए अब मैं सत्पथ का प्राश्रयलेता हूं। जैसा कि निम्न पञ्च से प्रकट है:
मिथ्यात्व कर्मपदलहिचरमायते में युग्म वृशे कुपथयाननिदानभूते ।
प्राशाघरोक्ति लसदंजन संप्रयोगरन्छीकृते प्टथुल सत्पथमाश्रितोऽस्मि ॥६॥ पुरुदेव चम्पू के अन्त में कवि ने मिथ्यात्व कर्म रूप पंक से गंदले अपने मानस को आशाधर को सूक्तियों की निर्मली से स्वच्छ होने का भाव प्रकट किया है।
भव्य कण्ठाभरण पंजिका में पाशाधर की सूक्तियों की बड़ी प्रशंसा की गई है। इससे लगता है कि मदन १. मिथ्यात्व पंककलुषे मम मानसे ऽस्मिन्नाशाधरोक्ति कत्कप्रसरं प्रसन्ने ।
उल्लासितेन शरदा पुरुदेव भक्तया तच्चम्प दंभजलजेन समुज्जजम्भे ॥१ २. सूक्त्यैव तेषां भवभीरखो ये गृहाश्रमस्था चरितात्मधर्माः । त एवं शेषा अमिणां सहाय धन्याः स्युराशापरसूरिमुख्याः ॥२३६