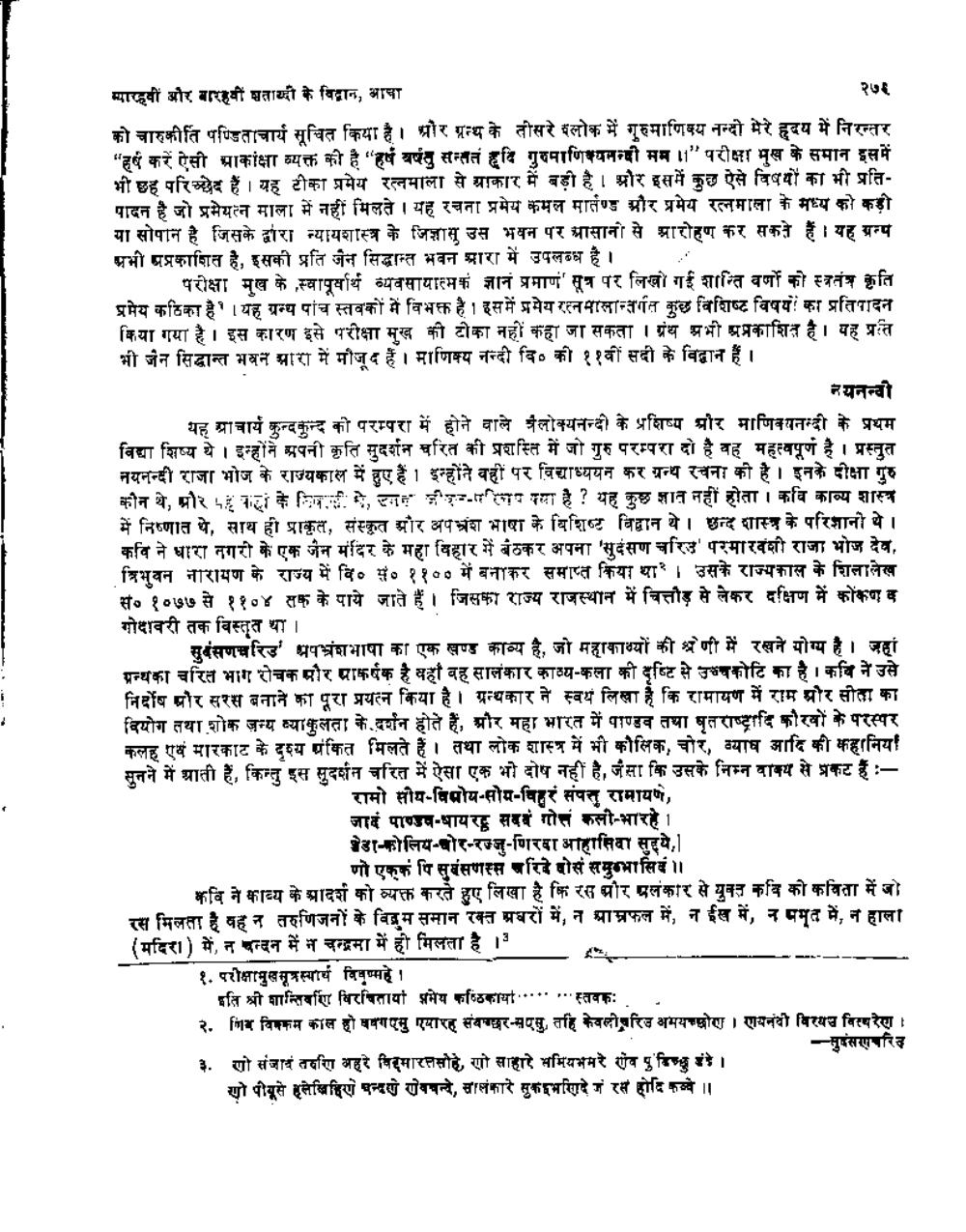________________
म्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के विद्वान, आचा
२७६
को चारुकीर्ति पण्डिताचार्य सूचित किया है। और ग्रन्थ के तीसरे श्लोक में गुरुमाणिक्य नन्दो मेरे हृदय में निरन्तर "हर्ष करें ऐसी आकांक्षा व्यक्त की है "हर्ष वर्षतु सन्ततं हृदि गुरुमाणिक्यनन्दी मम ।।" परीक्षा मुख के समान इसमें भी छह परिच्छेद हैं। यह टीका प्रमेय रत्नमाला से ग्राकार में बड़ी है। और इसमें कुछ ऐसे विषयों का भी प्रतिपादन है जो प्रयत्न माला में नहीं मिलते। यह रचना प्रमेय कमल मार्तण्ड और प्रमेय रत्नमाला के मध्य को कड़ी या सोपान है जिसके द्वारा न्यायशास्त्र के जिज्ञासु उस भवन पर आसानी से आरोहण कर सकते हैं। यह ग्रन्य अभी प्रकाशित है, इसकी प्रति जैन सिद्धान्त भवन प्रारा में उपलब्ध है ।
परीक्षा मुख के स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणं' सूत्र पर लिखो गई शान्ति वर्णों को स्वतंत्र कृति प्रमेय कठिका है | यह ग्रन्थ पांच स्तबकों में विभक्त है। इसमें प्रमेय रत्नमालान्तर्गत कुछ विशिष्ट विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस कारण इसे परीक्षा मुख की टीका नहीं कहा जा सकता । ग्रंथ अभी अप्रकाशित है। यह प्रति भी जैन सिद्धान्त भवन आरा में मौजूद हैं। माणिक्य नन्दी वि० की ११वीं सदी के विद्वान हैं ।
नयनन्वी
यह प्राचार्य कुन्दकुन्द 'की परम्परा में होने वाले त्रैलोक्यनन्दी के प्रशिष्य श्रीर माणिक्यनन्दी के प्रथम विद्या शिष्य थे । इन्होंने अपनी कृति सुदर्शन चरित की प्रशस्ति में जो गुरु परम्परा दो है वह महत्वपूर्ण है । प्रस्तुत नयनन्दी राजा भोज के राज्यकाल में हुए हैं। इन्होंने वहीं पर विद्याध्ययन कर ग्रन्थ रचना की है। इनके दीक्षा गुरु कौन थे, क्या है? यह कुछ ज्ञात नहीं होता । कवि काव्य शास्त्र में निष्णात थे, साथ ही प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश भाषा के विशिष्ट विद्वान थे। छन्द शास्त्र के परिज्ञानी थे । कवि ने धारा नगरी के एक जैन मंदिर के महा विहार में बैठकर अपना 'सुदंसण चरित्र' परमारवंशी राजा भोज देव, त्रिभुवन नारायण के राज्य में वि० सं० ११०० में बनाकर समाप्त किया था। उसके राज्यकाल के शिलालेख सं० १०७७ से ११०४ तक के पाये जाते हैं। जिसका राज्य राजस्थान में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में कोंकण व गोदावरी तक विस्तृत था ।
सुदंसणचरिउ अपभ्रंशभाषा का एक खण्ड काव्य है, जो महाकाव्यों की श्रेणी में रखने योग्य है। जहां ग्रन्थका चरित भाग रोचक और पाकर्षक है वहाँ वह सालंकार काव्य-कला की दृष्टि से उच्चकोटि का है। कवि ने उसे निर्दोष और सरस बनाने का पूरा प्रयत्न किया है। ग्रन्थकार ने स्वयं लिखा है कि रामायण में राम और सीता का faयोग तथा शोक जन्य व्याकुलता के दर्शन होते हैं, और महा भारत में पाण्डव तथा धृतराष्ट्रादि कौरवों के परस्पर कलह एवं मारकाट के दृश्य पंक्ति मिलते हैं। तथा लोक शास्त्र में भी कौलिक, चोर, व्याध आदि की कहानियाँ सुनने में थाती हैं, किन्तु इस सुदर्शन चरित में ऐसा एक भी दोष नहीं है, जैसा कि उसके निम्न वाक्य से प्रकट हैं :
रामो सो विद्यय-सोय-विहरं संपतु रामायणे, जावं पाण्डव- धायरट्ठ सवयं गोलं कली- भारहे। डा-कोलिय-थोर-रज्जु-गिरवा आहासिवा सुये, ।
viteos free चरिदे बोस समुभासिवं ॥
कवि ने काव्य के आदर्श को व्यक्त करते हुए लिखा है कि रस और एलंकार से युक्त कवि की कविता में जो रस मिलता है वह न तरुणिजनों के विद्रुम समान रक्त प्रवरों में न आम्रफल में, न ईख में, न ममृत में, न हाला ( मंदिर 1 ) में, न चन्दन में न चन्द्रमा में ही मिलता है ।
१. परीक्षासूत्रस्याचं विवृष्महे ।
इति श्री शान्ति विरचितायां प्रमेय कण्ठिकाया
........ स्तवकः
२. for विक्कम काल हो वषगए एयारह संच्छर-ससु तहि केवल्दी चरिउ अमय छोरा । एायनंदी विरयञ्च वित्यरेण ।
- सुदंसणचरिद
३. यो संजावं तदरिण अहरे विमारतसोहे, यो साहारे समियममरे व पु बिच्छु । णो पीयूसे लेखहिणे चन्द विचन्ये, सालंकारे सुकद्दमणिदे गं रस होदि कव्वे ॥