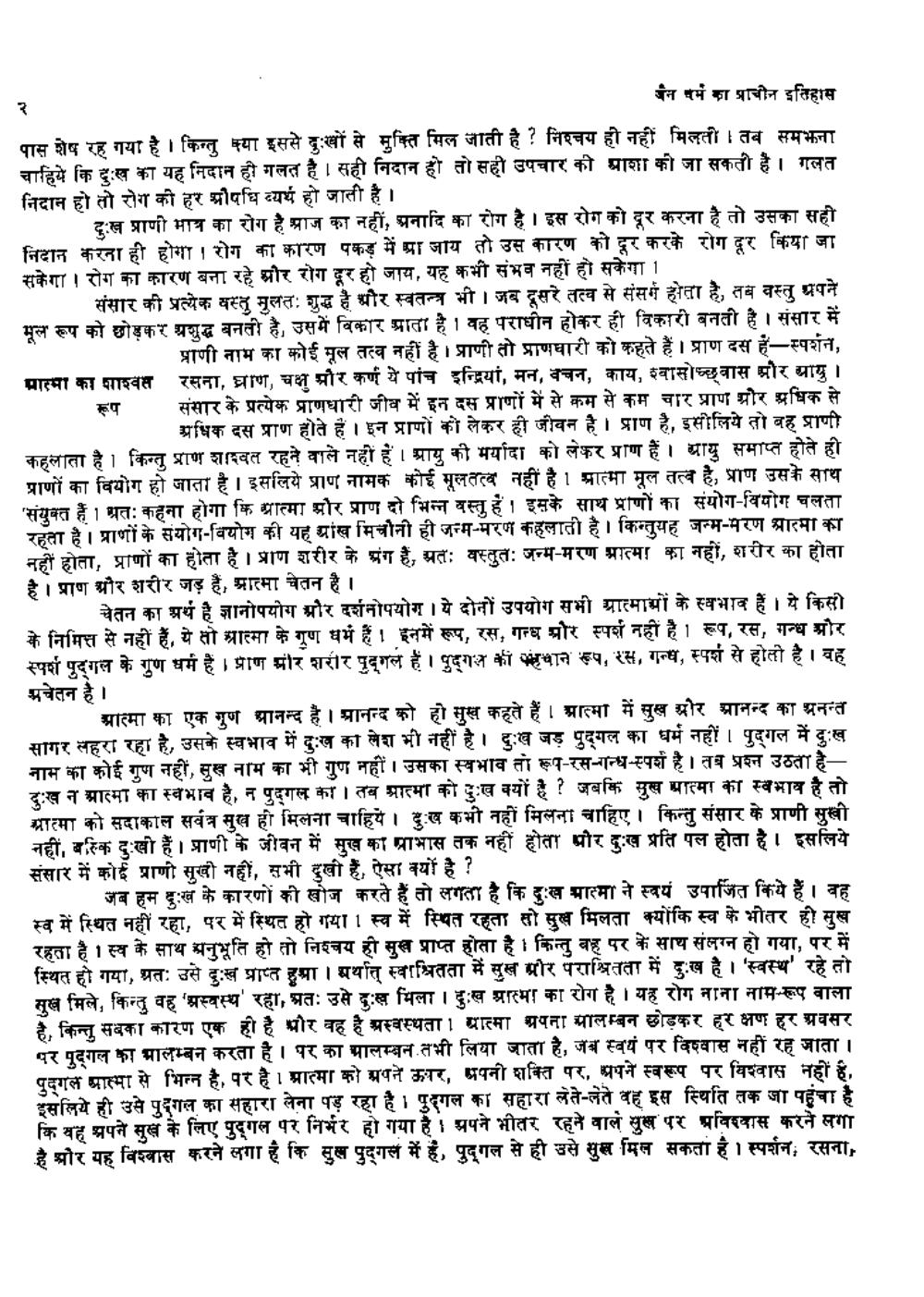________________
जैन धर्म का प्राचीन इतिहास
२
पास शेष रह गया है । किन्तु क्या इससे दुःखों से मुक्ति मिल जाती है ? निश्चय ही नहीं मिलती । तब समझना चाहिये कि दुःख का यह निदान ही गलत है। सही निदान हो तो सही उपचार की प्राशा की जा सकती हैं। गलत निदान तो रोग की हर श्रौषधि व्यर्थ हो जाती है ।
दुःख प्राणी मात्र का रोग है श्राज का नहीं, अनादि का रोग है। इस रोग को दूर करना है तो उसका सही निदान करना ही होगा । रोग का कारण पकड़ में प्रा जाय तो उस कारण को दूर करके रोग दूर किया जा सकेगा । रोग का कारण बना रहे और रोग दूर हो जाय, यह कभी संभव नहीं हो सकेगा 1
संसार की प्रत्येक वस्तु मुलतः शुद्ध है और स्वतन्त्र भी जब दूसरे तत्व से संसर्ग होता है, तब वस्तु अपने मूल रूप को छोड़कर अशुद्ध बनती है, उसमें विकार श्राता है । वह पराधीन होकर ही विकारी बनती है । संसार में प्राणी नाम का कोई मूल तत्व नहीं है। प्राणी तो प्राणघारी को कहते हैं । प्राण दस हैं- स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पांच इन्द्रियां, मन, वचन, काय, श्वासोच्छ्वास और बायु | संसार के प्रत्येक प्राणधारी जीव में इन दस प्राणों में से कम से कम चार प्राण और अधिक से
प्रात्मा का शाश्वत रूप
अधिक दस प्राण होते हैं। इन प्राणों को लेकर ही जीवन है। प्राण है, इसीलिये तो वह प्राणी कहलाता है । किन्तु प्राण शाश्वत रहने वाले नहीं हैं। आयु की मर्यादा को लेकर प्राण हैं। आयु समाप्त होते ही प्राणों का वियोग हो जाता है । इसलिये प्राण नामक कोई मूलतत्व नहीं है । श्रात्मा मूल तत्व है, प्राण उसके साथ 'संयुक्त हैं । श्रतः कहना होगा कि आत्मा और प्राण दो भिन्न वस्तु हैं। इसके साथ प्राणों का संयोग-वियोग चलता रहता है । प्राणों के संयोग-वियोग की यह ग्रांख मिचौनी ही जन्म-मरण कहलाती है। किन्तुयह जन्म-मरण श्रात्मा का नहीं होता, प्राणों का होता है। प्राण शरीर के अंग हैं, अतः वस्तुतः जन्म-मरण श्रात्मा का नहीं, शरीर का होता है। प्राण और शरीर जड़ हैं, श्रात्मा चेतन है ।
चेतन का अर्थ है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । ये दोनों उपयोग सभी ग्रात्माओं के स्वभाव हैं। ये किसी के निमित्त से नहीं हैं, ये तो श्रात्मा के गुण धर्म हैं । इनमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श नहीं है । रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पुद्गल के गुण धर्म हैं। प्राण और शरीर पुद्गल हैं । पुद्गल की पहचान रूप, रस, गन्ध, स्पर्श से होती है । वह अचेतन है ।
आत्मा का एक गुण आनन्द है । श्रानन्द को हो सुख कहते हैं। आत्मा में सुख और आनन्द का अनन्त सागर लहरा रहा है, उसके स्वभाव में दुःख का लेश भी नहीं है । दुःख जड़ पुद्गल का धर्म नहीं । पुद्गल में दुःख नाम का कोई गुण नहीं, सुख नाम का भी गुण नहीं। उसका स्वभाव तो रूप-रस- गन्ध-स्पर्श है। तब प्रश्न उठता है— दुःख न आत्मा का स्वभाव है, न पुद्गल का। तब श्रात्मा को दुःख क्यों है ? जबकि सुख मात्मा का स्वभाव है तो श्रात्मा को सदाकाल सर्वत्र सुख ही मिलना चाहिये । दुःख कभी नहीं मिलना चाहिए। किन्तु संसार के प्राणी सुखी नहीं, बल्कि दुःखी हैं । प्राणी के जीवन में सुख का प्राभास तक नहीं होता भौर दुःख प्रति पल होता है । इसलिये संसार में कोई प्राणी सुखी नहीं, सभी दुखी हैं, ऐसा क्यों है ?
जब हम दुःख के कारणों की खोज करते हैं तो लगता है कि दुःख श्रात्मा ने स्वयं उपार्जित किये हैं। वह स्व में स्थित नहीं रहा, पर में स्थित हो गया । स्व में स्थित रहता सो सुख मिलता क्योंकि स्व के भीतर ही सुख रहता है । स्व के साथ अनुभूति हो तो निश्चय ही सुख प्राप्त होता है। किन्तु वह पर के साथ संलग्न हो गया, पर में स्थित हो गया, अतः उसे दुःख प्राप्त हुआ । अर्थात् स्वाश्रितता में सुख और पराश्रितता में दुःख है । 'स्वस्थ' रहे तो सुख मिले, किन्तु वह 'अस्वस्थ' रहा, अतः उसे दुःख मिला । दुःख आत्मा का रोग है। यह रोग नाना नाम-रूप वाला है, किन्तु सबका कारण एक ही है और वह है अस्वस्थता | ग्रात्मा अपना मालम्बन छोड़कर हर क्षण हर अवसर पर पुद्गल का भालम्बन करता है। पर का आलम्बन तभी लिया जाता है, जब स्वयं पर विश्वास नहीं रह जाता । पुद्गल आत्मा से भिन्न है, पर है। आत्मा को अपने ऊपर अपनी शक्ति पर अपने स्वरूप पर विश्वास नहीं है, इसलिये ही उसे पुद्गल का सहारा लेना पड़ रहा है। पुद्गल का सहारा लेते-लेते वह इस स्थिति तक जा पहुंचा है। कि वह अपने सुख के लिए पुद्गल पर निर्भर हो गया है। अपने भीतर रहने वाले सुख पर अविश्वास करने लगा है और यह विश्वास करने लगा है कि सुख पुद्गल में हैं, पुद्गल से ही उसे सुख मिल सकता है। स्पर्शन; रसना,