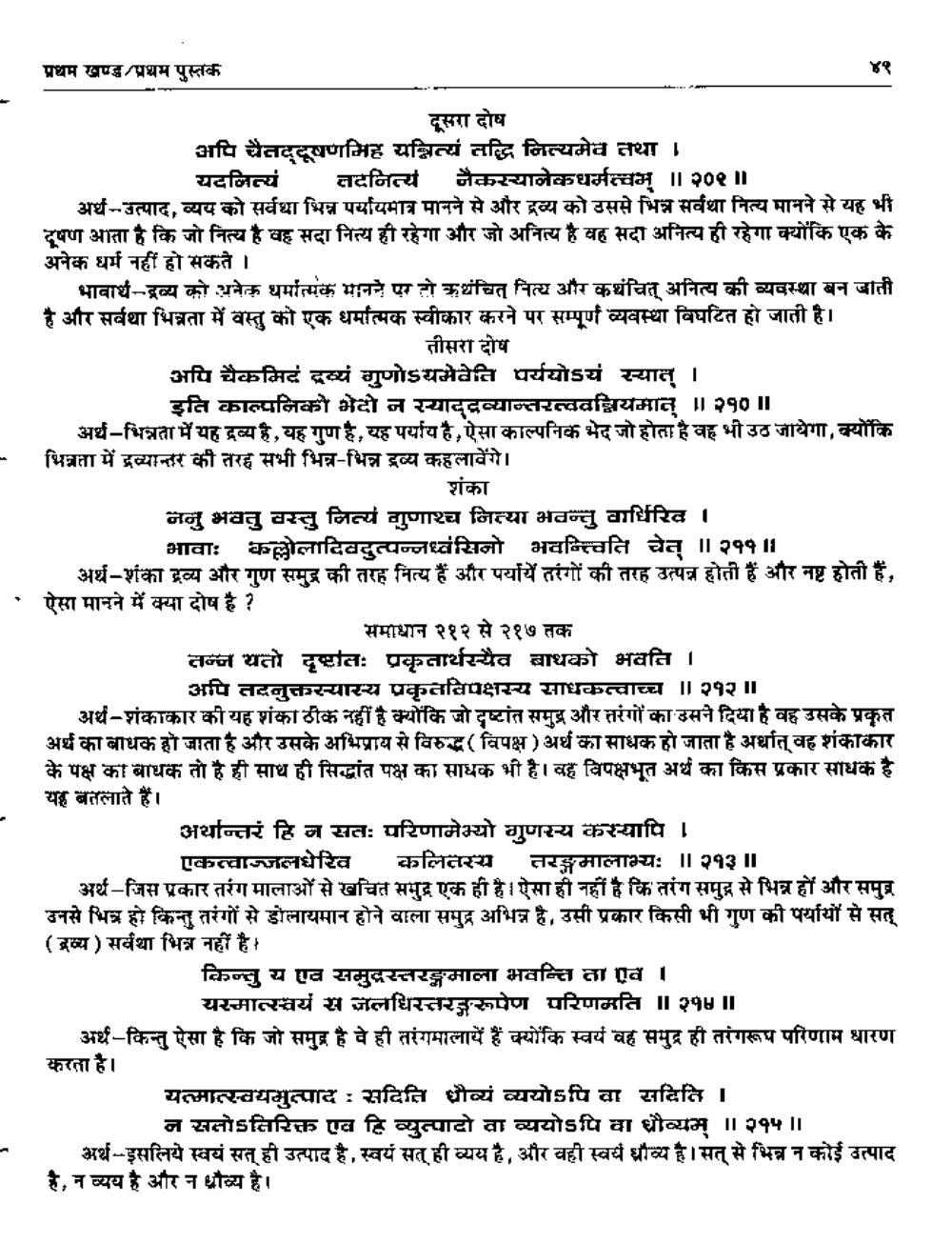________________
प्रथम खण्ड/प्रथम पुस्तक
दूसरा दोष अपि चैतदूषणमिह यन्नित्यं तद्धि नित्यमेव तथा ।
यदलित्यं तदनित्य जैकरयाजेकधर्मस्वम् ॥ २०॥ अर्थ-उत्पाद, व्यय को सर्वथा भिन्न पर्यायमात्र मानने से और द्रव्य को उससे भिन्न सर्वथा नित्य मानने से यह भी दूषण आता है कि जो नित्य है वह सदा नित्य ही रहेगा और जो अनित्य है वह सदा अनित्य ही रहेगा क्योंकि एक के अनेक धर्म नहीं हो सकते ।
भावार्थ-द्रव्य को अनेक थर्मात्मक मानने पर तो कथंचित नित्य और कथंचित् अनित्य की व्यवस्था बन जाती है और सर्वथा भिन्नता में वस्तु को एक धर्मात्मक स्वीकार करने पर सम्पूर्ण व्यवस्था विघटित हो जाती है।
तीसरा दोष अपि चैकमिदं द्रव्यं गुणोऽयमेवेति पर्ययोऽयं स्यात् ।
इति काल्पनिको भेदो न स्यादव्यान्तरत्तवनियमान् ॥ २१० ॥ अर्थ-भिन्नता में यह द्रव्य है,यह गुण है,यह पर्याय है,ऐसा काल्पनिक भेद जो होता है वह भी उठ जायेगा, क्योंकि भित्रता में द्रव्यान्तर की तरह सभी भिन्न-भिन्न द्रव्य कहलावेंगे।
शंका ननु भवतु वस्तु जित्य गुणाश्च नित्या भवन्तु वाधिरित ।
भावाः कल्लोलादिवदुत्पन्नध्वंसिनो भवन्विति चेत् ॥ २११ ॥ ___ अर्थ-शंका द्रव्य और गुण समुद्र की तरह नित्य हैं और पर्यायें तरंगों की तरह उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती है, ' ऐसा मानने में क्या दोष है ?
समाधान २१२ से २१७ तक तन्न यतो दृशीतः प्रकृतार्थस्यैव बाधको भवति ।
अपि तदनुत्तस्यास्य प्रकृतविपक्षस्य साधकत्वाच्च ।। २१२॥ अर्थ-शंकाकार की यह शंकाठीक नहीं है क्योंकि जो दृष्टांत समुद्र और तरंगों का उसने दिया है वह उसके प्रकृत अर्थका बाधक हो जाता है और उसके अभिप्राय से विरुद्ध (विपक्ष) अर्थका साधक हो जाता है अर्थात वह शंकाकार के पक्ष का बाधक तो है ही साथ ही सिद्धांत पक्षका साधक भी है। वह विपक्षभूत अर्थ का किस प्रकार साधक है यह बतलाते हैं।
अर्थान्तरं हि न सतः परिणामेम्यो गुणस्य कस्यापि ।
एकत्ताञ्जलधेरिव कलितस्य तरङ्गमालाभ्यः ॥ २१३॥ अर्थ-जिस प्रकार तरंग मालाओं से खचित समुद्र एक ही है। ऐसा ही नहीं है कि तरंग समुद्र से भिन्न हों और समुद्र उनसे भित्र हो किन्तु तरंगों से डोलायमान होने वाला समुद्र अभिन्न है, उसी प्रकार किसी भी गुण की पर्यायों से सत् (ख्य) सर्वथा भित्र नहीं है।
किन्तु य एव समुद्रस्तरङ्गमाला भवन्ति ता एव ।
यस्मात्स्वयं स जलधिरतरङ्गरूपेण परिणमति ॥ २१४ ॥ अर्थ-किन्तु ऐसा है कि जो समुद्र है वे ही तरंगमालायें हैं क्योंकि स्वयं वह समुद्र ही तरंगरूप परिणाम धारण करता है।
यत्मात्स्वयमत्पाद: सदिति धौव्यं व्ययोऽपि वा सदिति ।
न सतोऽतिरिक्त एव हि व्युत्पादो वा व्ययोऽपि वा धौव्यम् ॥ २१५ ।। ___ अर्थ-इसलिये स्वयं सत् ही उत्पाद है, स्वयं सत् ही व्यय है, और वही स्वयं धौव्य है। सत् से भिन्न न कोई उत्पाद है, न व्यय है और न धौव्य है।