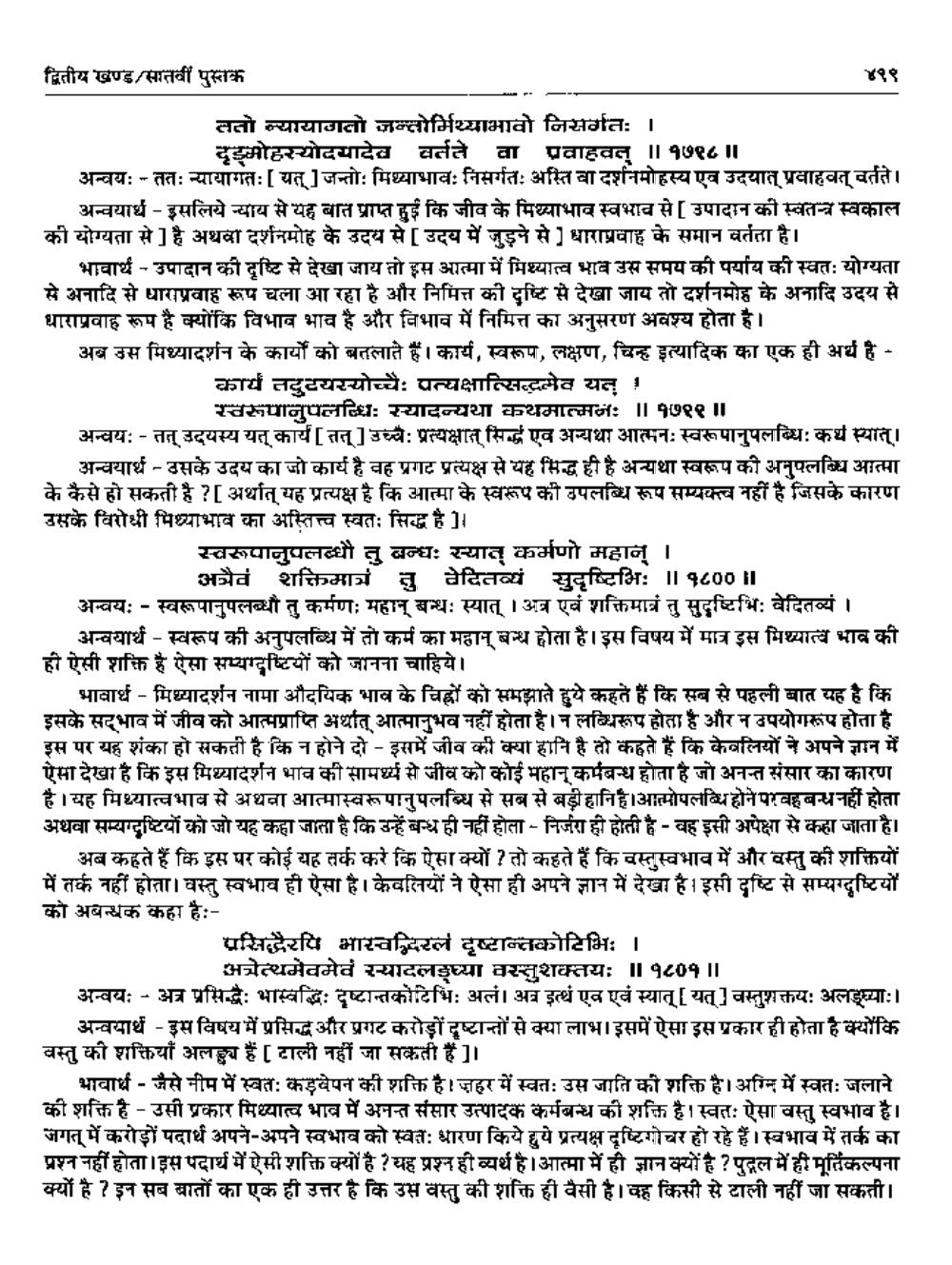________________
द्वितीय खण्ड/सातवीं पुस्तक
४२९
ततो न्यायागतो जन्तोर्मिथ्याभावो निसर्गतः ।
दृइमोहस्योदयादेव वर्तते वा प्रवाहवत् || १७९८।। अन्वयः - ततः न्यायागतः [ यत् ] जन्तो: मिथ्याभावः निसर्गतः अस्ति वा दर्शनमोहस्य एव उदयात् प्रवाहवत् वर्तते।
अन्वयार्थ - इसलिये न्याय से यह बात प्राप्त हुई कि जीव के मिथ्याभाव स्वभाव से [ उपादान की स्वतन्त्र स्वकाल की योग्यता से ] है अथवा दर्शनमोह के उदय से [ उदय में जुड़ने से ] धाराप्रवाह के समान वर्तता है।
वार्थ - उपादान की दृष्टि से देखा जाय तो इस आत्मा में मिथ्यात्वभाव उस समय की पर्याय की स्वत: योग्यता से अनादि से धाराप्रवाह रूप चला आ रहा है और निमित्त की दृष्टि से देखा जाय तो दर्शनमोह के अनादि उदय से धाराप्रवाह रूप है क्योंकि विभाव भाव है और विभाव में निमित्त का अनुसरण अवश्य होता है। अब उस मिध्यादर्शन के कार्यों को बतलाते हैं। कार्य, स्वरूप, लक्षण, चिन्ह इत्यादिक का एक ही अर्थ है -
कार्य तट्टयरयोच्चैः प्रत्यक्षात्सिदमेव यल !
रवरूपानपलब्धिः स्यादन्यथा कथमात्मनः ॥ १७९९ ।। अन्वयः - तत् उदयस्य यत् कार्य [तत्] उच्चैः प्रत्यक्षात् सिद्धं एव अन्यथा आत्मन: स्वरूपानुपलब्धिः कथं स्यात्।
अन्वयार्थ - उसके उदय का जो कार्य है वह प्रगट प्रत्यक्ष से यह सिद्ध ही है अन्यथा स्वरूप की अनुपलब्धि आत्मा के कैसे हो सकती है?[अर्थात यह प्रत्यक्ष है कि आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि रूप सम्यक्त
त् यह प्रत्यक्ष है कि आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि रूप सम्यक्त्व नहीं है जिसके कारण उसके विरोधी मिथ्याभाव का अस्तित्त्व स्वतः सिद्ध है।
स्वरूपानुपलब्धौ तु बन्धः स्यात् कर्मणो महान् ।
अत्रैवं शक्तिमानं तु वेदितव्यं सुदृष्टिभिः ॥ १८०० ॥ अन्वयः - स्वरूपानुपलब्धौ तु कर्मण: महान् बन्ध: स्यात् । अत्र एवं शक्तिमात्रं तु सुदृष्टिभिः वेदितव्यं ।
अन्वयार्थ - स्वरूप की अनुपलब्धि में तो कर्म का महान् बन्ध होता है। इस विषय में मात्र इस मिथ्यात्व भाव की ही ऐसी शक्ति है ऐसा सम्यग्दृष्टियों को जानना चाहिये।
भावार्थ - मिथ्यादर्शन नामा औदयिक भाव के चिह्नों को समझाते हुये कहते हैं कि सब से पहली बात यह है कि इसके सद्भाव में जीव को आत्मप्राप्ति अर्थात् आत्मानुभव नहीं होता है। न लब्धिरूप होता है और न उपयोगरूपहोता है इस पर यह शंका हो सकती है कि न होने दो- इसमें जीव की क्या हानि है तो कहते हैं कि केवलियों ने अपने ज्ञान में ऐसा देखा है कि इस मिथ्यादर्शन भाव की सामर्थ्य से जीव को कोई महान कर्मबन्ध होता है जो अनन्त संसार का कारण है। यह मिथ्यात्वभाव से अथवा आत्मास्वरूपानुपलब्धि से सब से बड़ी हानि है।आत्मोपलब्धिहोनेपरवहबन्धनहीं होता अथवा सम्यग्दृष्टियों को जो यह कहा जाता है कि उन्हें बन्ध ही नहीं होता - निर्जरा ही होती है - वह इसी अपेक्षा से कहा जाता है।
अब कहते हैं कि इस पर कोई यह तर्क करे कि ऐसा क्यों ? तो कहते हैं कि वस्तुस्वभाव में और वस्तु की शक्तियों में तर्क नहीं होता। वस्तु स्वभाव ही ऐसा है। केवलियों ने ऐसा ही अपने ज्ञान में देखा है। इसी दृष्टि से सम्यग्दृष्टियों को अबन्धक कहा है:
प्रसिद्वैरपि भारचदिरल दृष्टान्तकोटिभिः ।
अत्यमेवमेवं स्यादलघ्या वस्तुशक्तयः ॥ १८०१॥ अन्वयः - अत्र प्रसिद्धैः भास्वद्धिः दृष्टान्तकोदिभिः अलं। अब इत्थं एव एवं स्यात[यत वस्तुशक्तयः अलइय्याः।
अन्वयार्थ - इस विषय में प्रसिद्ध और प्रगट करोड़ों दृष्टान्तों से क्या लाभाइसमें ऐसा इस प्रकार ही होता है क्योंकि वस्तु की शक्तियाँ अलठ्य हैं [ टाली नहीं जा सकती हैं।
भावार्थ - जैसे नीम में स्वत: कड़वेपन की शक्ति है। जहर में स्वत: उस जाति की शक्ति है। अग्नि में स्वतः जलाने की शक्ति है - उसी प्रकार मिथ्यात्व भाव में अनन्त संसार उत्पादक कर्मबन्ध की शक्ति है। स्वतः ऐसा वस्तु स्वभाव है। जगत् में करोड़ों पदार्थ अपने-अपने स्वभाव को स्वत: धारण किये हुये प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। स्वभाव में तर्क का
पदार्थ में ऐसी शक्ति क्यों है? यह प्रश्न ही व्यर्थ है।आत्मा में ही ज्ञान क्यों है? पदल में ही मर्तिकल्पना क्यों है ? इन सब बातों का एक ही उत्तर है कि उस वस्तु की शक्ति ही वैसी है। वह किसी से टाली नहीं जा सकती।