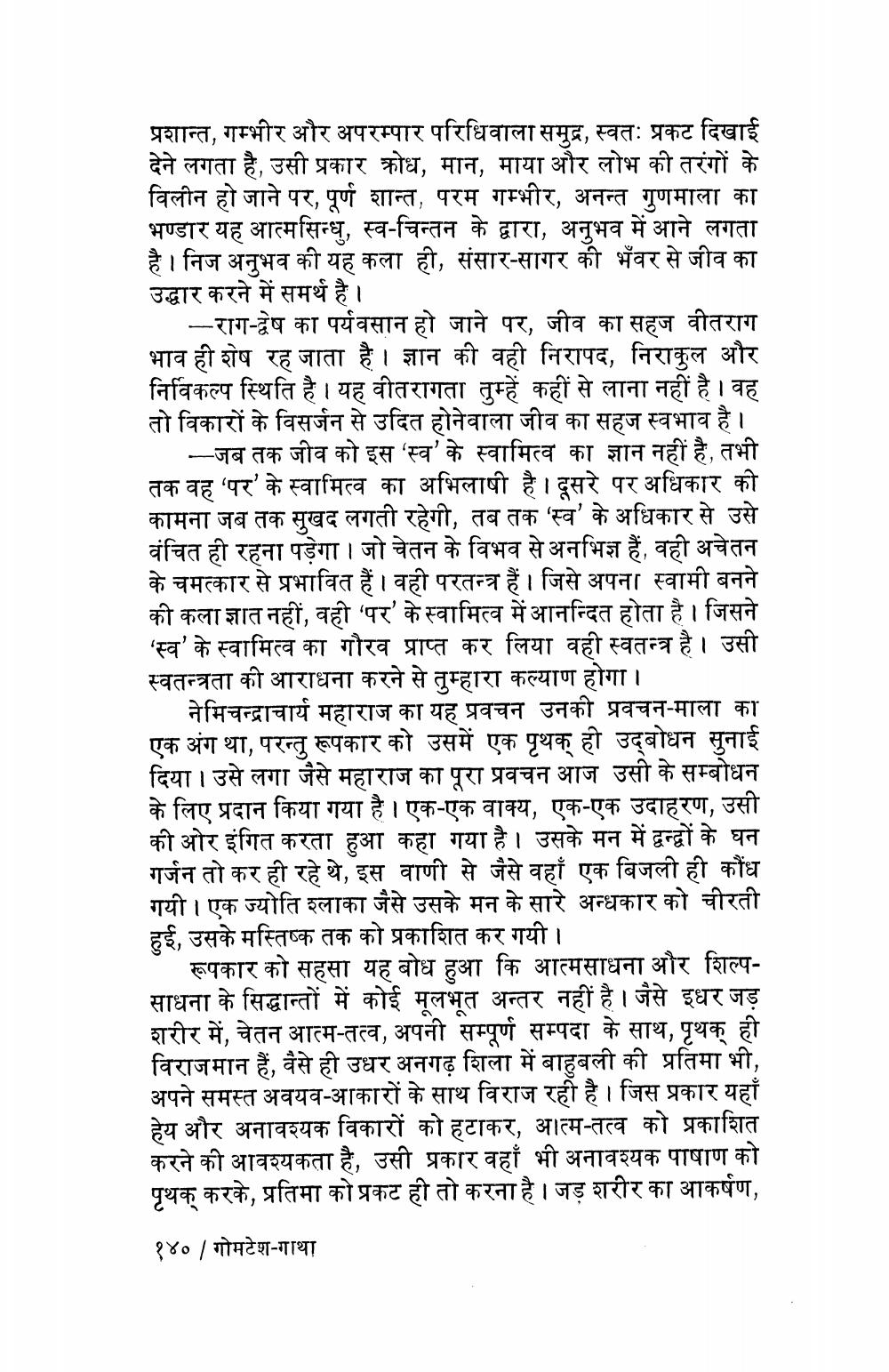________________
प्रशान्त, गम्भीर और अपरम्पार परिधिवाला समुद्र, स्वतः प्रकट दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार क्रोध, मान, माया और लोभ की तरंगों के विलीन हो जाने पर, पूर्ण शान्त, परम गम्भीर, अनन्त गुणमाला का भण्डार यह आत्मसिन्धु, स्व-चिन्तन के द्वारा, अनुभव में आने लगता है। निज अनुभव की यह कला ही, संसार-सागर की भँवर से जीव का उद्धार करने में समर्थ है।
-राग-द्वेष का पर्यवसान हो जाने पर, जीव का सहज वीतराग भाव ही शेष रह जाता है। ज्ञान की वही निरापद, निराकुल और निर्विकल्प स्थिति है। यह वीतरागता तुम्हें कहीं से लाना नहीं है। वह तो विकारों के विसर्जन से उदित होनेवाला जीव का सहज स्वभाव है।
-जब तक जीव को इस 'स्व' के स्वामित्व का ज्ञान नहीं है, तभी तक वह 'पर' के स्वामित्व का अभिलाषी है। दूसरे पर अधिकार की कामना जब तक सुखद लगती रहेगी, तब तक 'स्व' के अधिकार से उसे वंचित ही रहना पड़ेगा। जो चेतन के विभव से अनभिज्ञ हैं, वही अचेतन के चमत्कार से प्रभावित हैं। वही परतन्त्र हैं। जिसे अपना स्वामी बनने की कला ज्ञात नहीं, वही 'पर' के स्वामित्व में आनन्दित होता है । जिसने 'स्व' के स्वामित्व का गौरव प्राप्त कर लिया वही स्वतन्त्र है। उसी स्वतन्त्रता की आराधना करने से तुम्हारा कल्याण होगा।
नेमिचन्द्राचार्य महाराज का यह प्रवचन उनकी प्रवचन-माला का एक अंग था, परन्तु रूपकार को उसमें एक पृथक् ही उद्बोधन सुनाई दिया। उसे लगा जैसे महाराज का पूरा प्रवचन आज उसी के सम्बोधन के लिए प्रदान किया गया है। एक-एक वाक्य, एक-एक उदाहरण, उसी की ओर इंगित करता हुआ कहा गया है। उसके मन में द्वन्द्वों के घन गर्जन तो कर ही रहे थे, इस वाणी से जैसे वहाँ एक बिजली ही कौंध गयी। एक ज्योति श्लाका जैसे उसके मन के सारे अन्धकार को चीरती हुई, उसके मस्तिष्क तक को प्रकाशित कर गयी।
रूपकार को सहसा यह बोध हुआ कि आत्मसाधना और शिल्पसाधना के सिद्धान्तों में कोई मूलभूत अन्तर नहीं है। जैसे इधर जड़ शरीर में, चेतन आत्म-तत्व, अपनी सम्पूर्ण सम्पदा के साथ, पृथक् ही विराजमान हैं, वैसे ही उधर अनगढ़ शिला में बाहुबली की प्रतिमा भी, अपने समस्त अवयव-आकारों के साथ विराज रही है। जिस प्रकार यहाँ हेय और अनावश्यक विकारों को हटाकर, आत्म-तत्व को प्रकाशित करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार वहाँ भी अनावश्यक पाषाण को पृथक् करके, प्रतिमा को प्रकट ही तो करना है। जड़ शरीर का आकर्षण,
१४० / गोमटेश-गाथा