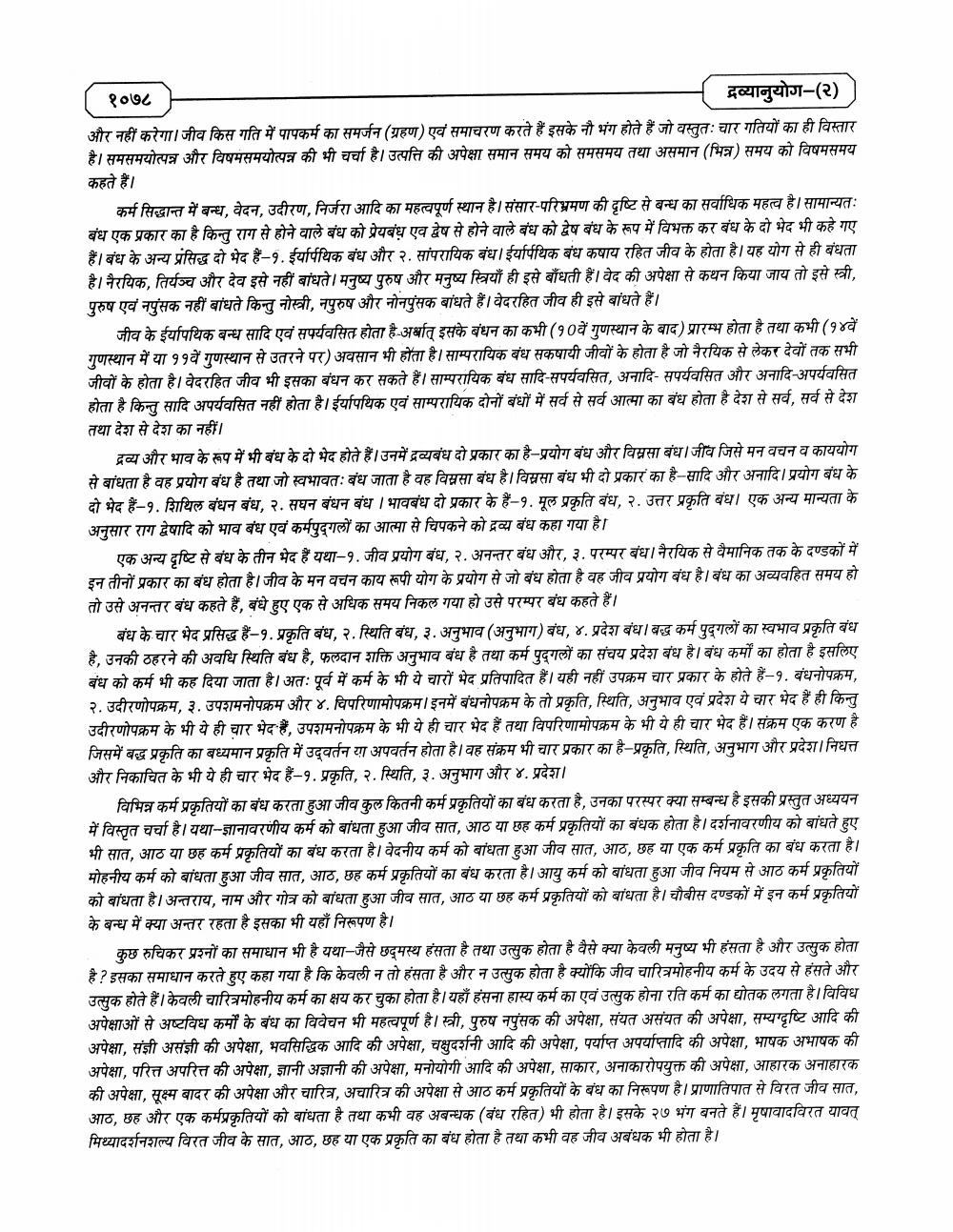________________
१०७८
द्रव्यानुयोग-(२) और नहीं करेगा। जीव किस गति में पापकर्म का समर्जन (ग्रहण) एवं समाचरण करते हैं इसके नौ भंग होते हैं जो वस्तुतः चार गतियों का ही विस्तार है। समसमयोत्पन्न और विषमसमयोत्पन्न की भी चर्चा है। उत्पत्ति की अपेक्षा समान समय को समसमय तथा असमान (भिन्न) समय को विषमसमय कहते हैं।
कर्म सिद्धान्त में बन्ध, वेदन, उदीरण, निर्जरा आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। संसार-परिभ्रमण की दृष्टि से बन्ध का सर्वाधिक महत्व है। सामान्यतः बंध एक प्रकार का है किन्तु राग से होने वाले बंध को प्रेयबंध एव द्वेष से होने वाले बंध को द्वेष बंध के रूप में विभक्त कर बंध के दो भेद भी कहे गए हैं। बंध के अन्य प्रसिद्ध दो भेद हैं-१. ईपिथिक बंध और २. सांपरायिक बंध। ईपिथिक बंध कषाय रहित जीव के होता है। यह योग से ही बंधता है। नैरयिक, तिर्यञ्च और देव इसे नहीं बांधते। मनुष्य पुरुष और मनुष्य स्त्रियाँ ही इसे बाँधती हैं। वेद की अपेक्षा से कथन किया जाय तो इसे स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक नहीं बांधते किन्तु नोस्त्री, नपुरुष और नोनपुंसक बांधते हैं। वेदरहित जीव ही इसे बांधते हैं।
जीव के ईपिथिक बन्ध सादि एवं सपर्यवसित होता है अर्थात् इसके बंधन का कभी (90वें गुणस्थान के बाद) प्रारम्भ होता है तथा कभी (१४वें गुणस्थान में या ११वें गुणस्थान से उतरने पर) अवसान भी होता है। साम्परायिक बंध सकषायी जीवों के होता है जो नैरयिक से लेकर देवों तक सभी जीवों के होता है। वेदरहित जीव भी इसका बंधन कर सकते हैं। साम्परायिक बंध सादि-सपर्यवसित, अनादि-सपर्यवसित और अनादि-अपर्यवसित होता है किन्तु सादि अपर्यवसित नहीं होता है। ईर्यापथिक एवं साम्परायिक दोनों बंधों में सर्व से सर्व आत्मा का बंध होता है देश से सर्व, सर्व से देश तथा देश से देश का नहीं।
द्रव्य और भाव के रूप में भी बंध के दो भेद होते हैं। उनमें द्रव्यबंध दो प्रकार का है-प्रयोग बंध और विनसा बंध। जीव जिसे मन वचन व काययोग से बांधता है वह प्रयोग बंध है तथा जो स्वभावतः बंध जाता है वह विनसा बंध है। विनसा बंध भी दो प्रकार का है-सादि और अनादि। प्रयोग बंध के दो भेद हैं-१. शिथिल बंधन बंध, २. सघन बंधन बंध | भावबंध दो प्रकार के हैं-१. मूल प्रकृति बंध, २. उत्तर प्रकृति बंध। एक अन्य मान्यता के अनुसार राग द्वेषादि को भाव बंध एवं कर्मपुद्गलों का आत्मा से चिपकने को द्रव्य बंध कहा गया है।
एक अन्य दृष्टि से बंध के तीन भेद हैं यथा-१. जीव प्रयोग बंध, २. अनन्तर बंध और, ३. परम्पर बंध। नैरयिक से वैमानिक तक के दण्डकों में इन तीनों प्रकार का बंध होता है। जीव के मन वचन काय रूपी योग के प्रयोग से जो बंध होता है वह जीव प्रयोग बंध है। बंध का अव्यवहित समय हो तो उसे अनन्तर बंध कहते हैं, बंधे हुए एक से अधिक समय निकल गया हो उसे परम्पर बंध कहते हैं।
बंध के चार भेद प्रसिद्ध हैं-१. प्रकृति बंध, २. स्थिति बंध, ३. अनुभाव (अनुभाग) बंध, ४. प्रदेश बंधा बद्ध कर्म पुद्गलों का स्वभाव प्रकृति बंध है, उनकी ठहरने की अवधि स्थिति बंध है, फलदान शक्ति अनुभाव बंध है तथा कर्म पुद्गलों का संचय प्रदेश बंध है। बंध कर्मों का होता है इसलिए बंध को कर्म भी कह दिया जाता है। अतः पूर्व में कर्म के भी ये चारों भेद प्रतिपादित हैं। यही नहीं उपक्रम चार प्रकार के होते हैं-१. बंधनोपक्रम, २. उदीरणोपक्रम, ३. उपशमनोपक्रम और ४. विपरिणामोपक्रम। इनमें बंधनोपक्रम के तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाव एवं प्रदेश ये चार भेद हैं ही किन्तु उदीरणोपक्रम के भी ये ही चार भेद हैं, उपशमनोपक्रम के भी ये ही चार भेद हैं तथा विपरिणामोपक्रम के भी ये ही चार भेद हैं। संक्रम एक करण है जिसमें बद्ध प्रकृति का बध्यमान प्रकृति में उद्वर्तन या अपवर्तन होता है। वह संक्रम भी चार प्रकार का है-प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। निधत्त और निकाचित के भी ये ही चार भेद हैं-१. प्रकृति, २. स्थिति, ३. अनुभाग और ४. प्रदेश।
विभिन्न कर्म प्रकृतियों का बंध करता हुआ जीव कुल कितनी कर्म प्रकृतियों का बंध करता है, उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है इसकी प्रस्तुत अध्ययन में विस्तृत चर्चा है। यथा-ज्ञानावरणीय कर्म को बांधता हुआ जीव सात, आठ या छह कर्म प्रकृतियों का बंधक होता है। दर्शनावरणीय को बांधते हुए भी सात, आठ या छह कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। वेदनीय कर्म को बांधता हुआ जीव सात, आठ, छह या एक कर्म प्रकृति का बंध करता है। मोहनीय कर्म को बांधता हुआ जीव सात, आठ, छह कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। आयु कर्म को बांधता हुआ जीव नियम से आठ कर्म प्रकृतियों को बांधता है। अन्तराय, नाम और गोत्र को बांधता हुआ जीव सात, आठ या छह कर्म प्रकृतियों को बांधता है। चौबीस दण्डकों में इन कर्म प्रकृतियों के बन्ध में क्या अन्तर रहता है इसका भी यहाँ निरूपण है। ___ कुछ रुचिकर प्रश्नों का समाधान भी है यथा-जैसे छद्मस्थ हंसता है तथा उत्सुक होता है वैसे क्या केवली मनुष्य भी हंसता है और उत्सुक होता है ? इसका समाधान करते हुए कहा गया है कि केवली न तो हंसता है और न उत्सुक होता है क्योंकि जीव चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से हंसते और उत्सुक होते हैं। केवली चारित्रमोहनीय कर्म का क्षय कर चुका होता है। यहाँ हंसना हास्य कर्म का एवं उत्सुक होना रति कर्म का द्योतक लगता है। विविध अपेक्षाओं से अष्टविध कर्मों के बंध का विवेचन भी महत्वपूर्ण है। स्त्री, पुरुष नपुंसक की अपेक्षा, संयत असंयत की अपेक्षा, सम्यग्दृष्टि आदि की अपेक्षा, संज्ञी असंज्ञी की अपेक्षा, भवसिद्धिक आदि की अपेक्षा, चक्षुदर्शनी आदि की अपेक्षा, पर्याप्त अपर्याप्तादि की अपेक्षा, भाषक अभाषक की अपेक्षा, परित्त अपरित्त की अपेक्षा, ज्ञानी अज्ञानी की अपेक्षा, मनोयोगी आदि की अपेक्षा, साकार, अनाकारोपयुक्त की अपेक्षा, आहारक अनाहारक की अपेक्षा, सूक्ष्म बादर की अपेक्षा और चारित्र, अचारित्र की अपेक्षा से आठ कर्म प्रकृतियों के बंध का निरूपण है। प्राणातिपात से विरत जीव सात, आठ, छह और एक कर्मप्रकृतियों को बांधता है तथा कभी वह अबन्धक (बंध रहित) भी होता है। इसके २७ भंग बनते हैं। मृषावादविरत यावत् मिथ्यादर्शनशल्य विरत जीव के सात, आठ, छह या एक प्रकृति का बंध होता है तथा कभी वह जीव अबंधक भी होता है।