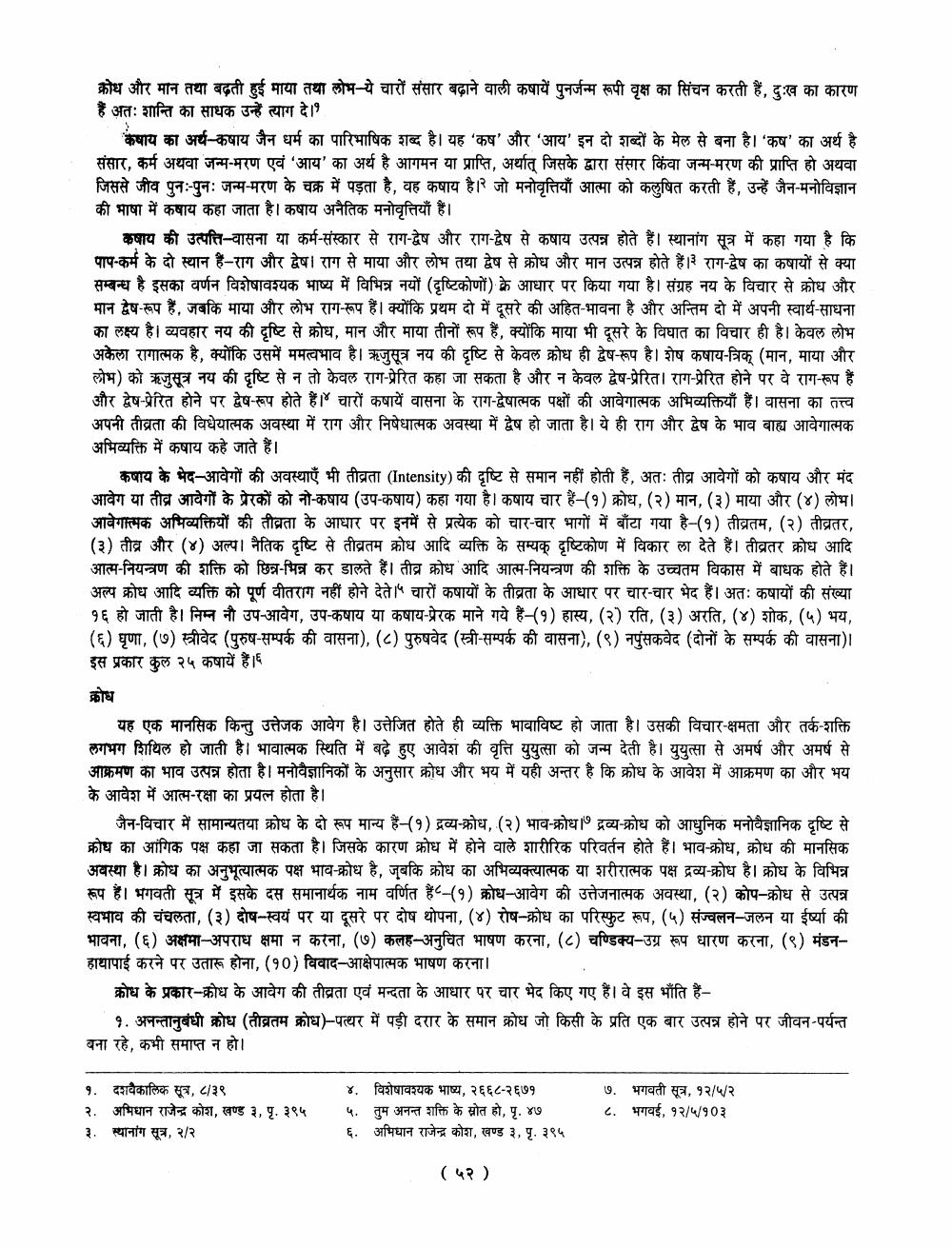________________
क्रोध और मान तथा बढ़ती हुई माया तथा लोभ-ये चारों संसार बढ़ाने वाली कषायें पुनर्जन्म रूपी वृक्ष का सिंचन करती हैं, दुःख का कारण हैं अतः शान्ति का साधक उन्हें त्याग दे।'
कषाय का अर्थ-कषाय जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है। यह 'कष' और 'आय' इन दो शब्दों के मेल से बना है। 'कष' का अर्थ है संसार, कर्म अथवा जन्म-मरण एवं 'आय' का अर्थ है आगमन या प्राप्ति, अर्थात् जिसके द्वारा संसार किंवा जन्म-मरण की प्राप्ति हो अथवा जिससे जीव पुनःपुनः जन्म-मरण के चक्र में पड़ता है, वह कषाय है। जो मनोवृत्तियाँ आत्मा को कलुषित करती हैं, उन्हें जैन-मनोविज्ञान की भाषा में कषाय कहा जाता है। कषाय अनैतिक मनोवृत्तियाँ हैं।
कषाय की उत्पत्ति-वासना या कर्म-संस्कार से राग-द्वेष और राग-द्वेष से कषाय उत्पन्न होते हैं। स्थानांग सूत्र में कहा गया है कि पाप-कर्म के दो स्थान है-राग और द्वेष। राग से माया और लोभ तथा द्वेष से क्रोध और मान उत्पन्न होते हैं।३ राग-द्वेष का कषायों से क्या सम्बन्ध है इसका वर्णन विशेषावश्यक भाष्य में विभिन्न नयों (दृष्टिकोणों) के आधार पर किया गया है। संग्रह नय के विचार से क्रोध और मान द्वेष-रूप हैं, जबकि माया और लोभ राग-रूप हैं। क्योंकि प्रथम दो में दूसरे की अहित-भावना है और अन्तिम दो में अपनी स्वार्थ-साधना का लक्ष्य है। व्यवहार नय की दृष्टि से क्रोध, मान और माया तीनों रूप हैं, क्योंकि माया भी दूसरे के विघात का विचार ही है। केवल लोभ अकेला रागात्मक है, क्योंकि उसमें ममत्वभाव है। ऋजुसूत्र नय की दृष्टि से केवल क्रोध ही द्वेष-रूप है। शेष कषाय-त्रिक (मान, माया और लोभ) को ऋजुसूत्र नय की दृष्टि से न तो केवल राग-प्रेरित कहा जा सकता है और न केवल द्वेष-प्रेरित। राग-प्रेरित होने पर वे राग-रूप हैं
और द्वेष-प्रेरित होने पर द्वेष-रूप होते हैं। चारों कषायें वासना के राग-द्वेषात्मक पक्षों की आवेगात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं। वासना का तत्त्व अपनी तीव्रता की विधेयात्मक अवस्था में राग और निषेधात्मक अवस्था में द्वेष हो जाता है। ये ही राग और द्वेष के भाव बाह्य आवेगात्मक अभिव्यक्ति में कषाय कहे जाते हैं।
कषाय के भेद-आवेगों की अवस्थाएँ भी तीव्रता (Intensity) की दृष्टि से समान नहीं होती हैं, अतः तीव्र आवेगों को कषाय और मंद आवेग या तीव्र आवेगों के प्रेरकों को नो-कषाय (उप-कषाय) कहा गया है। कषाय चार हैं-(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया और (४) लोभ । आवेगात्मक अभिव्यक्तियों की तीव्रता के आधार पर इनमें से प्रत्येक को चार-चार भागों में बाँटा गया है-(१) तीव्रतम, (२) तीव्रतर, (३) तीव्र और (४) अल्प। नैतिक दृष्टि से तीव्रतम क्रोध आदि व्यक्ति के सम्यक् दृष्टिकोण में विकार ला देते हैं। तीव्रतर क्रोध आदि आत्म-नियन्त्रण की शक्ति को छिन्न-भिन्न कर डालते हैं। तीव्र क्रोध आदि आत्म-नियन्त्रण की शक्ति के उच्चतम विकास में बाधक होते हैं। अल्प क्रोध आदि व्यक्ति को पूर्ण वीतराग नहीं होने देते।५ चारों कषायों के तीव्रता के आधार पर चार-चार भेद हैं। अतः कषायों की संख्या १६ हो जाती है। निम्न नौ उप-आवेग, उप-कषाय या कषाय-प्रेरक माने गये हैं-(१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) शोक, (५) भय, (६) घृणा, (७) स्त्रीवेद (पुरुष-सम्पर्क की वासना), (८) पुरुषवेद (स्त्री-सम्पर्क की वासना), (९) नपुंसकवेद (दोनों के सम्पर्क की वासना)। इस प्रकार कुल २५ कषायें हैं।६ क्रोध
यह एक मानसिक किन्तु उत्तेजक आवेग है। उत्तेजित होते ही व्यक्ति भावाविष्ट हो जाता है। उसकी विचार-क्षमता और तर्क-शक्ति लगभग शिथिल हो जाती है। भावात्मक स्थिति में बढ़े हुए आवेश की वृत्ति युयुत्सा को जन्म देती है। युयुत्सा से अमर्ष और अमर्ष से आक्रमण का भाव उत्पन्न होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्रोध और भय में यही अन्तर है कि क्रोध के आवेश में आक्रमण का और भय के आवेश में आत्म-रक्षा का प्रयत्न होता है।
जैन-विचार में सामान्यतया क्रोध के दो रूप मान्य हैं-(१) द्रव्य-क्रोध, (२) भाव-क्रोध। द्रव्य-क्रोध को आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रोध का आंगिक पक्ष कहा जा सकता है। जिसके कारण क्रोध में होने वाले शारीरिक परिवर्तन होते हैं। भाव-क्रोध, क्रोध की मानसिक अवस्था है। क्रोध का अनुभूत्यात्मक पक्ष भाव-क्रोध है, जबकि क्रोध का अभिव्यक्त्यात्मक या शरीरात्मक पक्ष द्रव्य-क्रोध है। क्रोध के विभिन्न रूप हैं। भगवती सूत्र में इसके दस समानार्थक नाम वर्णित हैं८-(१) क्रोध-आवेग को उत्तेजनात्मक अवस्था, (२) कोप-क्रोध से उत्पन्न स्वभाव की चंचलता, (३) दोष-स्वयं पर या दूसरे पर दोष थोपना, (४) रोष-क्रोध का परिस्फुट रूप, (५) संज्वलन-जलन या ईर्ष्या की भावना, (६) अक्षमा-अपराध क्षमा न करना, (७) कलह-अनुचित भाषण करना, (८) चण्डिक्य-उग्र रूप धारण करना, (९) मंडनहाथापाई करने पर उतारू होना, (१०) विवाद-आक्षेपात्मक भाषण करना।
क्रोध के प्रकार-क्रोध के आवेग की तीव्रता एवं मन्दता के आधार पर चार भेद किए गए हैं। वे इस भाँति हैं
१. अनन्तानुबंधी क्रोध (तीव्रतम क्रोध)-पत्थर में पड़ी दरार के समान क्रोध जो किसी के प्रति एक बार उत्पन्न होने पर जीवन-पर्यन्त बना रहे, कभी समाप्त न हो।
१. दशवकालिक सूत्र, ८/३९ २. अभिधान राजेन्द्र कोश, खण्ड ३, पृ. ३९५ ३. स्थानांग सूत्र, २/२
४. विशेषावश्यक भाष्य, २६६८-२६७१ ५. तुम अनन्त शक्ति के स्रोत हो, पृ. ४७ ६. अभिधान राजेन्द्र कोश, खण्ड ३, पृ. ३९५
७. भगवती सूत्र, १२/५/२ ८. भगवई, १२/५/१०३
(५२)