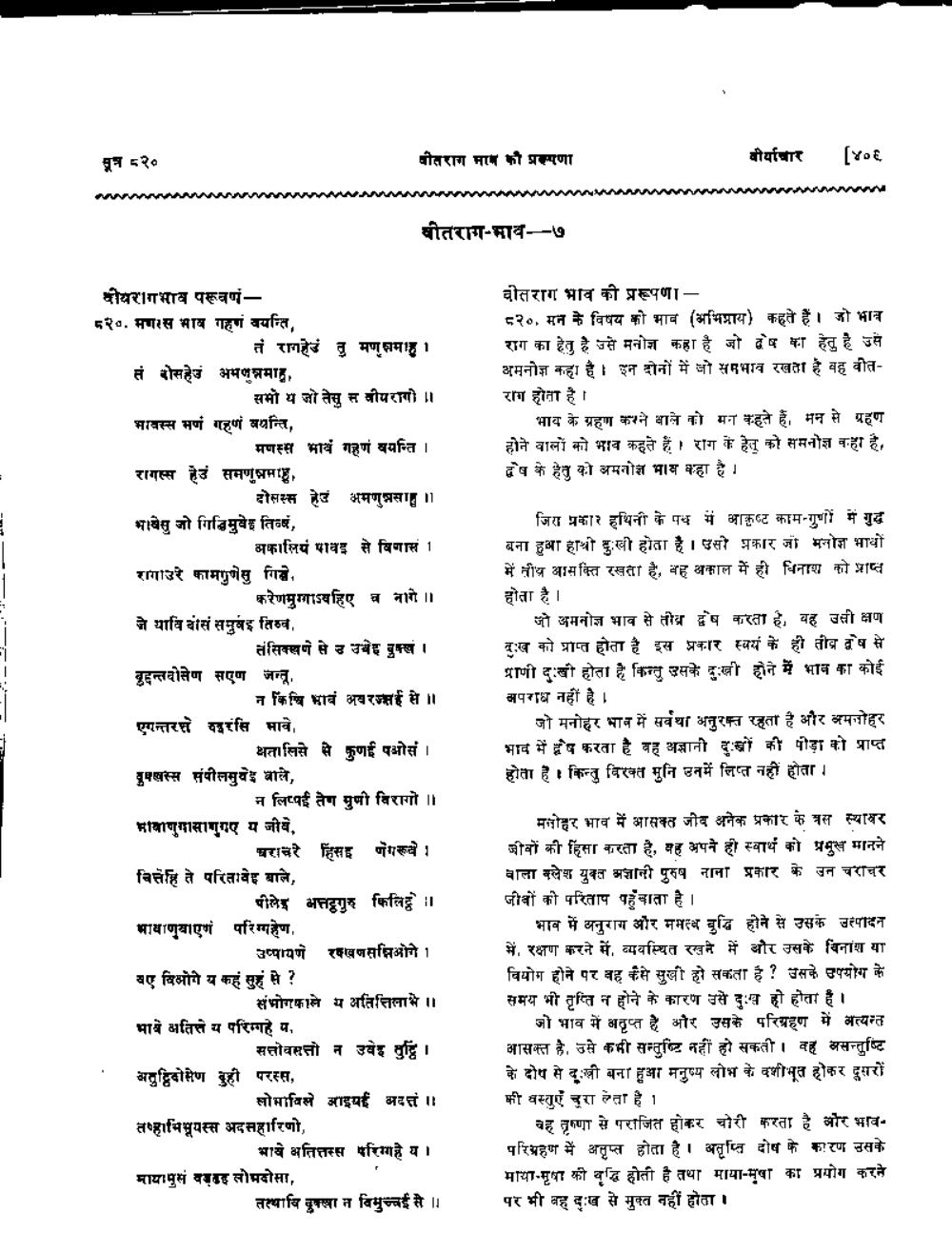________________
सूत्र ८२०
वीतराग माष को प्रपणा
वीर्याचार
[४०६
वीतराग-माव-७
वीतराग भाव की प्ररूपणा८२०, मन के विषय को भाब (अभिप्राय) कहते हैं। जो भाव राग का हेतु है उसे मनोज्ञ कहा है जो द्वेष का हेतु है उस अमनोज कहा है। इन दोनों में जो समभाव रखता है वह वीतराग होता है।
भाव के ग्रहण करने वाले को मन कहते हैं, मन से ग्रहण होने वालों को भाव कहते हैं। राग के हेतु को समनोज्ञ वहा है, द्वेष के हेतु को अमनोज्ञ भाव कहा है।
वोयरागभाव परूवर्ण१२०. मगरस भाव गहगं वयन्ति,
तं रागहेडं तु मणनमाह। सं रोसहेड अमणनमार,
समो य जो तेसु स बीयरागो। भावस्स मणं गहणं अयन्ति,
मणस्स भावं गहणं वयन्ति । रागल्स हेउं समणुनमाह,
दोसस्स हे अमणुनसा ॥ भावेसु जो गिबिमुवेझ तिवं,
अकालिय पावई से विणास 1 रागाउरे कामगुणेसु गिल्वे,
करेणमुग्गाऽवहिए व नागे ।। जे याविबांसं समुबइ तिच,
संसिक्खणे से उ उबेद चुक्ख । बुद्दन्तदोषेण सएण जन्तू.
न किंचि भावं अवरज्सई से ॥ एगन्तरसे बदरंसि भावे,
अतासिसे से कुणई पोस । पखस्स संपीलमुवेइ बाले,
न लिप्पई तेग मुणी विरागो ।। मावाणुगासागुगए य जीवे,
घराचरे हिंसइ गरूवे । चितहि ते परितावेद बाले,
पीलेइ अत्तगुरु फिलिट्ठ ।। भावाणुयाएणं परिग्रहेण,
उप्पायणे रक्षणसनिओगे। यए विओगे य कहं सुहं से?
संभोगकाले य अतित्तिलाभे ।। भावे अतित्ते य परिग्गहे य,
सत्तोवस्तो न उवेइ तुट्टि। अतुट्टिदोमेण बुही परस्स,
लोमाविले आइयई अदत्तं ।। तहामिभूयस्स अदसहारिणो,
भावे अतित्तस्स परिग्गहे य । मायामुसं वबढइ लोमदोसा,
तथापि दुक्खा न विमुच्चई से ।।
जिरा प्रकार हथिनी के पथ में आकृष्ट काम-गुणों में गुद्ध बना हुआ हाथी दुःखी होता है। उसी प्रकार जो मनोज भावों में तीव आसक्ति रखता है, वह बकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है।
जो अमनोज्ञ भाव से तीव्र द्वष करता है, वह उसी क्षण दुःख को प्राप्त होता है इस प्रकार स्वयं के ही तीव्र द्वष से प्राणी दुःखी होता है किन्तु उसके दुःखी होने में भाव का कोई अपराध नहीं है।
जो मनोहर भान में सर्वथा अनुरक्त रहता है और अमनोहर भाव में वष करता है वह अज्ञानी दुःखों की पीड़ा को प्राप्त होता है। किन्तु विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता।
मनोहर भाव में आसक्त जीव अनेक प्रकार के बस स्थावर जीवों की हिंसा करता है, वह अपने ही स्वार्थ को प्रमुख मानने वाला क्लेश युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चराचर जीवों को परिताप पहुंचाता है।
भाव में अनुराग और ममत्व बुद्धि होने से उसके उत्पादन में, रक्षण करने में, व्यवस्थित रखने में और उसके विनाश या वियोग होने पर वह कैसे सुखी हो सकता है ? उसके उपयोग के समय भी तृप्ति न होने के कारण उसे दुःख हो होता है।
जो भाव में अतृप्त है और उसके परिग्रहण में अत्यन्त आसक्त है, उसे कभी सन्तुष्टि नहीं हो सकती। वह असन्तुष्टि के दोष से दुःखी बना हुआ मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर दुसरों की वस्तुएं चुरा लेता है ।
वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और भावपरिग्रहण में अतृप्त होता है । अतृप्ति दोष के कारण उसके माया-मृषा की वृद्धि होती है तथा माया-मषा का प्रयोग करने पर भी बह दुःख से मुक्त नहीं होता।