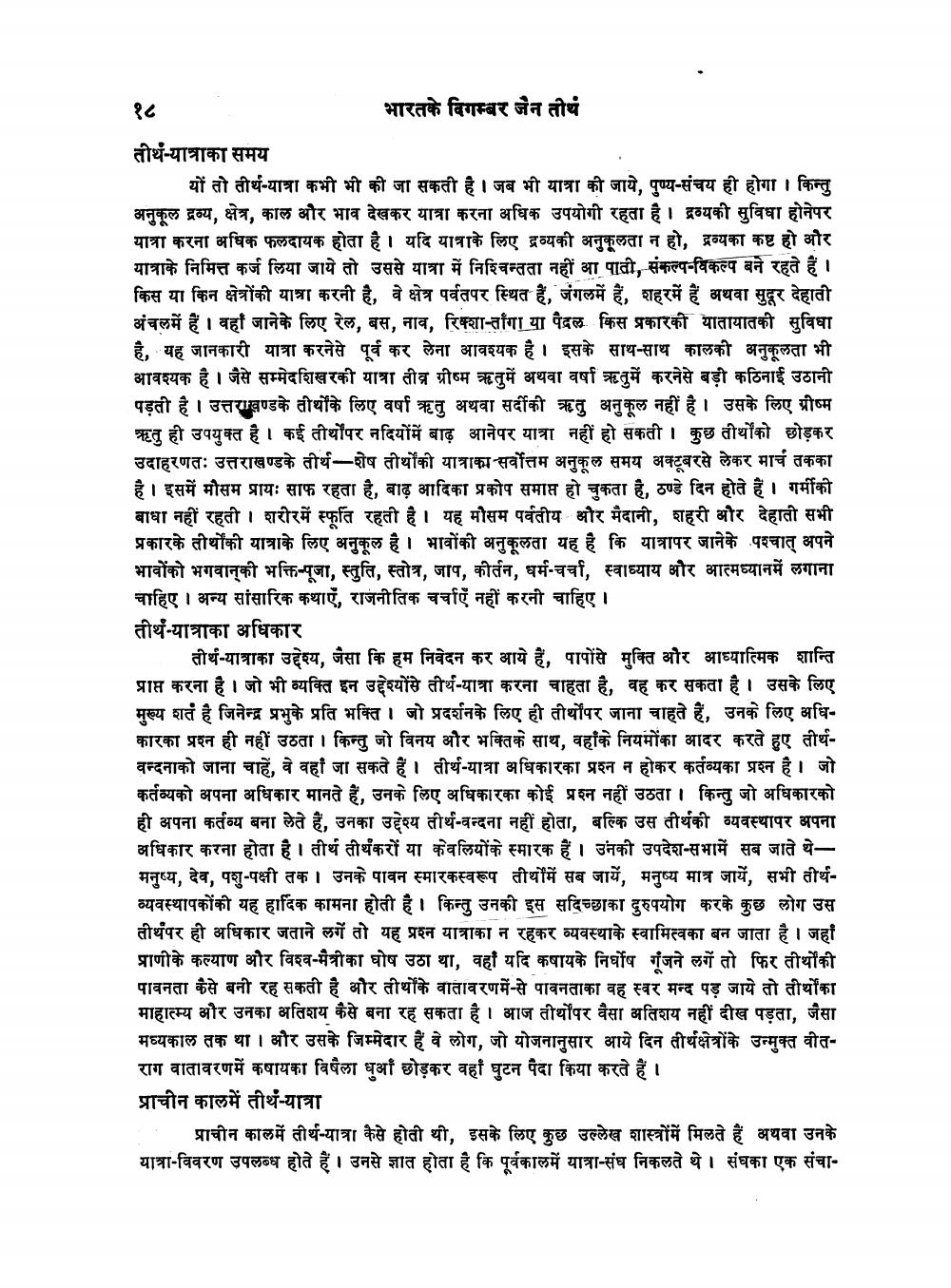________________
१८
भारतके दिगम्बर जैन तीर्थ
तीर्थ-यात्राका समय
यों तो तीर्थ यात्रा कभी भी की जा सकती है। जब भी यात्रा की जाये, पुण्य-संचय ही होगा। किन्तु अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव देखकर यात्रा करना अधिक उपयोगी रहता है। द्रव्यकी सुविधा होनेपर यात्रा करना अधिक फलदायक होता है। यदि यात्राके लिए द्रव्यकी अनुकूलता न हो, द्रव्यका कष्ट हो और यात्राके निमित्त कर्ज लिया जाये तो उससे यात्रा में निश्चिन्तता नहीं आ पाती, संकल्प-विकल्प बने रहते हैं । किस या किन क्षेत्रोंकी यात्रा करनी है, वे क्षेत्र पर्वतपर स्थित हैं, जंगलमें हैं, शहरमें हैं अथवा सुदूर देहाती अंचलमें हैं । वहाँ जानेके लिए रेल, बस, नाव, रिक्शा-तांगा या पैदल किस प्रकारको यातायातकी सुविधा है, यह जानकारी यात्रा करनेसे पूर्व कर लेना आवश्यक है। इसके साथ-साथ कालकी अनुकूलता भी आवश्यक है। जैसे सम्मेदशिखरकी यात्रा तीव्र ग्रीष्म ऋतुमें अथवा वर्षा ऋतुमें करनेसे बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है । उत्तराखण्डके तीर्थोंके लिए वर्षा ऋतु अथवा सर्दीकी ऋतु अनुकूल नहीं है। उसके लिए ग्रीष्म ऋतु ही उपयुक्त है । कई तीर्थोपर नदियों में बाढ़ आनेपर यात्रा नहीं हो सकती। कुछ तीर्थोंको छोड़कर उदाहरणतः उत्तराखण्डके तीर्थ-शेष तीर्थोंकी यात्राका सर्वोत्तम अनुकूल समय अक्टूबरसे लेकर मार्च तकका है । इसमें मौसम प्रायः साफ रहता है, बाढ़ आदिका प्रकोप समाप्त हो चुकता है, ठण्डे दिन होते हैं । गर्मीकी बाधा नहीं रहती। शरीर में स्फूति रहती है। यह मौसम पर्वतीय और मैदानी, शहरी और देहाती सभी प्रकारके तीर्थोंकी यात्राके लिए अनुकूल है। भावोंकी अनुकूलता यह है कि यात्रापर जानेके पश्चात् अपने भावोंको भगवान्की भक्ति-पूजा, स्तुति, स्तोत्र, जाप, कीर्तन, धर्म-चचों, स्वाध्याय और आत्मध्यान लगाना चाहिए । अन्य सांसारिक कथाएँ, राजनीतिक चर्चाएँ नहीं करनी चाहिए। तीर्थ यात्राका अधिकार
तीर्थ-यात्राका उद्देश्य, जैसा कि हम निवेदन कर आये हैं, पापोंसे मुक्ति और आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करना है। जो भी व्यक्ति इन उद्देश्योंसे तीर्थ-यात्रा करना चाहता है, वह कर सकता है। उसके लिए मुख्य शतं है जिनेन्द्र प्रभुके प्रति भक्ति । जो प्रदर्शनके लिए ही तीर्थोपर जाना चाहते हैं, उनके लिए अधिकारका प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु जो विनय और भक्तिके साथ, वहाँके नियमोंका आदर करते हुए तीर्थवन्दनाको जाना चाहें, वे वहां जा सकते हैं। तीर्थ-यात्रा अधिकारका प्रश्न न होकर कर्तव्यका प्रश्न है। जो कर्तव्यको अपना अधिकार मानते हैं, उनके लिए अधिकारका कोई प्रश्न नहीं उठता। किन्तु जो अधिकारको ही अपना कर्तव्य बना लेते हैं, उनका उद्देश्य तीर्थ-वन्दना नहीं होता, बल्कि उस तीर्थकी व्यवस्थापर अपना अधिकार करना होता है। तीर्थ तीर्थंकरों या केवलियोंके स्मारक हैं। उनकी उपदेश-सभामें सब जाते थेमनुष्य, देव, पशु-पक्षी तक । उनके पावन स्मारकस्वरूप तीर्थोंमें सब जायें, मनुष्य मात्र जायें, सभी तीर्थव्यवस्थापकोंकी यह हार्दिक कामना होती है। किन्तु उनकी इस सदिच्छाका दुरुपयोग करके कुछ लोग उस तीर्थपर ही अधिकार जताने लगें तो यह प्रश्न यात्राका न रहकर व्यवस्थाके स्वामित्वका बन जाता है । जहाँ प्राणीके कल्याण और विश्व-मैत्रीका घोष उठा था, वहाँ यदि कषायके निर्घोष गंजने लगें तो फिर तीर्थों की पावनता कैसे बनी रह सकती है और तीर्थोके वातावरणमें-से पावनताका वह स्वर मन्द पड़ जाये तो तीर्थों का माहात्म्य और उनका अतिशय कैसे बना रह सकता है। आज तीर्थोंपर वैसा अतिशय नहीं दीख पड़ता, जैसा मध्यकाल तक था। और उसके जिम्मेदार हैं वे लोग, जो योजनानुसार आये दिन तीर्थक्षेत्रोंके उन्मुक्त वीतराग वातावरणमें कषायका विषैला धुआँ छोड़कर वहाँ घुटन पैदा किया करते हैं। प्राचीन कालमें तीर्थ-यात्रा
प्राचीन कालमें तीर्थ यात्रा कैसे होती थी, इसके लिए कुछ उल्लेख शास्त्रोंमें मिलते हैं अथवा उनके यात्रा-विवरण उपलब्ध होते हैं । उनसे ज्ञात होता है कि पूर्वकालमें यात्रा-संघ निकलते थे। संघका एक संचा