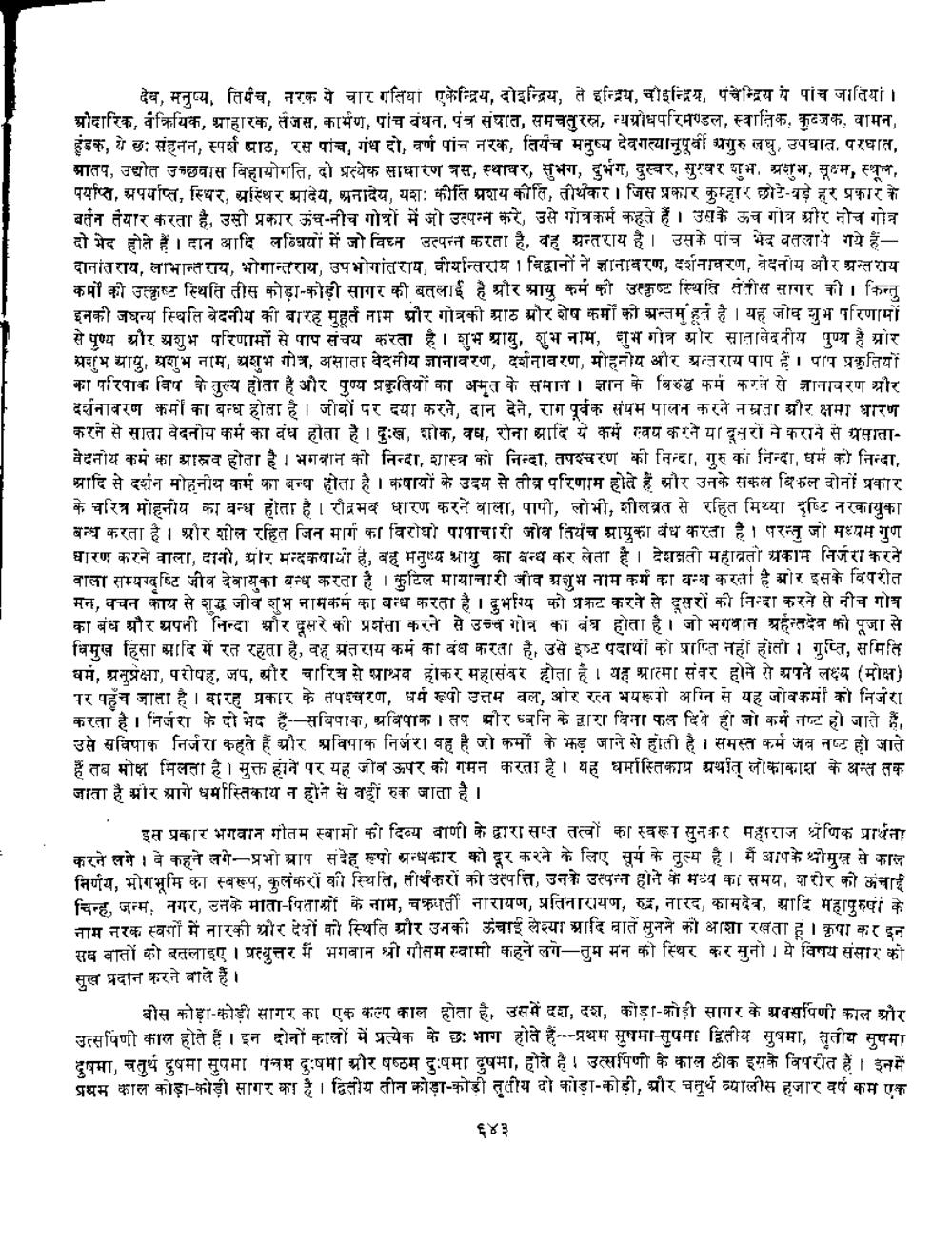________________
देव, मनुष्य, तिच, नरक ये चार गतियां एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय ये पांच जातियां । प्रौदारिक, वक्रियिक, पाहारक, तेजस, कार्मण, पांच बंधन, पंच संघात, समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वातिक, कुटजक, वामन, हुंडक, ये छः संहनन, स्पर्श पाठ, रस पांच, गंध दो, वर्ण पांच नरक, तिर्यंच मनुष्य देवगत्यानुपूर्वी अगुरु लघु, उपघात, परघात,
आतप, उद्योत जल्छवास बिहायोगति, दो प्रत्येक साधारण त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, दुस्वर, सुरवर शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, स्थूल, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर मादेय, अनादेय, यशः कीर्ति प्रशय कीति, तीर्थकर । जिस प्रकार कुम्हार छोटे-बड़े हर प्रकार के बर्तन तैयार करता है, उसी प्रकार ऊंच-नीच गोत्रों में जो उत्पन्न करे, उसे गोत्रकर्म कहते हैं। उसके ऊच गोत्र और नीच गोत्र दो भेद होते हैं । दान आदि लब्धियों में जो विघ्न उत्पन्न करता है, वह अन्तराय है। उसके पांच भेद बतलाये गये हैंदानांतराय, लाभान्त राय, भोगान्तराय, उपभोगांतराय, वीर्यान्तराय । विद्वानों ने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्त राय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ा-कोड़ी सागर की बतलाई है और आयु कम की उत्कृष्ट स्थिति संतीस सागर की। किन्तु इनकी जघन्य स्थिति वेदनीय की बारह मुहर्त नाम और गोत्रको पाठ और शेष कर्मों को अन्तमुहूर्त है । यह जोव शुभ परिणामों से पुण्य और अशुभ परिणामों से पाप संचय करता है। शुभ प्रायु, शुभ नाम, शुभ गोत्र और सातावेदनीय पुण्य है पोर अशुभ मायु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, असाता बेदनीय ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अत्तराय पाप है। पाप प्रकृतियों का परिपाक विष के तुल्य होता है और पुण्य प्रकृतियों का अमृत के समान। ज्ञान के विरुद्ध कर्म करने से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों का बन्ध होता है। जीवों पर दया करने, दान देने, राग पूर्वक संयम पालन करने नम्रता और क्षमा धारण करने से माता वेदनीय कर्म का बंध होता है। दुःख, शोक, वय, रोना आदि ये कर्म स्वयं करने या दुसरों ने कराने से असातावेदनोय कर्म का आस्रव होता है। भगवान को निन्दा, शास्त्र को निन्दा, तपश्चरण को निन्दा, गुरु को निन्दा, धर्म को निन्दा, आदि से दर्शन मोहनीय कर्म का बन्ध होता है । कषायों के उदय से तीव्र परिणाम होते हैं और उनके सकल विफल दोनों प्रकार के चरित्र मोहनीय का बन्ध होता है। रौद्रभव धारण करने वाला, पापी, लोभी, शीलवत से रहित मिथ्या दृष्टिनरकायुका बन्ध करता है। और शील रहित जिन मार्ग का विरोधो पापाचारी जोव तिर्यच आयुका बंध करता है। परन्तु जो मध्यम गुण धारण करने वाला, दानो, ओर मन्दकषायी है, वह मनुष्य आयु का बन्ध कर लेता है। देशमती महानतो काम निर्जरा करने वाला सम्यग्दष्टि जीव देवायुका बन्ध करता है । कुटिल मायाचारी जीव अशुभ नाम कर्म का बन्य करता है और इसके विपरीत मन, वचन काय से शुद्ध जीव शुभ नामकम का बन्ध करता है । दुर्भाग्य को प्रकट करने से दूसरों की निन्दा करने से नीच गोत्र का बंध और अपनी निन्दा और दूसरे की प्रशंसा करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। जो भगवान अर्हन्तदेव की पूजा से विमुख हिंसा प्रादि में रत रहता है, वह अंतराय कर्म का बंध करता है, उसे इष्ट पदार्थों को प्राप्ति नहीं होती। गुप्ति, समिति धर्म, अनुप्रेक्षा, परोषह, जप, और चारित्र से पाश्रव होकर महासंबर होता है। यह प्रात्मा संवर होने से अपने लक्ष्य (मोक्ष) पर पहुँच जाता है। बारह प्रकार के तपश्चरण, धर्म रूपी उत्तम बल, ओर रत्न भयरूपो अग्नि से यह जोवकर्मा को निजेरा करता है। निर्जरा के दो भेद हैं--सविपाक, अविपाक । तप और ध्वनि के द्वारा बिना फल दिये हो जो कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं और अविपाक निर्जरा वह है जो कर्मों के झड़ जाने से होती है । समस्त कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तब मोक्ष मिलता है। मुक्त होने पर यह जीव ऊपर को गमन करता है। यह धर्मास्तिकाय अर्थात् लोकाकाश के अन्त तक जाता है और आगे धर्मास्तिकाय न होने से वहीं रुक जाता है।
इस प्रकार भगवान गौतम स्वामी को दिव्य वाणी के द्वारा सप्त तत्वों का स्वरूप सुनकर महाराज श्रेणिक प्रार्थना करने लगे। वे कहने लगे-प्रभो पाप संदेह रूपो अन्धकार को दूर करने के लिए सूर्य के तुल्य है। मैं आपके थोमस से काल निर्णय. भोगभूमि का स्वरूप, कूलंकरों की स्थिति, तीर्थंकरों की उत्पत्ति, उनके उत्पन्न होने के मध्य का समय, यारीर को भाई चिन्ह, जन्म, नगर, उनके माता-पितानों के नाम, चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र, नारद, कामदेव, ग्रादि महापुरुषों के नाम नरक स्वर्गों में नारकी और देवों वो स्थिति और उनकी ऊंचाई लेश्या आदि बातें सुनने को आशा रखता है। कृपा करदन सब बातों को बतलाइए । प्रत्युत्तर में भगवान श्री गौतम स्वामी कहने लगे-तुम मन को स्थिर कर सुनो । ये विषय संसारको सुख प्रदान करने वाले हैं।
बीस कोड़ा-कोड़ी सागर का एक करप काल होता है, उसमें दा, दश, कोड़ा-कोड़ी सागर के प्रवसपिणी काल और उत्सपिणी काल होते हैं । इन दोनों कालों में प्रत्येक के छः भाग होते हैं--प्रथम सुषमा सुपमा द्वितीय सुषमा, तृतीय सुषमा दुषमा, चतुर्थ दुषमा सुपमा पंचम दुःषमा और षष्ठम दुःषमा दुषमा, होते है। उत्सपिणी के काल ठीक इसके विपरीत हैं। इनमें प्रथम काल कोड़ा-कोड़ी सागर का है। द्वितीय तीन कोड़ा-कोड़ी तृतीय दो कोड़ा-कोड़ी, और चतुर्थ व्यालीस हजार वर्ष कम एक