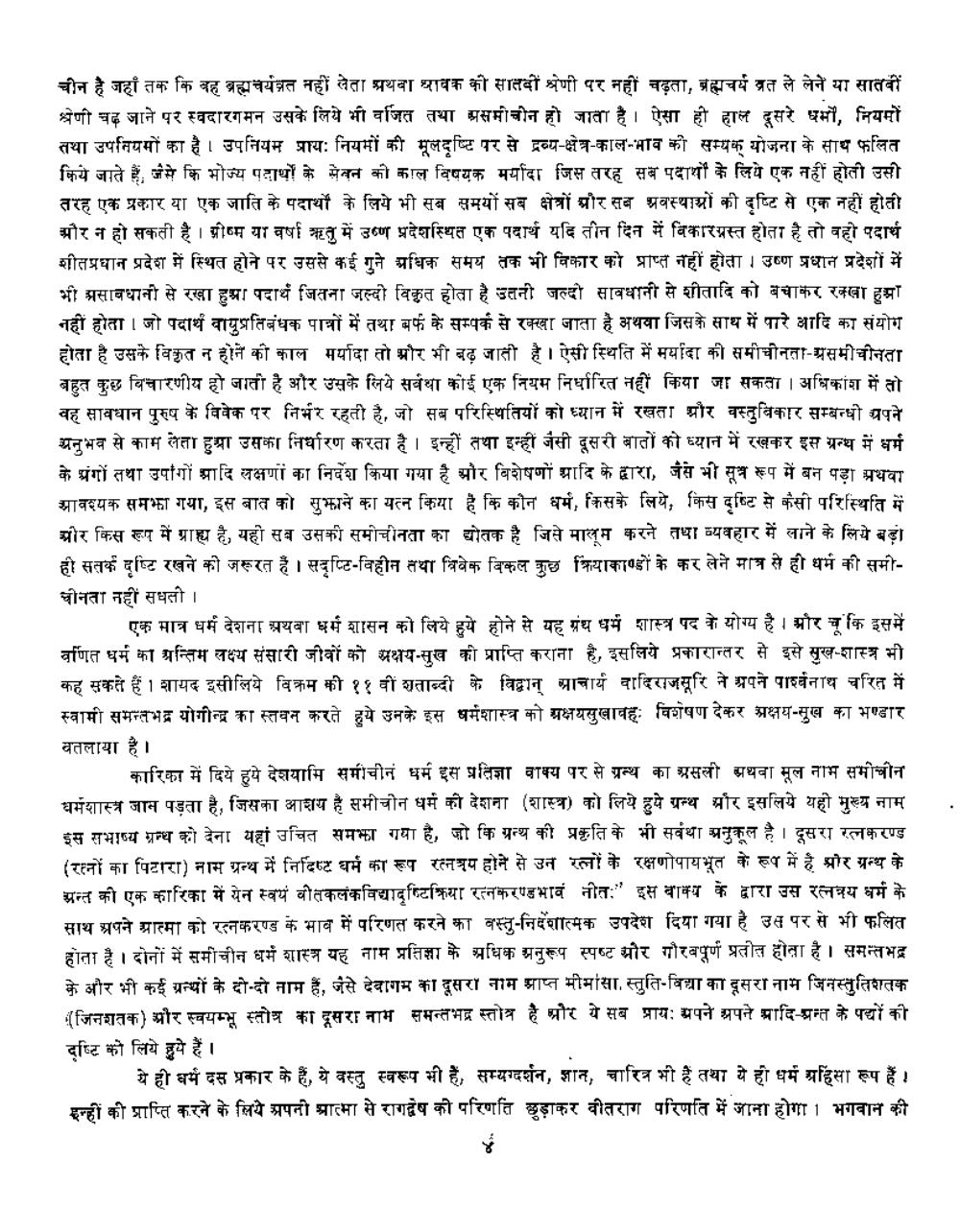________________
चीन है जहाँ तक कि वह ब्रह्मचर्यत्रत नहीं लेता अथवा धावक को सातदों श्रेणी पर नहीं चढ़ता, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेने या सातवीं श्रेणी चढ़ जाने पर स्वदारगमन उसके लिये भी वजित तथा असमीचीन हो जाता है। ऐसा ही हाल दुसरे धर्मों, नियमों तथा उपनियमों का है। उपनियम प्राय: नियमों की मूलदृष्टि पर से द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की सम्यक योजना के साथ फलित किये जाते हैं, जैसे कि भोज्य पदार्थों के सेवन को काल विषयक मर्यादा जिस तरह सब पदार्थों के लिये एक नहीं होती उसी तरह एक प्रकार या एक जाति के पदार्थों के लिये भी सब समयों सब क्षेत्रों और सब अवस्थाओं की दृष्टि से एक नहीं होती और न हो सकती है । ग्रीष्म या वर्षा ऋतु में उष्ण प्रदेशस्थित एक पदार्थ यदि तीन दिन में विकारग्रस्त होता है तो वही पदार्थ शीतप्रधान प्रदेश में स्थित होने पर उससे कई गुने अधिक समय तक भी विकार को प्राप्त नहीं होता । उष्ण प्रधान प्रदेशों में भी असावधानी से रखा हुप्रा पदार्थ जितना जल्दी विकृत होता है उतनी जल्दी सावधानी से शीतादि को बचाकर रखा हमा नहीं होता । जो पदार्थ वायुप्रतिबंधक पात्रों में तथा बर्फ के सम्पर्क से रक्खा जाता है अथवा जिसके साथ में पारे आदि का संयोग होता है उसके विकृत न होने की काल मर्यादा तो और भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मर्यादा की समीचीनता-असमीचीनता बहुत कुछ विचारणीय हो जाती है और उसके लिये सर्वथा कोई एक नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता । अधिकांश में तो वह सावधान पुरुष के विवेक पर निर्भर रहती है, जो सब परिस्थितियों को ध्यान में रखता और वस्तुबिकार सम्बन्धी अपने अनुभव से काम लेता हुया उसका निर्धारण करता है। इन्हीं तथा इन्हीं जैसी दुसरी बातों को ध्यान में रखकर इस ग्रन्थ में धर्म के अंगों तथा उपांगों आदि लक्षणों का निर्देश किया गया है और विशेषणों आदि के द्वारा, जैसे भी सूत्र रूप में बन पड़ा अथवा आवश्यक समझा गया, इस बात को सुझाने का यत्न किया है कि कौन' धर्म, किसके लिये, किस दृष्टि से कैसी परिस्थिति में और किस रूप में ग्राह्य है, यही सब उसकी समीचीनता का द्योतक है जिसे मालूम करने तथा व्यवहार में लाने के लिये बड़ी ही सतर्क दृष्टि रखने की जरूरत हैं । सदृष्टि-विहीन तथा विवेक विकल कूछ त्रियाकाण्डों के कर लेने मात्र से ही धर्म की समीचीनता नहीं सधती।
एक मात्र धर्म देशना अथवा धर्म शासन को लिये हये होने से यह ग्रंथ धर्म शास्त्र पद के योग्य है । और चुकि इसमें वर्णित धर्म का अन्तिम लक्ष्य संसारी जीवों को अक्षय-सूख की प्राप्ति कराना है, इसलिये प्रकारान्तर से इसे सुख-शास्त्र भी कह सकते हैं । शायद इसीलिये विक्रम की ११ वीं शताब्दी के विद्वान प्राचार्य वादिराजसूरि ने अपने पार्श्वनाथ चरित में स्वामी समन्तभद्र योगीन्द्र का स्तवन करते हुये उनके इस धर्मशास्त्र को अक्षयसुखावहः विशेषण देकर अक्षय-सुख का भण्डार बतलाया है।
कारिका में दिये हये देशयामि समीचीनं धर्म इस प्रतिज्ञा वाक्य पर से ग्रन्थ का असली अथवा मूल नाम समीचीन धर्मशास्त्र जान पड़ता है, जिसका आशय है समीचीन धर्म की देशना (शास्त्र) को लिये हुये ग्रन्थ और इसलिये यही मुख्य नाम इस सभाष्य मन्ध को देना यहां उचित समझा गया है, जो कि ग्रन्थ की प्रकृति के भी सर्वथा अनुकूल है। दुसरा रत्नकरण्ड (रत्नों का पिटारा) नाम ग्रन्थ में निर्दिष्ट धर्म का रूप रत्नत्रय होने से उन रत्नों के रक्षणोपायभूत के रूप में है और ग्रन्थ के अन्त की एक कारिका में येन स्वयं बीतकलंकविद्यादृष्टिक्रिया रत्नकरण्ड भावं नीतः" इस वाक्य के द्वारा उस रत्नत्रय धर्म के साथ अपने प्रात्मा को रत्नकरण्ड के भाव में परिणत करने का वस्तु-निर्देशात्मक उपदेश दिया गया है उस पर से भी फलित होता है । दोनों में समीचीन धर्म शास्त्र यह नाम प्रतिज्ञा के अधिक अनुरूप स्पष्ट और गौरवपूर्ण प्रतीत होता है। समन्तभद्र के और भी कई ग्रन्थों के दो-दो नाम हैं, जैसे देवागम का दूसरा नाम प्राप्त मीमांसा, स्तुति-विद्या का दूसरा नाम जिनस्तुतिशतक (जिनशतक) और स्वयम्भू स्तोत्र का दूसरा नाम समन्तभद्र स्तोत्र है और ये सब प्राय: अपने अपने प्रादि-अन्त के पद्यों की दृष्टि को लिये हुये हैं।
ये ही धर्म दस प्रकार के हैं, ये वस्तु स्वरूप भी हैं, सम्यग्दर्शन, शान, चारित्र भी है तथा ये ही धर्म अहिंसा रूप हैं। हन्दी की प्राप्ति करने के लिये अपनी प्रात्मा से रागद्वेष की परिणति छुड़ाकर वीतराग परिणति में जाना होगा। भगवान की