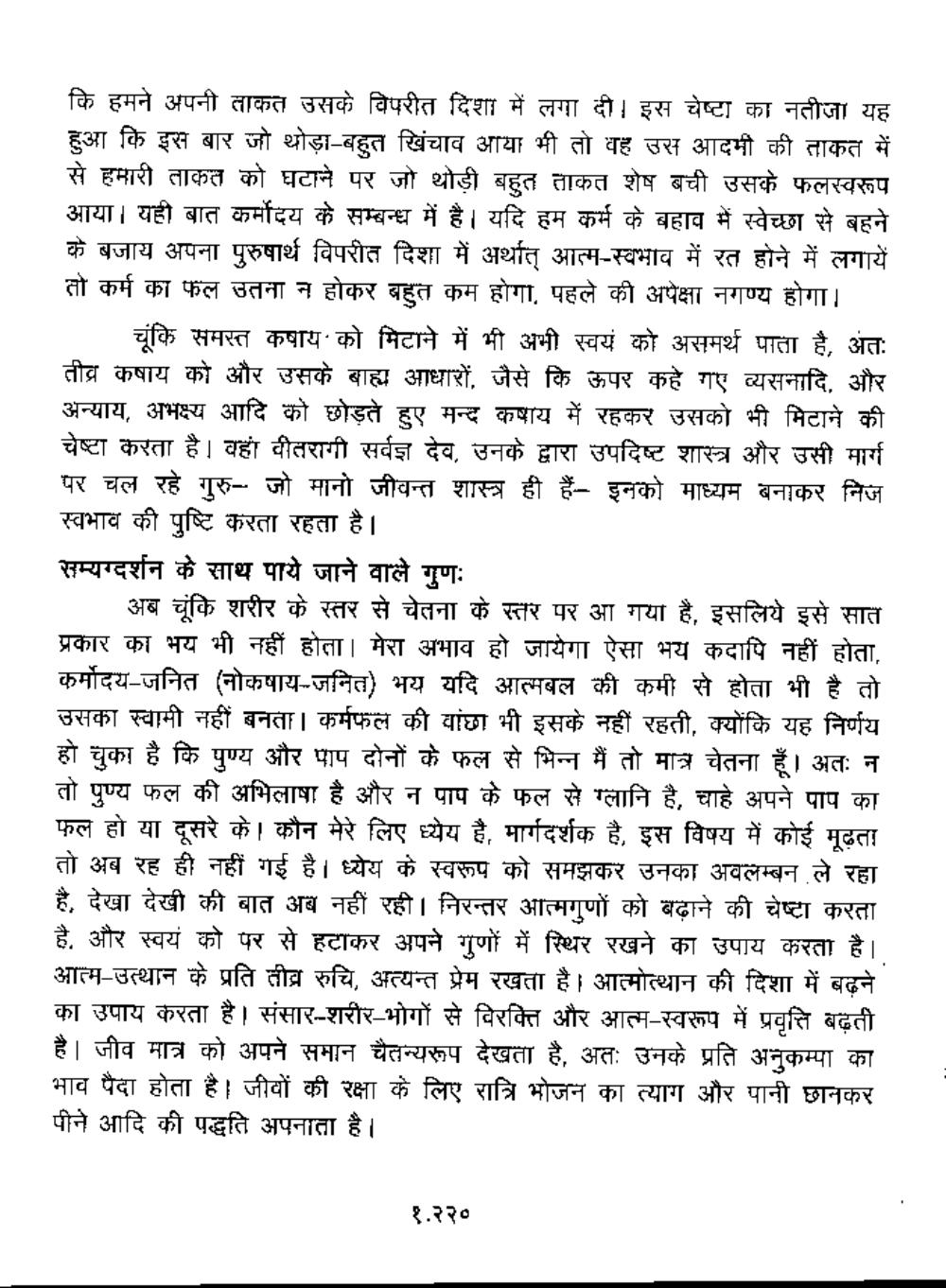________________
कि हमने अपनी ताकत उसके विपरीत दिशा में लगा दी। इस चेष्टा का नतीजा यह हुआ कि इस बार जो थोड़ा-बहुत खिंचाव आया भी तो वह उस आदमी की ताकत में से हमारी ताकत को घटाने पर जो थोड़ी बहुत ताकत शेष बची उसके फलस्वरूप आया। यही बात कर्मोदय के सम्बन्ध में है। यदि हम कर्म के बहाव में स्वेच्छा से बहने के बजाय अपना पुरुषार्थ विपरीत दिशा में अर्थात् आत्म-स्वभाव में रत होने में लगायें तो कर्म का फल उतना न होकर बहुत कम होगा. पहले की अपेक्षा नगण्य होगा।
चूंकि समस्त कषाय को मिटाने में भी अभी स्वयं को असमर्थ पाता है, अंतः तीव्र कषाय को और उसके बाह्य आधारों, जैसे कि ऊपर कहे गए व्यसनादि, और अन्याय, अभक्ष्य आदि को छोड़ते हुए मन्द कषाय में रहकर उसको भी मिटाने की चेष्टा करता है। वहीं वीतरागी सर्वज्ञ देव, उनके द्वारा उपदिष्ट शास्त्र और उसी मार्ग पर चल रहे गुरु-- जो मानो जीवन्त शास्त्र ही हैं- इनको माध्यम बनाकर निज स्वभाव की पुष्टि करता रहता है। सम्यग्दर्शन के साथ पाये जाने वाले गुणः
अब चूंकि शरीर के स्तर से चेतना के स्तर पर आ गया है, इसलिये इसे सात प्रकार का भय भी नहीं होता। मेरा अभाव हो जायेगा ऐसा भय कदापि नहीं होता, कर्मोदय-जनित (नोकषाय-जनित) भय यदि आत्मबल की कमी से होता भी है तो उसका स्वामी नहीं बनता। कर्मफल की वांछा भी इसके नहीं रहती, क्योंकि यह निर्णय हो चुका है कि पुण्य और पाप दोनों के फल से भिन्न मैं तो मात्र चेतना हूँ। अतः न तो पुण्य फल की अभिलाषा है और न पाप के फल से ग्लानि है, चाहे अपने पाप का फल हो या दूसरे के। कौन मेरे लिए ध्येय है, मार्गदर्शक है, इस विषय में कोई मूढ़ता तो अब रह ही नहीं गई है। ध्येय के स्वरूप को समझकर उनका अवलम्बन ले रहा है, देखा देखी की बात अब नहीं रही। निरन्तर आत्मगुणों को बढ़ाने की चेष्टा करता है. और स्वयं को पर से हटाकर अपने गुणों में स्थिर रखने का उपाय करता है। आत्म-उत्थान के प्रति तीव्र रुचि, अत्यन्त प्रेम रखता है। आत्मोत्थान की दिशा में बढ़ने का उपाय करता है। संसार-शरीर-भोगों से विरक्ति और आत्म-स्वरूप में प्रवृत्ति बढ़ती है। जीव मात्र को अपने समान चैतन्यरूप देखता है, अत: उनके प्रति अनुकम्पा का भाव पैदा होता है। जीवों की रक्षा के लिए रात्रि भोजन का त्याग और पानी छानकर पीने आदि की पद्धति अपनाता है।
१.२२०