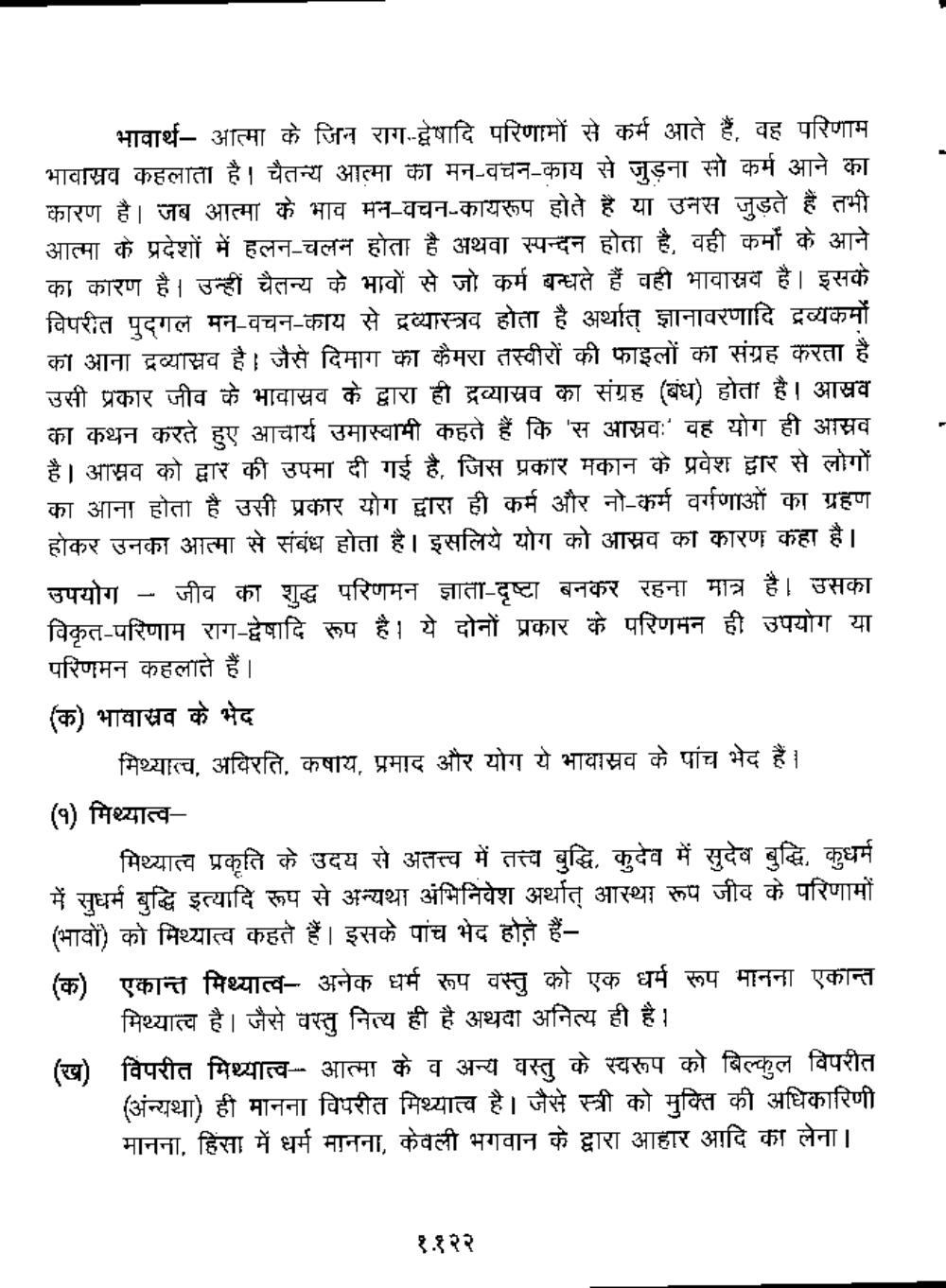________________
भावार्थ- आत्मा के जिन राग-द्वेषादि परिणामों से कर्म आते हैं, वह परिणाम भावास्रव कहलाता है। चैतन्य आत्मा का मन-वचन-काय से जुड़ना सो कर्म आने का कारण है। जब आत्मा के भाव मन-वचन-कायरूप होते है या उनस जुड़ते हैं तभी आत्मा के प्रदेशों में हलन-चलन होता है अथवा स्पन्दन होता है, वही कर्मों के आने का कारण है। उन्हीं चैतन्य के भावों से जो कर्म बन्धते हैं वही भावास्रव है। इसके विपरीत पुदगल मन-वचन-काय से द्रव्यास्त्रव होता है अर्थात् ज्ञानावरणादि द्रव्यकों का आना द्रव्यानव है। जैसे दिमाग का कैमरा तस्वीरों की फाइलों का संग्रह करता है उसी प्रकार जीव के भावास्रव के द्वारा ही द्रव्यास्रव का संग्रह (बंध) होता है। आस्रव का कथन करते हुए आचार्य उमास्वामी कहते हैं कि 'स आस्रवः' वह योग ही आम्रव है। आनव को द्वार की उपमा दी गई है, जिस प्रकार मकान के प्रवेश द्वार से लोगों का आना होता है उसी प्रकार योग द्वारा ही कर्म और नो-कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होकर उनका आत्मा से संबंध होता है। इसलिये योग को आस्रव का कारण कहा है। उपयोग - जीव का शुद्ध परिणमन ज्ञाता-दृष्टा बनकर रहना मात्र है। उसका विकृत-परिणाम राग-द्वेषादि रूप है। ये दोनों प्रकार के परिणमन ही उपयोग या परिणमन कहलाते हैं। (क) भावासव के भेद
मिथ्यात्च, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग ये भावानव के पांच भेद हैं। (१) मिथ्यात्व
मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से अतत्त्व में तत्त्व बुद्धि, कुदेव में सुदेव बुद्धि, कुधर्म में सुधर्म बुद्धि इत्यादि रूप से अन्यथा अंभिनिवेश अर्थात् आस्था रूप जीव के परिणामों (भावों) को मिथ्यात्व कहते हैं। इसके पांच भेद होते हैं(क) एकान्त मिथ्यात्व- अनेक धर्म रूप वस्तु को एक धर्म रूप मानना एकान्त
मिथ्यात्व है। जैसे वस्तु नित्य ही है अथदा अनित्य ही है। (ख) विपरीत मिथ्यात्व- आत्मा के व अन्य वस्तु के स्वरूप को बिल्कुल विपरीत
(अंन्यथा) ही मानना विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे स्त्री को मुक्ति की अधिकारिणी मानना, हिंसा में धर्म मानना, केवली भगवान के द्वारा आहार आदि का लेना।
१.१२२