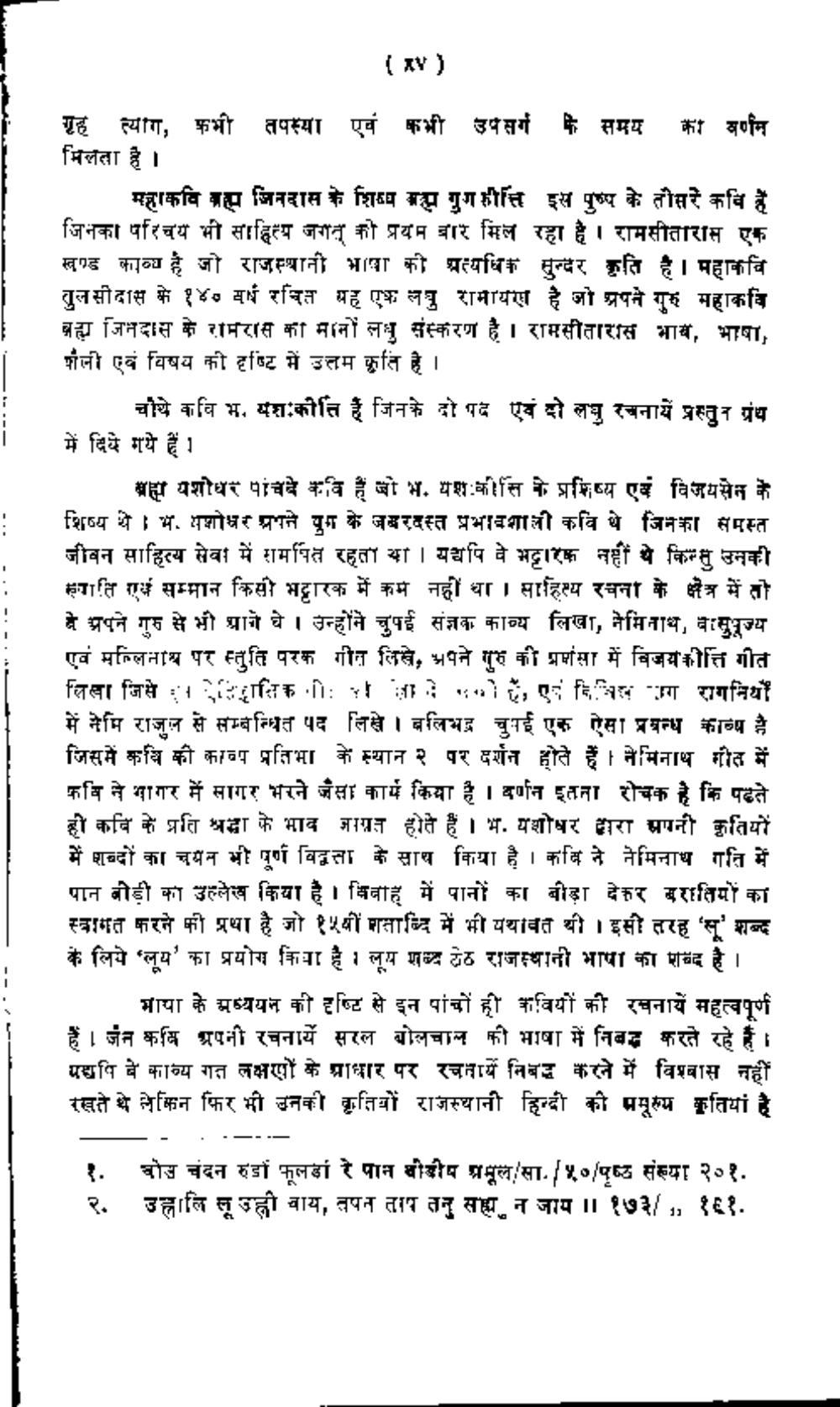________________
(v)
गृह त्याग, फभी तपस्या एवं कभी उपसर्ग के समय का वर्णन मिलता है।
महाकवि ब्रह्म जिनदास के शिष्य मम गुग कीति इस पुरुष के तीसरे कवि है जिनका परिचय भी साहित्य जगत् को प्रथम बार मिल रहा है । रामसीतारास एक स्खण्ड काव्य है जो राजस्थानी भाषा की अत्यधिक सुन्दर कृति है। महाकवि तुलसी दास के १४० मई रचित' यह एक लघु रामायण है जो अपने गुरु महाकवि ब्रह्म जिनदास के रामरास का मानों लधु संस्करण है । रामसीतारास भाब, भाषा, शानी एवं विषय की दृष्टि में उत्तम कृति है ।
___ चौथे कवि भ, यशःकोत्ति हैं जिनके दो पद एवं दो लघु रचनायें प्रस्तुत ग्रंथ में दिये गये हैं।
ब्रह्मा यशोधर पांचवे कवि हैं जो भ. यश कीसि के प्रशिष्य एवं विजयसेन के शिष्य थे। म. पशोधर प्रपने युग के जबरदस्त प्रभावशाली कवि थे जिनका समस्त जीवन साहित्य सेवा में समर्पित रहता था । यद्यपि वे भट्टारक नहीं थे किन्तु उनकी ख्याति एवं सम्मान किसी भद्रारक में कम नहीं था । साहित्य रचना के क्षेत्र में तो ने अपने गुरु से भी प्रागे घे । उन्होंने चुपई संज्ञक काव्य लिखा, नेमिनाथ, वासुभुज्य एवं मल्लिनाथ पर स्तुति परक गीत लिखे, अपने गुरु की प्रशंसा में विजय कीत्ति गीत लिखा जिसे : हासिक गी: ला है, एक विवाद ग रागनियों में नेमि राजुल से सम्बन्धित पद लिखे । बलिभद्र चुमई एक ऐसा प्रबन्ध काव्य है जिसमें कवि की काप प्रतिभा के स्थान २ पर दर्शन होते हैं । नेमिनाथ गीत में कवि ने गागर में सागर भरने जैसा कार्य किया है । वर्णन इतना रोचक है कि पढ़ते ही कवि के प्रति श्रद्धा के भाव जाग्रत होते हैं । 'भ. यशोधर द्वारा अपनी कृतियों में शब्दों का चयन भी पूर्ण विद्वत्ता के साथ किया है । कवि ने नेमिनाथ गति में पान बीड़ी का उल्लेख किया है । विवाह में पानों का बीड़ा देकर बरातिमों का स्वागत करने की प्रथा है जो १५वीं शताब्दि में भी यथावत थी। इसी तरह 'सू' शब्द के लिये 'लय' का प्रयोग किया है । लय शब्द देठ राजस्थानी भाषा का शब्द है ।
भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इन पांचों ही कवियों की रचनायें महत्वपूर्ण हैं । जन कवि अपनी रचनायें सरल बोलचाल की भाषा में निबद्ध करते रहे हैं। पद्यपि बे काव्य गत लक्षपों के प्राधार पर रचतायें निबद्ध करने में विश्वास नहीं रखते थे लेमिन फिर भी उनकी वृतियों राजस्थानी हिन्दी की प्रमूख्य कृतियां है
- - . .--.१. वोउ चंदन रुडों फूलडा रे पान बीबीष प्रमूल सा. ५०/पृष्ठ संख्या २०१. २. उहालि लू उही वाय, तपन ताप तनु साझ न जाय ॥ १७३/ 1, १६१.