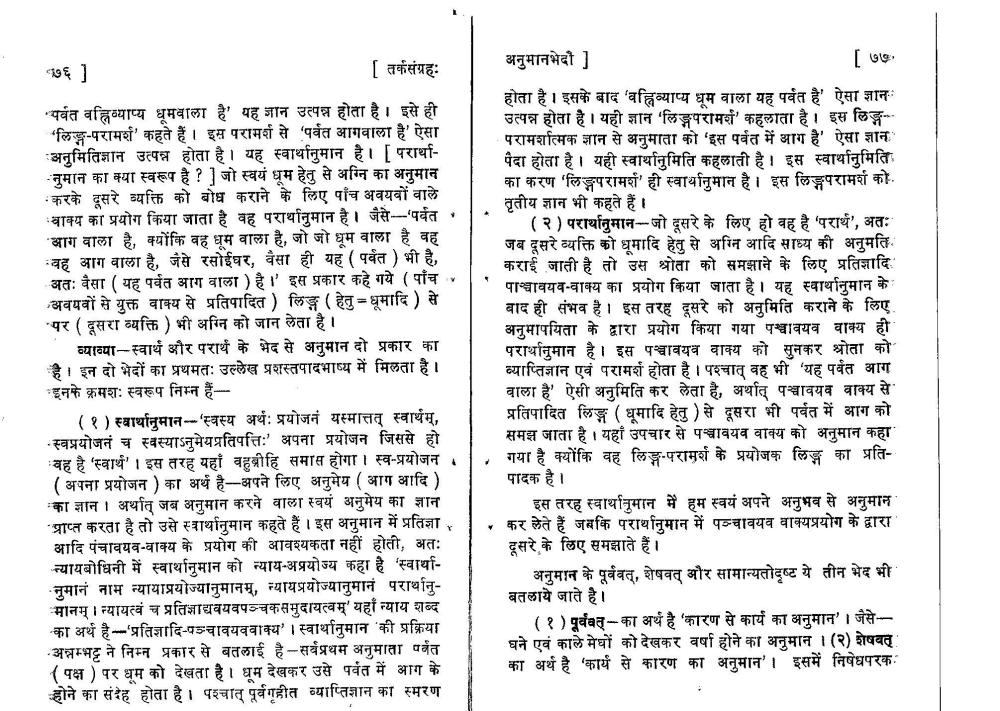________________ [ तर्कसंग्रहः अनुमानभेदी ] [77. "पर्वत वह्निव्याप्य धूमवाला है' यह जान उत्पन्न होता है। इसे ही 'लिङ्ग-परामर्श' कहते हैं। इस परामर्श से 'पर्वत आगवाला है' ऐसा अनुमितिज्ञान उत्पन्न होता है। यह स्वार्थानुमान है। [परार्था-नुमान का क्या स्वरूप है?] जो स्वयं धूम हेतु से अग्नि का अनुमान करके दूसरे व्यक्ति को बोध कराने के लिए पांच अवयवों वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह परार्थानुमान है। जैसे-'पर्वत / / 'आग वाला है, क्योंकि वह धूम वाला है, जो जो धूम वाला है वह / वह आग वाला है, जैसे रसोईघर, वैसा ही यह (पर्वत) भी है, अतः वैसा ( यह पर्वत आग वाला) है।' इस प्रकार कहे गये (पाँच / अवयवों से युक्त वाक्य से प्रतिपादित) लिङ्ग ( हेतु = धूमादि) से पर (दूसरा व्यक्ति) भी अग्नि को जान लेता है। व्याव्या-स्वार्थ और परार्थ के भेद से अनुमान दो प्रकार का है। इन दो भेदों का प्रथमत: उल्लेख प्रशस्तपादभाष्य में मिलता है। इनफे क्रमशः स्वरूप निम्न हैं (1) स्वार्थानुमान- 'स्वस्य अर्थः प्रयोजनं यस्मात्तत् स्वार्थम्, स्वप्रयोजनं च स्वस्याऽनुमेयप्रतिपत्तिः' अपना प्रयोजन जिससे हो वह है 'स्वार्थ' / इस तरह यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। स्व-प्रयोजन / (अपना प्रयोजन ) का अर्थ है-अपने लिए अनुमेय ( आग आदि) / का ज्ञान / अर्थात् जब अनुमान करने वाला स्वयं अनुमेय का ज्ञान "प्राप्त करता है तो उसे स्वार्थानुमान कहते हैं / इस अनुमान में प्रतिज्ञा आदि पंचावयव-वाक्य के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, अतः न्यायबोधिनी में स्वार्थानुमान को न्याय-अप्रयोज्य कहा है 'स्वार्था-नुमानं नाम न्यायाप्रयोज्यानुमानम्, न्यायप्रयोज्यानूमानं परार्थानमानम् / न्यायत्वं च प्रतिज्ञाद्यवयवपञ्चकसमुदायत्वम्' यहाँ न्याय शब्द का अर्थ है-'प्रतिज्ञादि-पञ्चावयववाक्य' / स्वार्थानुमान की प्रक्रिया अन्नम्भट्ट ने निम्न प्रकार से बतलाई है-सर्वप्रथम अनुमाता पर्चत (पक्ष) पर धम को देखता है। धम देखकर उसे पर्वत में आग के होने का संदेह होता है। पश्चात् पूर्व गृहीत व्याप्तिज्ञान का स्मरण होता है / इसके बाद 'वह्निव्याप्य धूम वाला यह पर्वत है' ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है / यही ज्ञान 'लिङ्गपरामर्श' कहलाता है। इस लिङ्गपरामर्शात्मक ज्ञान से अनुमाता को 'इस पर्वत में आग है' ऐसा ज्ञान पैदा होता है। यही स्वार्थानुमिति कहलाती है। इस स्वार्थानुमिति का करण 'लिङ्गपरामर्श' ही स्वार्थानुमान है। इस लिङ्गपरामर्श को. तृतीय ज्ञान भी कहते हैं। (2) परार्थानुमान-जो दूसरे के लिए हो वह है 'परार्थ', अतः जब दूसरे व्यक्ति को धूमादि हेतु से अग्नि आदि साध्य की अनुमति कराई जाती है तो उस श्रोता को समझाने के लिए प्रतिज्ञादि पाञ्चावयव-वाक्य का प्रयोग किया जाता है। यह स्वार्थानुमान के बाद ही संभव है। इस तरह दूसरे को अनुमिति कराने के लिए. अनुमापयिता के द्वारा प्रयोग किया गया पश्चावयव वाक्य ही परार्थानुमान है। इस पञ्चावयव वाक्य को सुनकर श्रोता को व्याप्तिज्ञान एवं परामर्श होता है। पश्चात् वह भी 'यह पर्वत आग वाला है' ऐसी अनुमिति कर लेता है, अर्थात् पञ्चावयव वाक्य से प्रतिपादित लिङ्ग (धूमादि हेतु) से दूसरा भी पर्वत में आग को समझ जाता है। यहाँ उपचार से पञ्चावयव वाक्य को अनुमान कहा गया है क्योंकि वह लिङ्ग-परामर्श के प्रयोजक लिङ्ग का प्रतिपादक है। इस तरह स्वार्थानुमान में हम स्वयं अपने अनुभव से अनुमान कर लेते हैं जबकि परार्थानुमान में पञ्चावयव वाक्यप्रयोग के द्वारा दूसरे के लिए समझाते हैं। अनुमान के पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यतोदष्ट ये तीन भेद भी बतलाये जाते है। (1) पूर्ववत्-का अर्थ है 'कारण से कार्य का अनुमान' / जैसेघने एवं काले मेघों को देखकर वर्षा होने का अनुमान / (2) शेषवत्' का अर्थ है 'कार्य से कारण का अनुमान'। इसमें निषेधपरकः