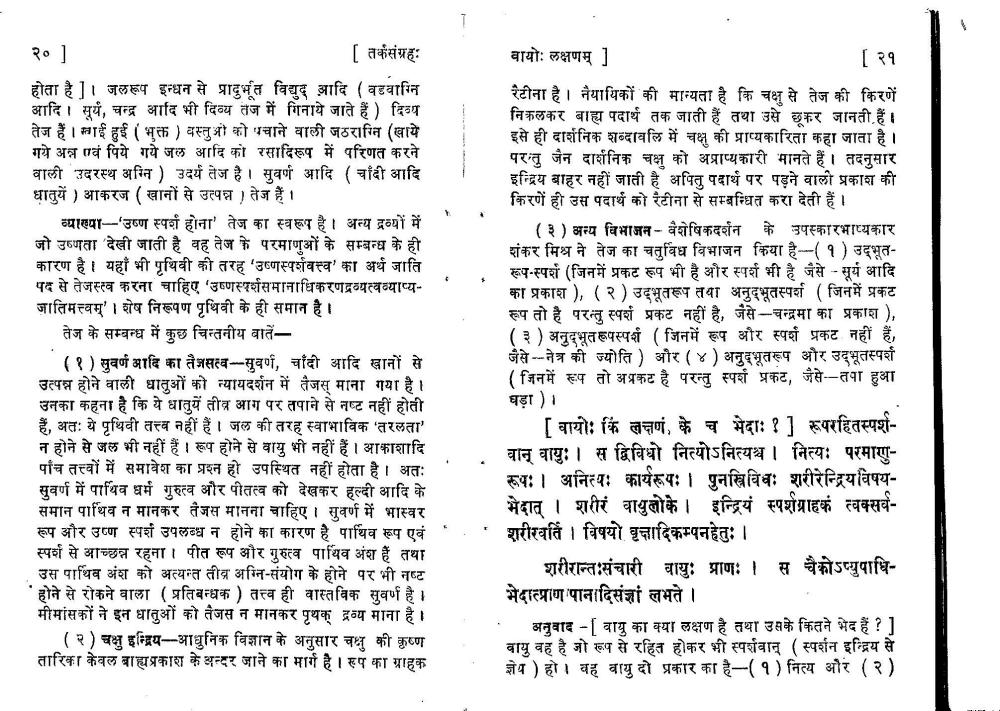________________ 20 ] [ तर्कसंग्रहः होता है ] / जलरूप इन्धन से प्रादुर्भूत विद्युद् आदि ( वडवाग्नि आदि। सूर्य, चन्द्र आदि भी दिव्य तज में गिनाये जाते हैं ) दिव्य तेज हैं / माई हुई ( भुक्त ) वस्तुओ को पचाने वाली जठराग्नि (खाये गये अन्न एवं पिये गये जल आदि को रसादिरूप में परिणत करने वाली उदरस्थ अग्नि) उदर्य तेज है। सुवर्ण आदि (चाँदी आदि धातुयें ) आकरज (खानों से उत्पन्न ) तेज हैं। व्याख्या-'उष्ण स्पर्श होना' तेज का स्वरूप है। अन्य द्रव्यों में जो उष्णता देखी जाती है वह तेज के परमाणुओं के सम्बन्ध के ही कारण है। यहाँ भी पृथिवी की तरह 'उष्णस्पर्शवत्व' का अर्थ जाति पद से तेजस्त्व करना चाहिए 'उष्णस्पर्शसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वम् / शेष निरूपण पृथिवी के ही समान है। तेज के सम्बन्ध में कुछ चिन्तनीय बातें (1) सुवर्ण आदि का तैजसत्व-सुवर्ण, चाँदी आदि खानों से उत्पन्न होने वाली धातुओं को न्यायदर्शन में तैजस माना गया है। उनका कहना है कि ये धातुयें तीव आग पर तपाने से नष्ट नहीं होती हैं, अतः ये पृथिवी तत्त्व नहीं हैं। जल की तरह स्वाभाविक 'तरलता' न होने से जल भी नहीं हैं / रूप होने से वायु भी नहीं हैं / आकाशादि पाँच तत्त्वों में समावेश का प्रश्न हो उपस्थित नहीं होता है। अतः सुवर्ण में पार्थिव धर्म गुरुत्व और पीतत्व को देखकर हल्दी आदि के समान पार्थिव न मानकर तैजस मानना चाहिए। सुवर्ण में भास्वर रूप और उष्ण स्पर्श उपलब्ध न होने का कारण है पार्थिव रूप एवं ' स्पर्श से आच्छन्न रहना। पीत रूप और गुरुत्व पार्थिव अंश हैं तथा उस पार्थिव अंश को अत्यन्त तीव्र अग्नि-संयोग के होने पर भी नष्ट होने से रोकने वाला (प्रतिबन्धक ) तत्त्व ही वास्तविक सुवर्ण है। मीमांसकों ने इन धातुओं को तेजस न मानकर पृथक् द्रव्य माना है। (2) चक्षु इन्द्रिय-आधुनिक विज्ञान के अनुसार चक्षु की कृष्ण तारिका केवल बाह्यप्रकाश के अन्दर जाने का मार्ग है / रूप का ग्राहक वायोः लक्षणम् ] [21 रैटीना है। नैयायिकों की मान्यता है कि चक्षु से तेज की किरणें निकलकर बाह्य पदार्थ तक जाती हैं तथा उसे छूकर जानती हैं / इसे ही दार्शनिक शब्दावलि में चक्षु की प्राप्यकारिता कहा जाता है / परन्तु जैन दार्शनिक चक्ष को अप्राप्यकारी मानते हैं। तदनुसार इन्द्रिय बाहर नहीं जाती है अपितु पदार्थ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें ही उस पदार्थ को रैटीना से सम्बन्धित करा देती हैं। (3) अन्य विभाजन- वैशेषिकदर्शन के उपस्कारभाष्यकार शंकर मिश्र ने तेज का चतुर्विध विभाजन किया है-(१) उद्भूतरूप-स्पर्श (जिनमें प्रकट रूप भी है और स्पर्श भी है जैसे - सूर्य आदि का प्रकाश ), (2) उद्भूतरूप तथा अनुभूतस्पर्श ( जिनमें प्रकट रूप तो है परन्तु स्पर्श प्रकट नहीं है, जैसे-चन्द्रमा का प्रकाश ), (3) अनुभूतरूपस्पर्श (जिनमें रूप और स्पर्श प्रकट नहीं हैं, जैसे--नेत्र की ज्योति ) और ( 4 ) अनुभूतरूप और उद्भूतस्पर्श (जिनमें रूप तो अप्रकट है परन्तु स्पर्श प्रकट, जैसे-तपा हुआ घड़ा)। [वायोः किं लक्षणं, के च भेदाः ? 1 रूपरहितस्पर्शवान् वायुः। स द्विविधो नित्योऽनित्यश्च / नित्यः परमाणुरूपः। अनित्यः कार्यरूपः। पुनत्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् / शरीरं वायुलोके। इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक्सर्व' शरीरवर्ति / विषयो वृक्षादिकम्पनहेतुः। शरीरान्तःसंचारी वायुः प्राणः / स चैकोऽप्युपाधिभेदात्प्राण पानादिसंज्ञां लभते / - अनुवाद -[ वायु का क्या लक्षण है तथा उसके कितने भेद हैं ? ] वायु वह है जो रूप से रहित होकर भी स्पर्शवान् (स्पर्शन इन्द्रिय से ज्ञेय ) हो। वह वायु दो प्रकार का है-(१) नित्य और (2)