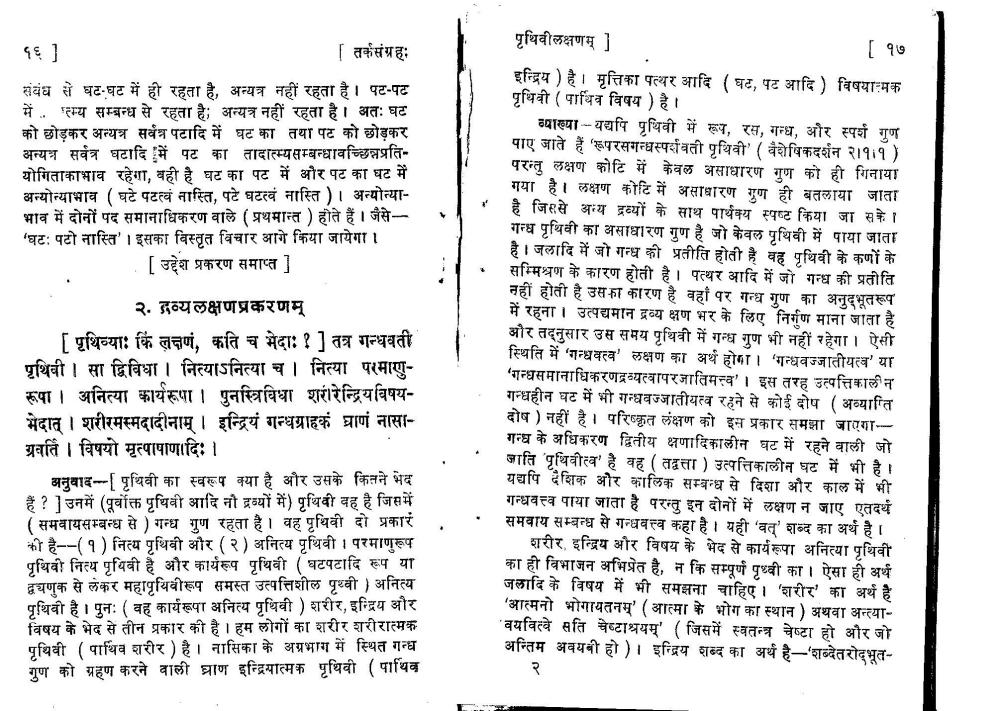________________ पृथिवीलक्षणम् ] 16] [ तर्कसंग्रहः [ 17 संबंध से घट-घट में ही रहता है, अन्यत्र नहीं रहता है। पट-पट में .. त्म्य सम्बन्ध से रहता है। अन्यत्र नहीं रहता है। अतः घट को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र पटादि में घट का तथा पट को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र घटादि में पट का तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभाव रहेगा, वही है घट का पट में और पट का घट में अन्योन्याभाव (घटे पटत्वं नास्ति, पटे घटत्वं नास्ति)। अन्योन्याभाव में दोनों पद समानाधिकरण वाले (प्रथमान्त) होते हैं / जैसे'घटः पटो नास्ति' / इसका विस्तृत विचार आगे किया जायेगा। [ उद्देश प्रकरण समाप्त] 2. द्रव्यलक्षणप्रकरणम् [पृथिव्याः किं लक्षणं, कति च भेदाः 1] तत्र गन्धवती पृथिवी। सा द्विविधा / नित्यानित्या च / नित्या परमाणुरूपा / अनित्या कार्यरूपा / पुनस्त्रिविधा शरारेन्द्रियविषयभेदात् / शरीरमस्मदादीनाम् / इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ति / विषयो मृत्पाषाणादिः / ___अनुवाद-[पृथिवी का स्वरूप क्या है और उसके कितने भेद हैं ? ] उनमें (पूर्वोक्त पृथिवी आदि नौ द्रव्यों में) पृथिवी वह है जिसमें (समवायसम्बन्ध से ) गन्ध गुण रहता है। वह पृथिवी दो प्रकार की है--(१) नित्य पृथिवी और (2) अनित्य पृथिवी / परमाणुरूप पृथिवी नित्य पृथिवी है और कार्यरूप पृथिवी (घटपटादि रूप या द्वघणुक से लेकर महापृयिवीरूप समस्त उत्पत्तिशील पृथ्वी ) अनित्य पृथिवी है। पुनः ( वह कार्यरूपा अनित्य पृथिवी) शरीर, इन्द्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार की है। हम लोगों का शरीर शरीरात्मक पृथिवी (पार्थिव शरीर ) है। नासिका के अग्रभाग में स्थित गन्ध गुण को ग्रहण करने वाली घ्राण इन्द्रियात्मक पृथिवी (पार्थिव इन्द्रिय) है। मृत्तिका पत्थर आदि (घट, पट आदि) विषयामक पृथिवी (पार्थिव विषय ) है। व्याख्या-यद्यपि पृथिवी में रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श गुण पाए जाते हैं 'रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी' (वैशेषिकदर्शन 2011) परन्तु लक्षण कोटि में केवल असाधारण गुण को ही गिनाया गया है। लक्षण कोटि में असाधारण गुण ही बतलाया जाता है जिससे अन्य द्रव्यों के साथ पार्थक्य स्पष्ट किया जा सके। गन्ध पृथिवी का असाधारण गुण है जो केवल प्रथिवी में पाया जाता है। जलादि में जो गन्ध की प्रतीति होती है वह प्रथिवी के कणों के सम्मिश्रण के कारण होती है। पत्थर आदि में जो गन्ध की प्रतीति नहीं होती है उसका कारण है वहाँ पर गन्ध गण का अनुभूतरूप में रहना। उत्पद्यमान द्रव्य क्षण भर के लिए निर्गण माना जाता है और तद्नुसार उस समय पृथिवी में गन्ध गुण भी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में 'गन्धवत्व' लक्षण का अर्थ होगा। 'गन्धवज्जातीयत्व' या 'गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वापरजातिमत्व'। इस तरह उत्पत्तिकालीन गन्धहीन घट में भी गन्धवज्जातीयत्व रहने से कोई दोष ( अव्याप्ति दोष) नहीं है। परिष्कृत लक्षण को इस प्रकार समझा जाएगागन्ध के अधिकरण द्वितीय क्षणादिकालीन घट में रहने वाली जो जाति 'पृथिवीत्व' है वह ( तद्वत्ता) उत्पत्तिकालीन घट में भी है। यद्यपि दैशिक और कालिक सम्बन्ध से दिशा और काल में भी गन्धवत्व पाया जाता है परन्तु इन दोनों में लक्षण न जाए एतदर्थ समवाय सम्बन्ध से गन्धवत्त्व कहा है। यही 'वत' शब्द का अर्थ है। शरीर, इन्द्रिय और विषय के भेद से कार्यरूपा अनित्या पृथिवी का ही विभाजन अभिप्रेत है, न कि सम्पूर्ण पृथ्वी का। ऐसा ही अर्थ जलादि के विषय में भी समझना चाहिए / 'शरीर' का अर्थ है 'आत्मनो भोगायतनम्' (आत्मा के भोग का स्थान) अथवा अन्त्या'वयवित्वे सति चेष्टाश्रयम्' (जिसमें स्वतन्त्र चेष्टा हो और जो अन्तिम अवयवी हो)। इन्द्रिय शब्द का अर्थ है-'शब्देतरोद्भूत