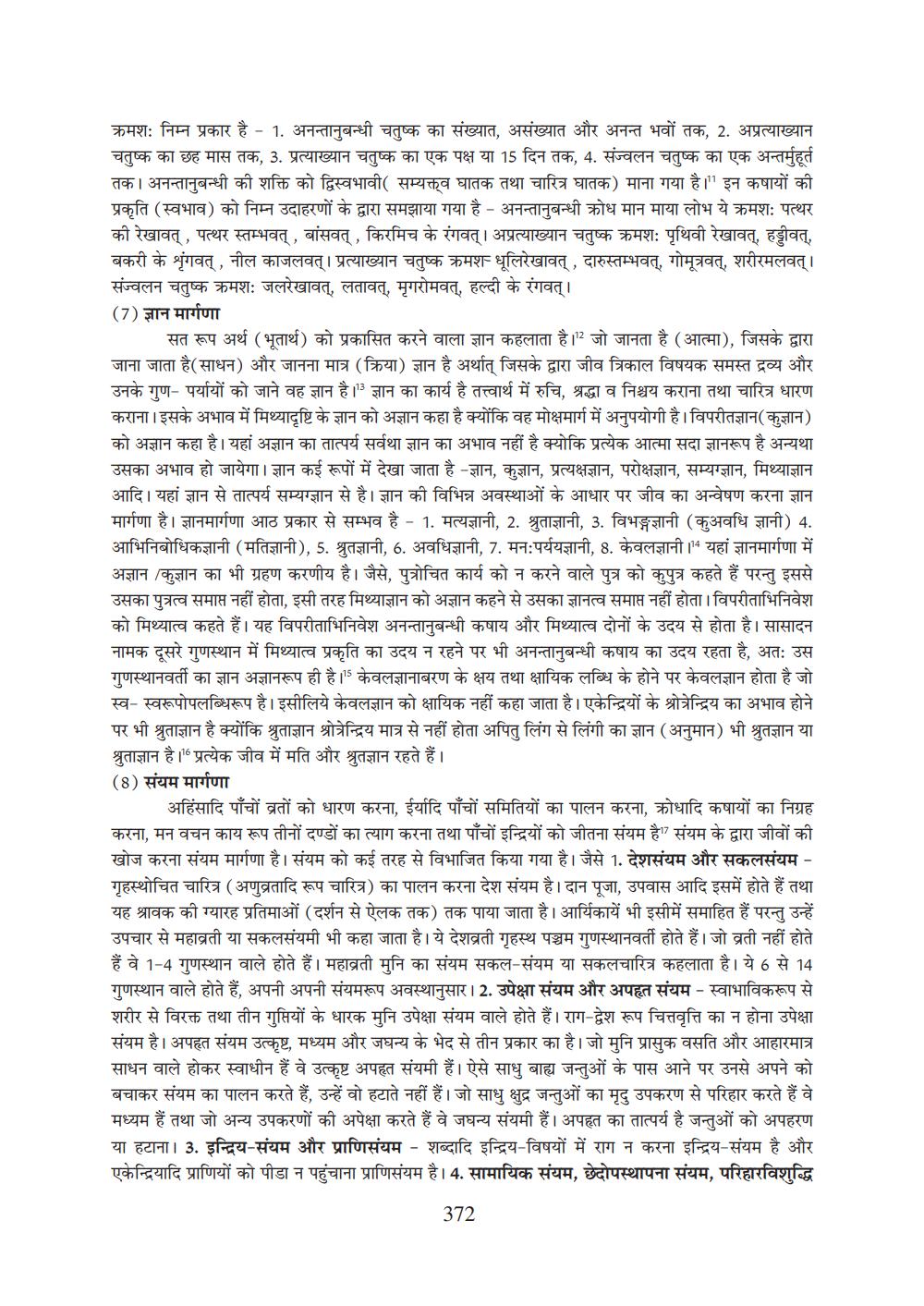________________ क्रमश: निम्न प्रकार है - 1. अनन्तानुबन्धी चतुष्क का संख्यात, असंख्यात और अनन्त भवों तक, 2. अप्रत्याख्यान चतुष्क का छह मास तक, 3. प्रत्याख्यान चतुष्क का एक पक्ष या 15 दिन तक, 4. संज्वलन चतुष्क का एक अन्तर्मुहूर्त तक। अनन्तानुबन्धी की शक्ति को द्विस्वभावी( सम्यक्त्व घातक तथा चारित्र घातक) माना गया है।" इन कषायों की प्रकृति (स्वभाव) को निम्न उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है - अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ ये क्रमश: पत्थर की रेखावत् , पत्थर स्तम्भवत् , बांसवत् , किरमिच के रंगवत्। अप्रत्याख्यान चतुष्क क्रमशः पृथिवी रेखावत्, हड्डीवत्, बकरी के शृंगवत् , नील काजलवत्। प्रत्याख्यान चतुष्क क्रमश-धूलिरेखावत् , दारुस्तम्भवत्, गोमूत्रवत्, शरीरमलवत्। संज्वलन चतुष्क क्रमशः जलरेखावत्, लतावत्, मृगरोमवत्, हल्दी के रंगवत् / (7) ज्ञान मार्गणा सत रूप अर्थ (भूतार्थ) को प्रकासित करने वाला ज्ञान कहलाता है। जो जानता है (आत्मा), जिसके द्वारा जाना जाता है(साधन) और जानना मात्र (क्रिया) ज्ञान है अर्थात् जिसके द्वारा जीव त्रिकाल विषयक समस्त द्रव्य और उनके गुण- पर्यायों को जाने वह ज्ञान है। ज्ञान का कार्य है तत्त्वार्थ में रुचि, श्रद्धा व निश्चय कराना तथा चारित्र धारण कराना। इसके अभाव में मिथ्यादृष्टि के ज्ञान को अज्ञान कहा है क्योंकि वह मोक्षमार्ग में अनुपयोगी है। विपरीतज्ञान(कुज्ञान) को अज्ञान कहा है। यहां अज्ञान का तात्पर्य सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं है क्योकि प्रत्येक आत्मा सदा ज्ञानरूप है अन्यथा उसका अभाव हो जायेगा। ज्ञान कई रूपों में देखा जाता है -ज्ञान, कुज्ञान, प्रत्यक्षज्ञान, परोक्षज्ञान, सम्यग्ज्ञान, मिथ्याज्ञान आदि। यहां ज्ञान से तात्पर्य सम्यग्ज्ञान से है। ज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर जीव का अन्वेषण करना ज्ञान मार्गणा है। ज्ञानमार्गणा आठ प्रकार से सम्भव है - 1. मत्यज्ञानी, 2. श्रुताज्ञानी, 3. विभङ्गज्ञानी (कुअवधि ज्ञानी) 4. आभिनिबोधिकज्ञानी (मतिज्ञानी), 5. श्रुतज्ञानी, 6. अवधिज्ञानी, 7. मन:पर्ययज्ञानी, 8. केवलज्ञानी। यहां ज्ञानमार्गणा में अज्ञान /कुज्ञान का भी ग्रहण करणीय है। जैसे, पुत्रोचित कार्य को न करने वाले पुत्र को कुपुत्र कहते हैं परन्तु इससे उसका पुत्रत्व समाप्त नहीं होता, इसी तरह मिथ्याज्ञान को अज्ञान कहने से उसका ज्ञानत्व समाप्त नहीं होता। विपरीताभिनिवेश को मिथ्यात्व कहते हैं। यह विपरीताभिनिवेश अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व दोनों के उदय से होता है। सासादन नामक दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का उदय न रहने पर भी अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय रहता है, अत: उस गुणस्थानवर्ती का ज्ञान अज्ञानरूप ही है। केवलज्ञानाबरण के क्षय तथा क्षायिक लब्धि के होने पर केवलज्ञान होता है जो स्व-स्वरूपोपलब्धिरूप है। इसीलिये केवलज्ञान को क्षायिक नहीं कहा जाता है। एकेन्द्रियों के श्रोत्रेन्द्रिय का अभाव होने पर भी श्रुताज्ञान है क्योंकि श्रुताज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय मात्र से नहीं होता अपितु लिंग से लिंगी का ज्ञान (अनुमान) भी श्रुतज्ञान या श्रुताज्ञान है। प्रत्येक जीव में मति और श्रुतज्ञान रहते हैं। (8) संयम मार्गणा अहिंसादि पाँचों व्रतों को धारण करना, ईर्यादि पाँचों समितियों का पालन करना, क्रोधादि कषायों का निग्रह करना, मन वचन काय रूप तीनों दण्डों का त्याग करना तथा पाँचों इन्द्रियों को जीतना संयम है। संयम के द्वारा जीवों की खोज करना संयम मार्गणा है। संयम को कई तरह से विभाजित किया गया है। जैसे 1. देशसंयम और सकलसंयम - गृहस्थोचित चारित्र (अणुव्रतादि रूप चारित्र) का पालन करना देश संयम है। दान पूजा, उपवास आदि इसमें होते हैं तथा यह श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं (दर्शन से ऐलक तक) तक पाया जाता है। आर्यिकायें भी इसीमें समाहित हैं परन्तु उन्हें उपचार से महाव्रती या सकलसंयमी भी कहा जाता है। ये देशव्रती गृहस्थ पञ्चम गुणस्थानवर्ती होते हैं। जो व्रती नहीं होते हैं वे 1-4 गुणस्थान वाले होते हैं। महाव्रती मुनि का संयम सकल-संयम या सकलचारित्र कहलाता है। ये 6 से 14 गुणस्थान वाले होते हैं, अपनी अपनी संयमरूप अवस्थानुसार। 2. उपेक्षा संयम और अपहृत संयम - स्वाभाविकरूप से शरीर से विरक्त तथा तीन गुप्तियों के धारक मुनि उपेक्षा संयम वाले होते हैं। राग-द्वेश रूप चित्तवृत्ति का न होना उपेक्षा संयम है। अपहत संयम उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से तीन प्रकार का है। जो मुनि प्रासुक वसति और आहारमात्र साधन वाले होकर स्वाधीन हैं वे उत्कृष्ट अपहृत संयमी हैं। ऐसे साधु बाह्य जन्तुओं के पास आने पर उनसे अपने को बचाकर संयम का पालन करते हैं, उन्हें वो हटाते नहीं हैं। जो साधु क्षुद्र जन्तुओं का मृदु उपकरण से परिहार करते हैं वे मध्यम हैं तथा जो अन्य उपकरणों की अपेक्षा करते हैं वे जघन्य संयमी हैं। अपहृत का तात्पर्य है जन्तुओं को अपहरण या हटाना। 3. इन्द्रिय-संयम और प्राणिसंयम - शब्दादि इन्द्रिय-विषयों में राग न करना इन्द्रिय-संयम है और एकेन्द्रियादि प्राणियों को पीडा न पहुंचाना प्राणिसंयम है। 4. सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहारविशुद्धि 372