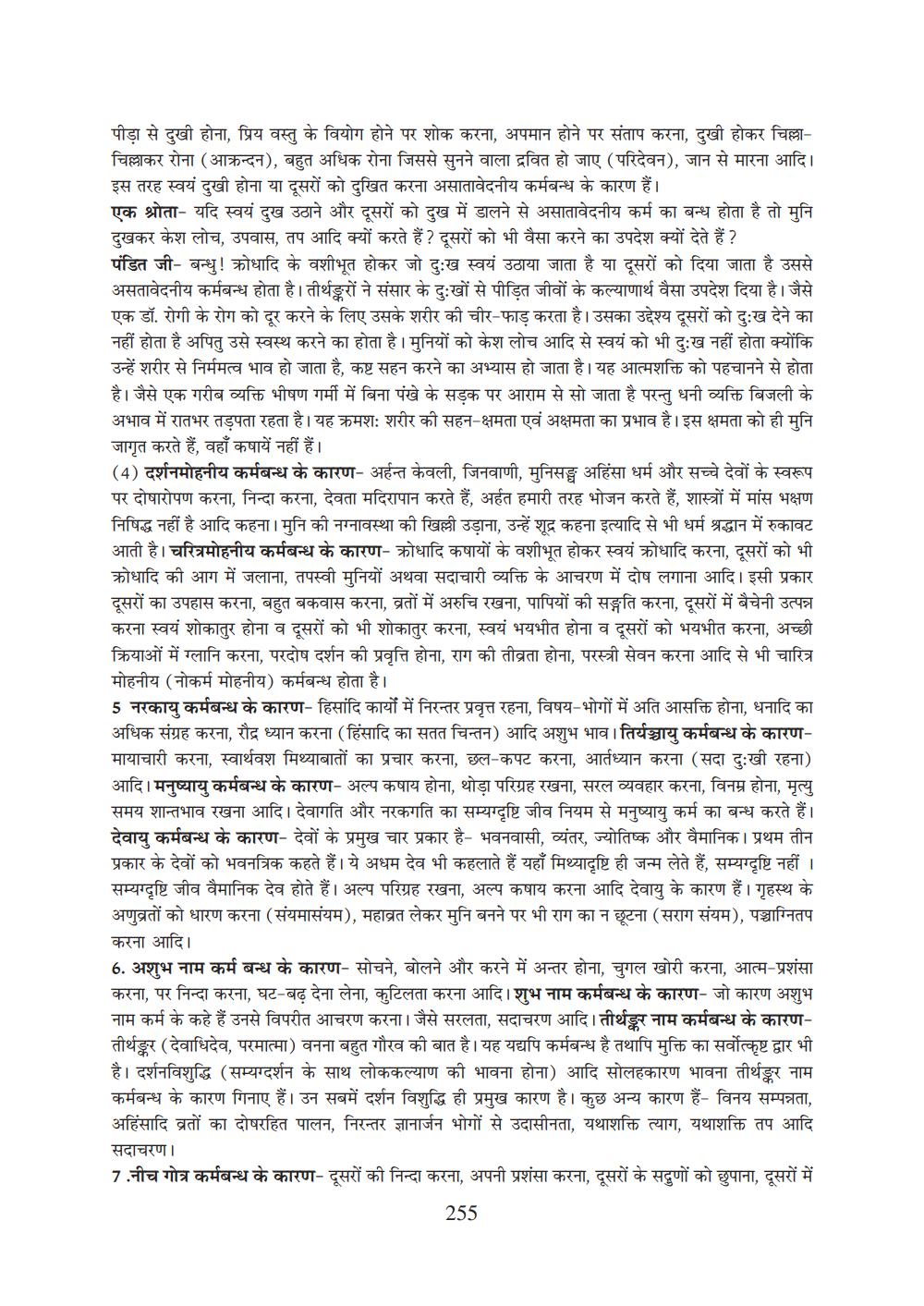________________ पीड़ा से दुखी होना, प्रिय वस्तु के वियोग होने पर शोक करना, अपमान होने पर संताप करना, दुखी होकर चिल्लाचिल्लाकर रोना (आक्रन्दन), बहुत अधिक रोना जिससे सुनने वाला द्रवित हो जाए (परिदेवन), जान से मारना आदि। इस तरह स्वयं दुखी होना या दूसरों को दुखित करना असातावेदनीय कर्मबन्ध के कारण हैं। एक श्रोता- यदि स्वयं दुख उठाने और दूसरों को दुख में डालने से असातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है तो मुनि दुखकर केश लोच, उपवास, तप आदि क्यों करते हैं? दूसरों को भी वैसा करने का उपदेश क्यों देते हैं? पंडित जी- बन्धु! क्रोधादि के वशीभूत होकर जो दुःख स्वयं उठाया जाता है या दूसरों को दिया जाता है उससे असतावेदनीय कर्मबन्ध होता है। तीर्थङ्करों ने संसार के दुःखों से पीड़ित जीवों के कल्याणार्थ वैसा उपदेश दिया है। जैसे एक डॉ. रोगी के रोग को दूर करने के लिए उसके शरीर की चीर-फाड़ करता है। उसका उद्देश्य दूसरों को दुःख देने का नहीं होता है अपितु उसे स्वस्थ करने का होता है। मुनियों को केश लोच आदि से स्वयं को भी दुःख नहीं होता क्योंकि उन्हें शरीर से निर्ममत्व भाव हो जाता है, कष्ट सहन करने का अभ्यास हो जाता है। यह आत्मशक्ति को पहचानने से होता है। जैसे एक गरीब व्यक्ति भीषण गर्मी में बिना पंखे के सड़क पर आराम से सो जाता है परन्तु धनी व्यक्ति बिजली के अभाव में रातभर तड़पता रहता है। यह क्रमश: शरीर की सहन-क्षमता एवं अक्षमता का प्रभाव है। इस क्षमता को ही मुनि जागृत करते हैं, वहाँ कषायें नहीं हैं। (4) दर्शनमोहनीय कर्मबन्ध के कारण- अर्हन्त केवली, जिनवाणी, मुनिसङ्घ अहिंसा धर्म और सच्चे देवों के स्वरूप पर दोषारोपण करना, निन्दा करना, देवता मदिरापान करते हैं, अर्हत हमारी तरह भोजन करते हैं, शास्त्रों में मांस भक्षण निषिद्ध नहीं है आदि कहना। मुनि की नग्नावस्था की खिल्ली उड़ाना, उन्हें शूद्र कहना इत्यादि से भी धर्म श्रद्धान में रुकावट आती है। चरित्रमोहनीय कर्मबन्ध के कारण- क्रोधादि कषायों के वशीभूत होकर स्वयं क्रोधादि करना, दूसरों को भी क्रोधादि की आग में जलाना, तपस्वी मुनियों अथवा सदाचारी व्यक्ति के आचरण में दोष लगाना आदि। इसी प्रकार दूसरों का उपहास करना, बहुत बकवास करना, व्रतों में अरुचि रखना, पापियों की सङ्गति करना, दूसरों में बैचेनी उत्पन्न करना स्वयं शोकातुर होना व दूसरों को भी शोकातुर करना, स्वयं भयभीत होना व दूसरों को भयभीत करना, अच्छी क्रियाओं में ग्लानि करना, परदोष दर्शन की प्रवृत्ति होना, राग की तीव्रता होना, परस्त्री सेवन करना आदि से भी चारित्र मोहनीय (नोकर्म मोहनीय) कर्मबन्ध होता है। 5 नरकायु कर्मबन्ध के कारण-हिसांदि कार्यों में निरन्तर प्रवृत्त रहना, विषय-भोगों में अति आसक्ति होना, धनादि का अधिक संग्रह करना, रौद्र ध्यान करना (हिंसादि का सतत चिन्तन) आदि अशुभ भाव। तिर्यञ्चायु कर्मबन्ध के कारणमायाचारी करना, स्वार्थवश मिथ्याबातों का प्रचार करना, छल-कपट करना, आर्तध्यान करना (सदा दुःखी रहना) आदि। मनुष्यायु कर्मबन्ध के कारण- अल्प कषाय होना, थोड़ा परिग्रह रखना, सरल व्यवहार करना, विनम्र होना, मृत्यु समय शान्तभाव रखना आदि। देवागति और नरकगति का सम्यग्दृष्टि जीव नियम से मनुष्यायु कर्म का बन्ध करते हैं। देवायु कर्मबन्ध के कारण- देवों के प्रमुख चार प्रकार है- भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। प्रथम तीन प्रकार के देवों को भवनत्रिक कहते हैं। ये अधम देव भी कहलाते हैं यहाँ मिथ्यादृष्टि ही जन्म लेते हैं, सम्यग्दृष्टि नहीं / सम्यग्दृष्टि जीव वैमानिक देव होते हैं। अल्प परिग्रह रखना, अल्प कषाय करना आदि देवायु के कारण हैं। गृहस्थ के अणुव्रतों को धारण करना (संयमासंयम), महाव्रत लेकर मुनि बनने पर भी राग का न छूटना (सराग संयम), पञ्चाग्नितप करना आदि। 6. अशुभ नाम कर्म बन्ध के कारण- सोचने, बोलने और करने में अन्तर होना, चुगल खोरी करना, आत्म-प्रशंसा करना, पर निन्दा करना, घट-बढ़ देना लेना, कुटिलता करना आदि। शुभ नाम कर्मबन्ध के कारण- जो कारण अशुभ नाम कर्म के कहे हैं उनसे विपरीत आचरण करना। जैसे सरलता, सदाचरण आदि। तीर्थङ्कर नाम कर्मबन्ध के कारणतीर्थङ्कर (देवाधिदेव, परमात्मा) वनना बहुत गौरव की बात है। यह यद्यपि कर्मबन्ध है तथापि मुक्ति का सर्वोत्कृष्ट द्वार भी है। दर्शनविशुद्धि (सम्यग्दर्शन के साथ लोककल्याण की भावना होना) आदि सोलहकारण भावना तीर्थङ्कर नाम कर्मबन्ध के कारण गिनाए हैं। उन सबमें दर्शन विशुद्धि ही प्रमुख कारण है। कुछ अन्य कारण हैं- विनय सम्पन्नता, अहिंसादि व्रतों का दोषरहित पालन, निरन्तर ज्ञानार्जन भोगों से उदासीनता, यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति तप आदि सदाचरण। 7.नीच गोत्र कर्मबन्ध के कारण- दूसरों की निन्दा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के सद्गुणों को छुपाना, दूसरों में 255 रणा