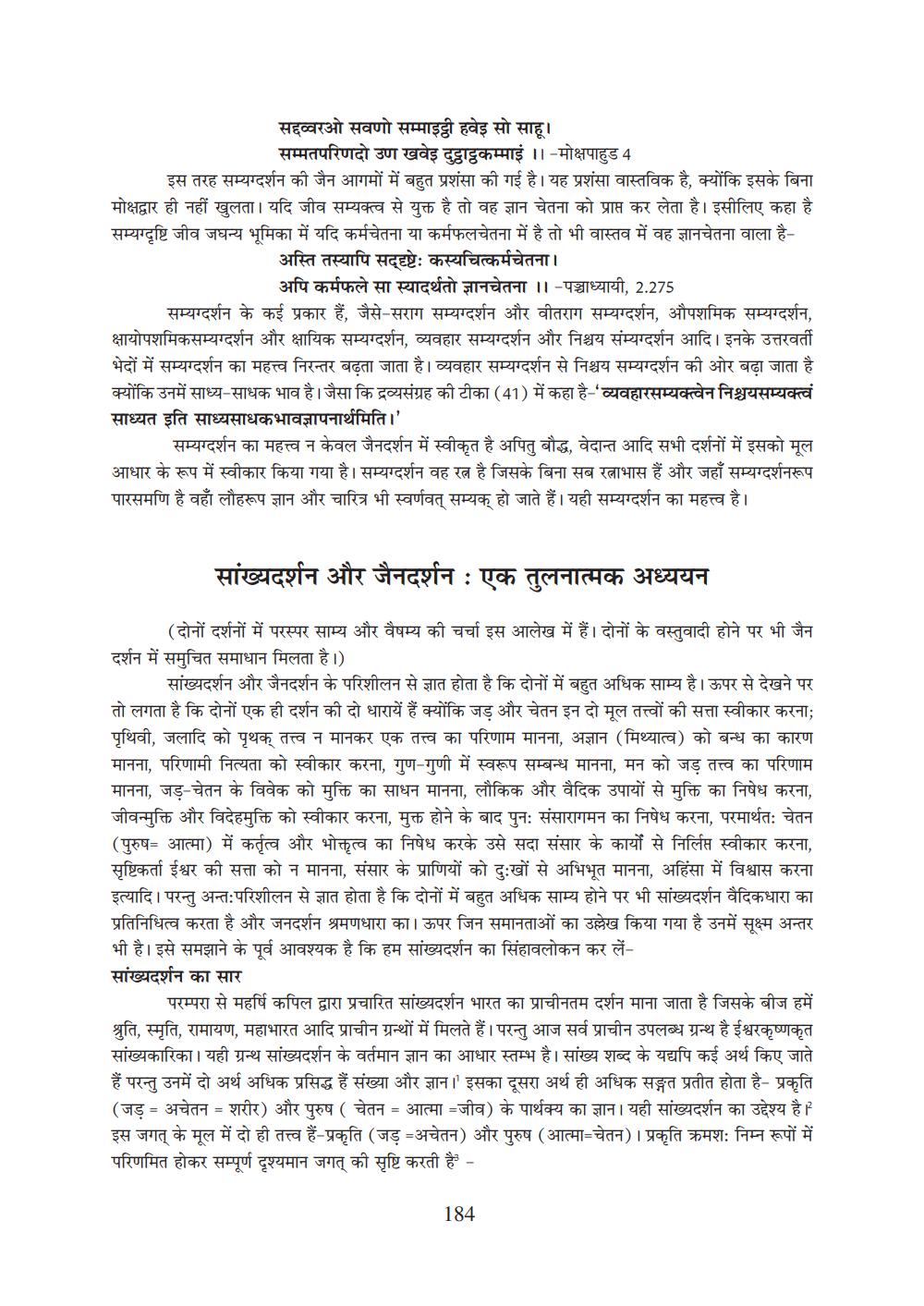________________ सद्दव्वरओ सवणो सम्माइट्ठी हवेइ सो साहू। सम्मतपरिणदो उण खवेइ दुवाट्टकम्माई / / -मोक्षपाहुड 4 इस तरह सम्यग्दर्शन की जैन आगमों में बहुत प्रशंसा की गई है। यह प्रशंसा वास्तविक है, क्योंकि इसके बिना मोक्षद्वार ही नहीं खुलता। यदि जीव सम्यक्त्व से युक्त है तो वह ज्ञान चेतना को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा है सम्यग्दृष्टि जीव जघन्य भूमिका में यदि कर्मचेतना या कर्मफलचेतना में है तो भी वास्तव में वह ज्ञानचेतना वाला है अस्ति तस्यापि सद्दृष्टेः कस्यचित्कर्मचेतना। अपि कर्मफले सा स्यादर्थतो ज्ञानचेतना / / -पञ्चाध्यायी, 2.275 सम्यग्दर्शन के कई प्रकार हैं, जैसे-सराग सम्यग्दर्शन और वीतराग सम्यग्दर्शन, औपशमिक सम्यग्दर्शन, क्षायोपशमिकसम्यग्दर्शन और क्षायिक सम्यग्दर्शन, व्यवहार सम्यग्दर्शन और निश्चय संम्यग्दर्शन आदि। इनके उत्तरवर्ती भेदों में सम्यग्दर्शन का महत्त्व निरन्तर बढ़ता जाता है। व्यवहार सम्यग्दर्शन से निश्चय सम्यग्दर्शन की ओर बढ़ा जाता है क्योंकि उनमें साध्य-साधक भाव है। जैसा कि द्रव्यसंग्रह की टीका (41) में कहा है-'व्यवहारसम्यक्त्वेन निश्चयसम्यक्त्वं साध्यत इति साध्यसाधकभावज्ञापनार्थमिति।' सम्यग्दर्शन का महत्त्व न केवल जैनदर्शन में स्वीकृत है अपितु बौद्ध, वेदान्त आदि सभी दर्शनों में इसको मूल आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। सम्यग्दर्शन वह रत्न है जिसके बिना सब रत्नाभास हैं और जहाँ सम्यग्दर्शनरूप पारसमणि है वहाँ लौहरूप ज्ञान और चारित्र भी स्वर्णवत् सम्यक् हो जाते हैं। यही सम्यग्दर्शन का महत्त्व है। सांख्यदर्शन और जैनदर्शन : एक तुलनात्मक अध्ययन (दोनों दर्शनों में परस्पर साम्य और वैषम्य की चर्चा इस आलेख में हैं। दोनों के वस्तुवादी होने पर भी जैन दर्शन में समुचित समाधान मिलता है।) सांख्यदर्शन और जैनदर्शन के परिशीलन से ज्ञात होता है कि दोनों में बहुत अधिक साम्य है। ऊपर से देखने पर तो लगता है कि दोनों एक ही दर्शन की दो धारायें हैं क्योंकि जड़ और चेतन इन दो मूल तत्त्वों की सत्ता स्वीकार करना; पृथिवी, जलादि को पृथक् तत्त्व न मानकर एक तत्त्व का परिणाम मानना, अज्ञान (मिथ्यात्व) को बन्ध का का मानना, परिणामी नित्यता को स्वीकार करना, गुण-गुणी में स्वरूप सम्बन्ध मानना, मन को जड़ तत्त्व का परिणाम मानना, जड़-चेतन के विवेक को मुक्ति का साधन मानना, लौकिक और वैदिक उपायों से मुक्ति का निषेध करना, जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति को स्वीकार करना, मुक्त होने के बाद पुनः संसारागमन का निषेध करना, परमार्थतः चेतन (पुरुष= आत्मा) में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का निषेध करके उसे सदा संसार के कार्यों से निर्लिप्त स्वीकार करना, सृष्टिकर्ता ईश्वर की सत्ता को न मानना, संसार के प्राणियों को दुःखों से अभिभूत मानना, अहिंसा में विश्वास करना इत्यादि। परन्तु अन्त:परिशीलन से ज्ञात होता है कि दोनों में बहुत अधिक साम्य होने पर भी सांख्यदर्शन वैदिकधारा का प्रतिनिधित्व करता है और जनदर्शन श्रमणधारा का। ऊपर जिन समानताओं का उल्लेख किया गया है उनमें सूक्ष्म अन्तर भी है। इसे समझाने के पूर्व आवश्यक है कि हम सांख्यदर्शन का सिंहावलोकन कर लेंसांख्यदर्शन का सार परम्परा से महर्षि कपिल द्वारा प्रचारित सांख्यदर्शन भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है जिसके बीज हमें श्रुति, स्मृति, रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में मिलते हैं। परन्तु आज सर्व प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ है ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिका। यही ग्रन्थ सांख्यदर्शन के वर्तमान ज्ञान का आधार स्तम्भ है। सांख्य शब्द के यद्यपि कई अर्थ किए जाते हैं परन्तु उनमें दो अर्थ अधिक प्रसिद्ध हैं संख्या और ज्ञान।' इसका दूसरा अर्थ ही अधिक सङ्गत प्रतीत होता है- प्रकृति (जड़ = अचेतन = शरीर) और पुरुष ( चेतन = आत्मा =जीव) के पार्थक्य का ज्ञान / यही सांख्यदर्शन का उद्देश्य है। इस जगत् के मूल में दो ही तत्त्व हैं-प्रकृति (जड़ =अचेतन) और पुरुष (आत्मा चेतन)। प्रकृति क्रमश: निम्न रूपों में परिणमित होकर सम्पूर्ण दृश्यमान जगत् की सृष्टि करती है - 184