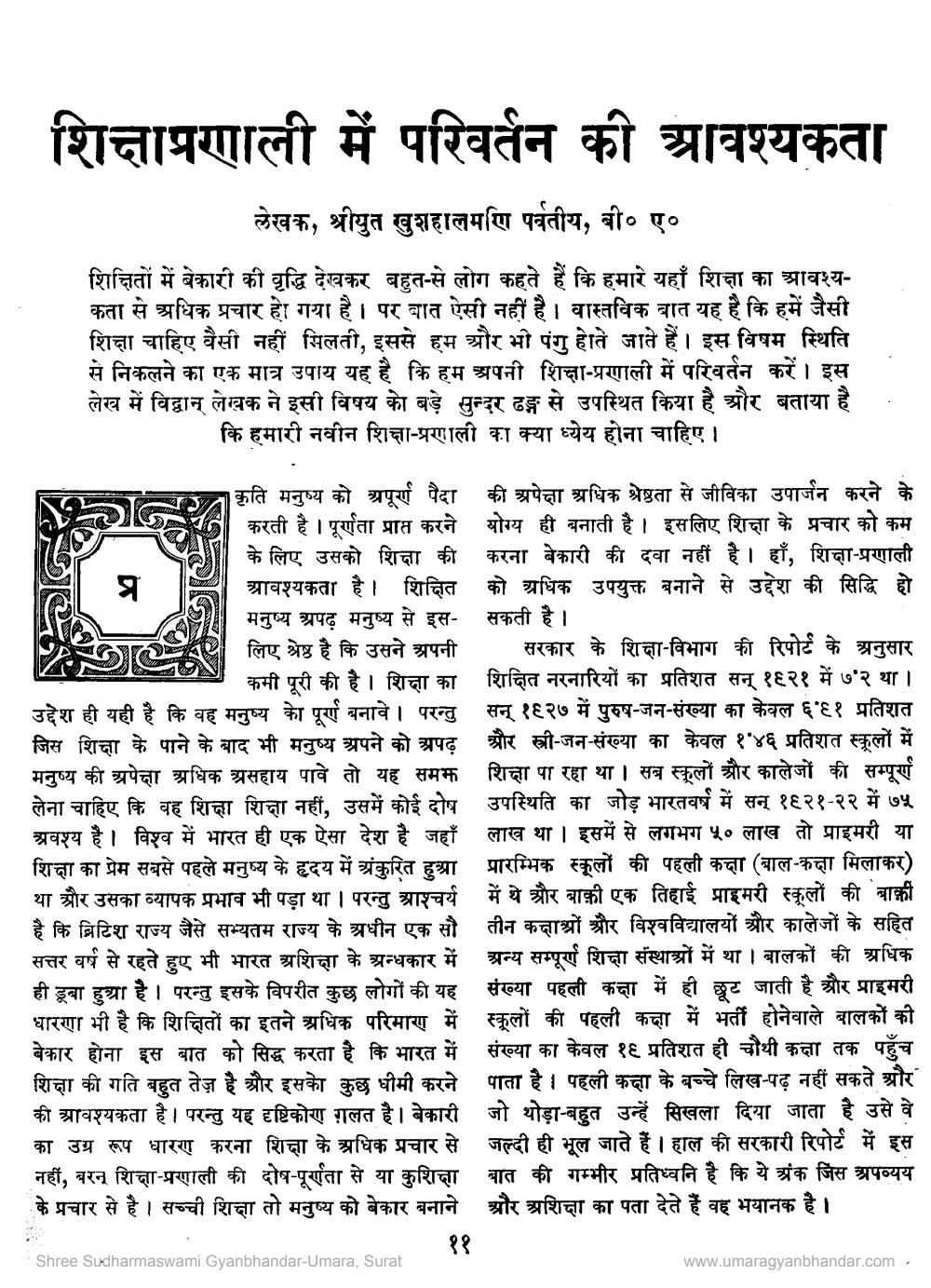________________
शिक्षाप्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता
लेखक, श्रीयुत खुशहालमणि पर्वतीय, बी० ए०
शिक्षितों में बेकारी की वृद्धि देखकर बहुत-से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का आवश्यकता से अधिक प्रचार हो गया है । पर बात ऐसी नहीं है। वास्तविक बात यह है कि हमें जैसी शिक्षा चाहिए वैसी नहीं मिलती, इससे हम और भी पंगु होते जाते हैं। इस विषम स्थिति से निकलने का एक मात्र उपाय यह है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करें। इस लेख में विद्वान् लेखक ने इसी विषय को बड़े सुन्दर ढङ्ग से उपस्थित किया है और बताया है। कि हमारी नवीन शिक्षा प्रणाली का क्या ध्येय होना चाहिए ।
प्र
कृति मनुष्य को पूर्ण पैदा करती है । पूर्णता प्राप्त करने के लिए उसको शिक्षा की आवश्यकता है । शिक्षित मनुष्य पढ़ मनुष्य से लिए श्रेष्ठ है कि उसने अपनी
इस
कमी पूरी की है । शिक्षा का उद्देश ही यही है कि वह मनुष्य को पूर्ण बनावे | परन्तु जिस शिक्षा के पाने के बाद भी मनुष्य अपने को पढ़ मनुष्य की अपेक्षा अधिक असहाय पावे तो यह समझ लेना चाहिए कि वह शिक्षा शिक्षा नहीं, उसमें कोई दोष अवश्य है । विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ शिक्षा का प्रेम सबसे पहले मनुष्य के हृदय में अंकुरित हुआ था और उसका व्यापक प्रभाव भी पड़ा था । परन्तु आश्चर्य है कि ब्रिटिश राज्य जैसे सभ्यतम राज्य के अधीन एक सौ सत्तर वर्ष से रहते हुए भी भारत शिक्षा के अन्धकार में
बा हुआ है । परन्तु इसके विपरीत कुछ लोगों की यह धारणा भी है कि शिक्षितों का इतने अधिक परिमाण में बेकार होना इस बात को सिद्ध करता है कि भारत में शिक्षा की गति बहुत तेज़ है और इसको कुछ धीमी करने की आवश्यकता है । परन्तु यह दृष्टिकोण ग़लत है । बेकारी का उग्र रूप धारण करना शिक्षा के अधिक प्रचार से नहीं, बरन् शिक्षा प्रणाली की दोष- पूर्णता से या कुशिक्षा के प्रचार से है। सच्ची शिक्षा तो मनुष्य को बेकार बनाने ११
Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat
की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठता से जीविका उपार्जन करने के योग्य ही बनाती है । इसलिए शिक्षा के प्रचार को कम करना बेकारी की दवा नहीं है। हाँ, शिक्षा-प्रणाली को अधिक उपयुक्त बनाने से उद्देश की सिद्धि हो सकती है ।
सरकार के शिक्षा-विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षित नरनारियों का प्रतिशत सन् १६२१ में ७२ था । सन् १९२७ में पुरुष - जन संख्या का केवल ६°६१ प्रतिशत और स्त्री- जन-संख्या का केवल १९४६ प्रतिशत स्कूलों में शिक्षा पा रहा था । सब स्कूलों और कालेजों की सम्पूर्ण उपस्थिति का जोड़ भारतवर्ष में सन् १६२१-२२ में ७५ लाख था । इसमें से लगभग ५० लाख तो प्राइमरी या प्रारम्भिक स्कूलों की पहली कक्षा (बाल - कक्षा मिलाकर ) में थे और बाक़ी एक तिहाई प्राइमरी स्कूलों की बाकी तीन कक्षाओं और विश्वविद्यालयों और कालेजों के सहित अन्य सम्पूर्ण शिक्षा संस्थानों में था । बालकों की अधिक संख्या पहली कक्षा में ही छूट जाती है और प्राइमरी स्कूलों की पहली कक्षा में भर्ती होनेवाले बालकों की संख्या का केवल १६ प्रतिशत ही चौथी कक्षा तक पहुँच पाता है । पहली कक्षा के बच्चे लिख-पढ़ नहीं सकते और जो थोड़ा-बहुत उन्हें सिखला दिया जाता है उसे वे जल्दी ही भूल जाते हैं । हाल की सरकारी रिपोर्ट में इस बात की गम्भीर प्रतिध्वनि है कि ये अंक जिस अपव्यय और अशिक्षा का पता देते हैं वह भयानक है ।
www.umaragyanbhandar.com -