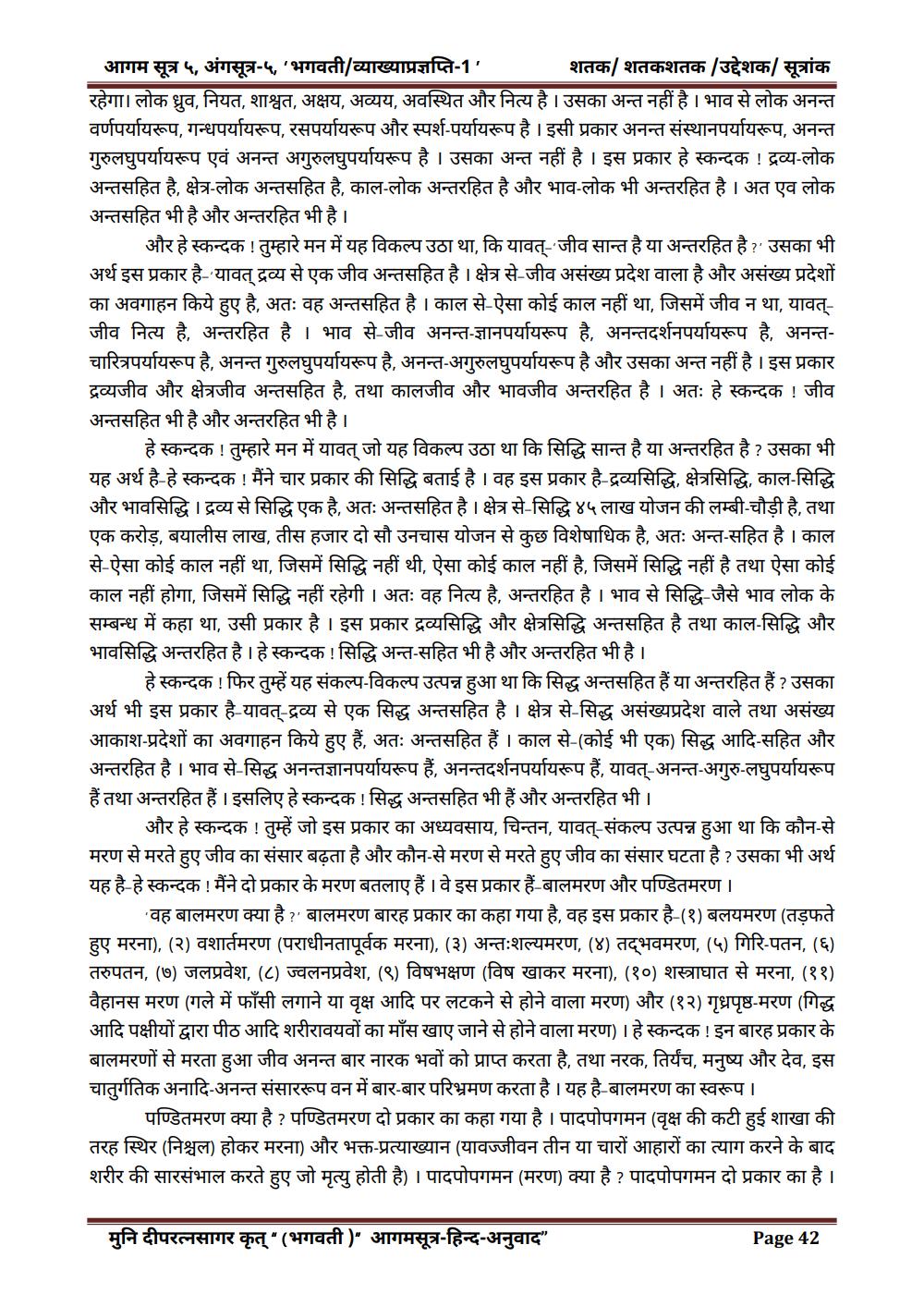________________
आगम सूत्र ५, अंगसूत्र-५, 'भगवती/व्याख्याप्रज्ञप्ति-1'
शतक/ शतकशतक/उद्देशक/ सूत्रांक रहेगा। लोक ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित और नित्य है। उसका अन्त नहीं है । भाव से लोक अनन्त वर्णपर्यायरूप, गन्धपर्यायरूप, रसपर्यायरूप और स्पर्श-पर्यायरूप है । इसी प्रकार अनन्त संस्थानपर्यायरूप, अनन्त गुरुलघुपर्यायरूप एवं अनन्त अगुरुलघुपर्यायरूप है । उसका अन्त नहीं है । इस प्रकार हे स्कन्दक ! द्रव्य-लोक अन्तसहित है, क्षेत्र-लोक अन्तसहित है, काल-लोक अन्तरहित है और भाव-लोक भी अन्तरहित है । अत एव लोक अन्तसहित भी है और अन्तरहित भी है।
और हे स्कन्दक! तुम्हारे मन में यह विकल्प उठा था, कि यावत्- जीव सान्त है या अन्तरहित है ?' उसका भी अर्थ इस प्रकार है- यावत् द्रव्य से एक जीव अन्तसहित है । क्षेत्र से-जीव असंख्य प्रदेश वाला है और असंख्य प्रदेशों का अवगाहन किये हुए है, अतः वह अन्तसहित है । काल से-ऐसा कोई काल नहीं था, जिसमें जीव न था, यावत्जीव नित्य है, अन्तरहित है । भाव से-जीव अनन्त-ज्ञानपर्यायरूप है, अनन्तदर्शनपर्यायरूप है, अनन्तचारित्रपर्यायरूप है, अनन्त गरुलांपर्यायरूप है, अनन्त-अगरुलघपर्यायरूप है और उसका अन्त नहीं द्रव्यजीव और क्षेत्रजीव अन्तसहित है, तथा कालजीव और भावजीव अन्तरहित है । अतः हे स्कन्दक ! जीव अन्तसहित भी है और अन्तरहित भी है।
हे स्कन्दक ! तुम्हारे मन में यावत् जो यह विकल्प उठा था कि सिद्धि सान्त है या अन्तरहित है ? उसका भी यह अर्थ है-हे स्कन्दक ! मैंने चार प्रकार की सिद्धि बताई है । वह इस प्रकार है-द्रव्यसिद्धि, क्षेत्रसिद्धि, काल-सिद्धि
और भावसिद्धि । द्रव्य से सिद्धि एक है, अतः अन्तसहित है। क्षेत्र से-सिद्धि ४५ लाख योजन की लम्बी-चौड़ी है, तथा एक करोड़, बयालीस लाख, तीस हजार दो सौ उनचास योजन से कुछ विशेषाधिक है, अतः अन्त-सहित है । काल से-ऐसा कोई काल नहीं था, जिसमें सिद्धि नहीं थी, ऐसा कोई काल नहीं है, जिसमें सिद्धि नहीं है तथा ऐसा कोई काल नहीं होगा, जिसमें सिद्धि नहीं रहेगी । अतः वह नित्य है, अन्तरहित है । भाव से सिद्धि-जैसे भाव लोक के सम्बन्ध में कहा था, उसी प्रकार है । इस प्रकार द्रव्यसिद्धि और क्षेत्रसिद्धि अन्तसहित है तथा काल-सिद्धि और भावसिद्धि अन्तरहित है । हे स्कन्दक! सिद्धि अन्त-सहित भी है और अन्तरहित भी है।
हे स्कन्दक ! फिर तुम्हें यह संकल्प-विकल्प उत्पन्न हुआ था कि सिद्ध अन्तसहित हैं या अन्तरहित हैं ? उसका अर्थ भी इस प्रकार है-यावत्-द्रव्य से एक सिद्ध अन्तसहित है । क्षेत्र से-सिद्ध असंख्यप्रदेश वाले तथा असंख्य आकाश-प्रदेशों का अवगाहन किये हुए हैं, अतः अन्तसहित हैं । काल से-(कोई भी एक) सिद्ध आदि-सहित और अन्तरहित है । भाव से सिद्ध अनन्तज्ञानपर्यायरूप हैं, अनन्तदर्शनपर्यायरूप हैं, यावत्-अनन्त-अगुरु-लघुपर्यायरूप हैं तथा अन्तरहित हैं । इसलिए हे स्कन्दक! सिद्ध अन्तसहित भी हैं और अन्तरहित भी।
और हे स्कन्दक ! तुम्हें जो इस प्रकार का अध्यवसाय, चिन्तन, यावत्-संकल्प उत्पन्न हुआ था कि कौन-से मरण से मरते हुए जीव का संसार बढ़ता है और कौन-से मरण से मरते हुए जीव का संसार घटता है ? उसका भी अर्थ यह है-हे स्कन्दक ! मैंने दो प्रकार के मरण बतलाए हैं । वे इस प्रकार हैं-बालमरण और पण्डितमरण ।
वह बालमरण क्या है ?' बालमरण बारह प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार है-(१) बलयमरण (तड़फते हुए मरना), (२) वशार्तमरण (पराधीनतापूर्वक मरना), (३) अन्तःशल्यमरण, (४) तद्भवमरण, (५) गिरि-पतन, (६) तरुपतन, (७) जलप्रवेश, (८) ज्वलनप्रवेश, (९) विषभक्षण (विष खाकर मरना), (१०) शस्त्राघात से मरना, (११) वैहानस मरण (गले में फाँसी लगाने या वृक्ष आदि पर लटकने से होने वाला मरण) और (१२) गृध्रपृष्ठ-मरण (गिद्ध आदि पक्षीयों द्वारा पीठ आदि शरीरावयवों का माँस खाए जाने से होने वाला मरण) । हे स्कन्दक! इन बारह प्रकार के बालमरणों से मरता हुआ जीव अनन्त बार नारक भवों को प्राप्त करता है, तथा नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इस चातुर्गतिक अनादि-अनन्त संसाररूप वन में बार-बार परिभ्रमण करता है । यह है-बालमरण का स्वरूप ।
___ पण्डितमरण क्या है ? पण्डितमरण दो प्रकार का कहा गया है । पादपोपगमन (वृक्ष की कटी हुई शाखा की तरह स्थिर (निश्चल) होकर मरना) और भक्त-प्रत्याख्यान (यावज्जीवन तीन या चारों आहारों का त्याग करने के बाद शरीर की सारसंभाल करते हुए जो मृत्यु होती है) । पादपोपगमन (मरण) क्या है ? पादपोपगमन दो प्रकार का है।
मुनि दीपरत्नसागर कृत् "(भगवती) आगमसूत्र-हिन्द-अनुवाद"
Page 42