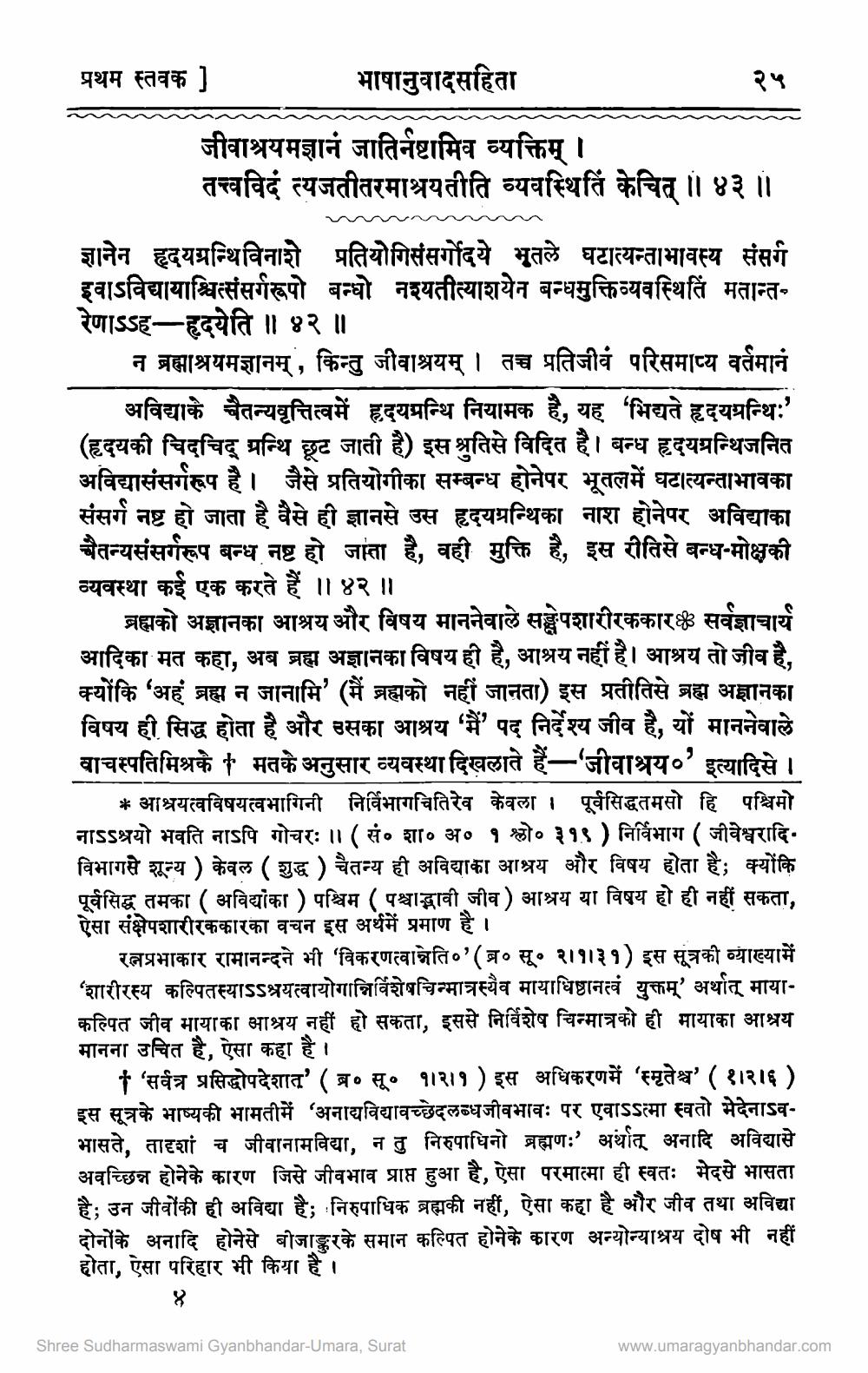________________
प्रथम स्तवक ]
भाषानुवादसहिता
२५
जीवाश्रयमज्ञानं जातिर्नष्टामिव व्यक्तिम् । तत्वविदं त्यजतीतरमाश्रयतीति व्यवस्थिति केचित् ॥ ४३ ॥
ज्ञानेन हृदयग्रन्थिविनाशे प्रतियोगिसंसर्गोदये भूतले घटात्यन्ताभावस्य संसर्ग इवाऽविद्यायाश्चित्संसर्गरूपो बन्धो नश्यतीत्याशयेन बन्धमुक्तिव्यवस्थिति मतान्त. रेणाऽऽह-हृदयेति ॥ ४२ ॥
न ब्रह्माश्रयमज्ञानम् , किन्तु जीवाश्रयम् । तच्च प्रतिजीवं परिसमाप्य वर्तमान
अविद्याके चैतन्यवृत्तित्वमें हृदयप्रन्थि नियामक है, यह 'भिद्यते हृदयग्रन्थिः ' (हृदयकी चिदचिद् ग्रन्थि छूट जाती है) इस श्रुतिसे विदित है। बन्ध हृदयग्रन्थिजनित अविद्यासंसर्गरूप है। जैसे प्रतियोगीका सम्बन्ध होनेपर भूतल में घटात्यन्ताभावका संसर्ग नष्ट हो जाता है वैसे ही ज्ञानसे उस हृदयग्रन्थिका नाश होनेपर अविद्याका चैतन्यसंसर्गरूप बन्ध नष्ट हो जाता है, वही मुक्ति है, इस रीतिसे बन्ध-मोक्षकी व्यवस्था कई एक करते हैं ॥४२॥
ब्रह्मको अज्ञानका आश्रय और विषय माननेवाले सङ्केपशारीरककार सर्वज्ञाचार्य आदिका मत कहा, अब ब्रह्म अज्ञानका विषय ही है, आश्रय नहीं है। आश्रय तो जीव है, क्योंकि 'अहं ब्रह्म न जानामि' (मैं ब्रह्मको नहीं जानता) इस प्रतीतिसे ब्रह्म अज्ञानका विषय ही सिद्ध होता है और उसका आश्रय 'मैं' पद निर्देश्य जीव है, यो माननेवाले वाचस्पतिमिश्रके + मतके अनुसार व्यवस्था दिखलाते हैं-'जीवाश्रयः' इत्यादिसे ।
__ * आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचितिरेव केवला । पूर्वसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाऽऽश्रयो भवति नाऽपि गोचरः ॥ (सं० शा० अ० १ श्लो० ३१९) निर्विभाग ( जीवेश्वरादि. विभागसे शून्य ) केवल ( शुद्ध ) चैतन्य ही अविद्याका आश्रय और विषय होता है; क्योंकि पूर्वसिद्ध तमका ( अविद्याका ) पश्चिम (पश्चाद्भावी जीव) आश्रय या विषय हो ही नहीं सकता, ऐसा संक्षेपशारीरककारका वचन इस अर्थमें प्रमाण है।
रत्नप्रभाकार रामानन्दने भी 'विकरणत्वान्नेति०' (ब्र० सू० २॥१॥३१) इस सूत्रकी व्याख्यामें 'शारीरस्य कल्पितस्याऽऽश्रयत्वायोगान्निर्विशेषचिन्मात्रस्यैव मायाधिष्ठानत्वं युक्तम्' अर्थात् मायाकल्पित जीव मायाका आश्रय नहीं हो सकता, इससे निर्विशेष चिन्मात्रको ही मायाका आश्रय मानना उचित है, ऐसा कहा है।
+ 'सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात' (ब्र. सू. १॥२॥१) इस अधिकरणमें 'स्मृतेश्च' (१।२६) इस सूत्रके भाष्यकी भामतीमें 'अनाद्यविद्यावच्छेदलब्धजीवभावः पर एवाऽऽत्मा स्वतो भेदेनाऽवभासते, तादृशां च जीवानामविद्या, न तु निरुपाधिनो ब्रह्मणः' अर्थात् अनादि अविद्यासे अवच्छिन्न होनेके कारण जिसे जीवभाव प्राप्त हुआ है, ऐसा परमात्मा ही स्वतः भेदसे भासता है; उन जीवोंकी ही अविद्या है; निरुपाधिक ब्रह्मकी नहीं, ऐसा कहा है और जीव तथा अविद्या दोनोंके अनादि होनेसे बोजाङ्करके समान कल्पित होनेके कारण अन्योन्याश्रय दोष भी नहीं होता, ऐसा परिहार भी किया है ।
Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat
www.umaragyanbhandar.com