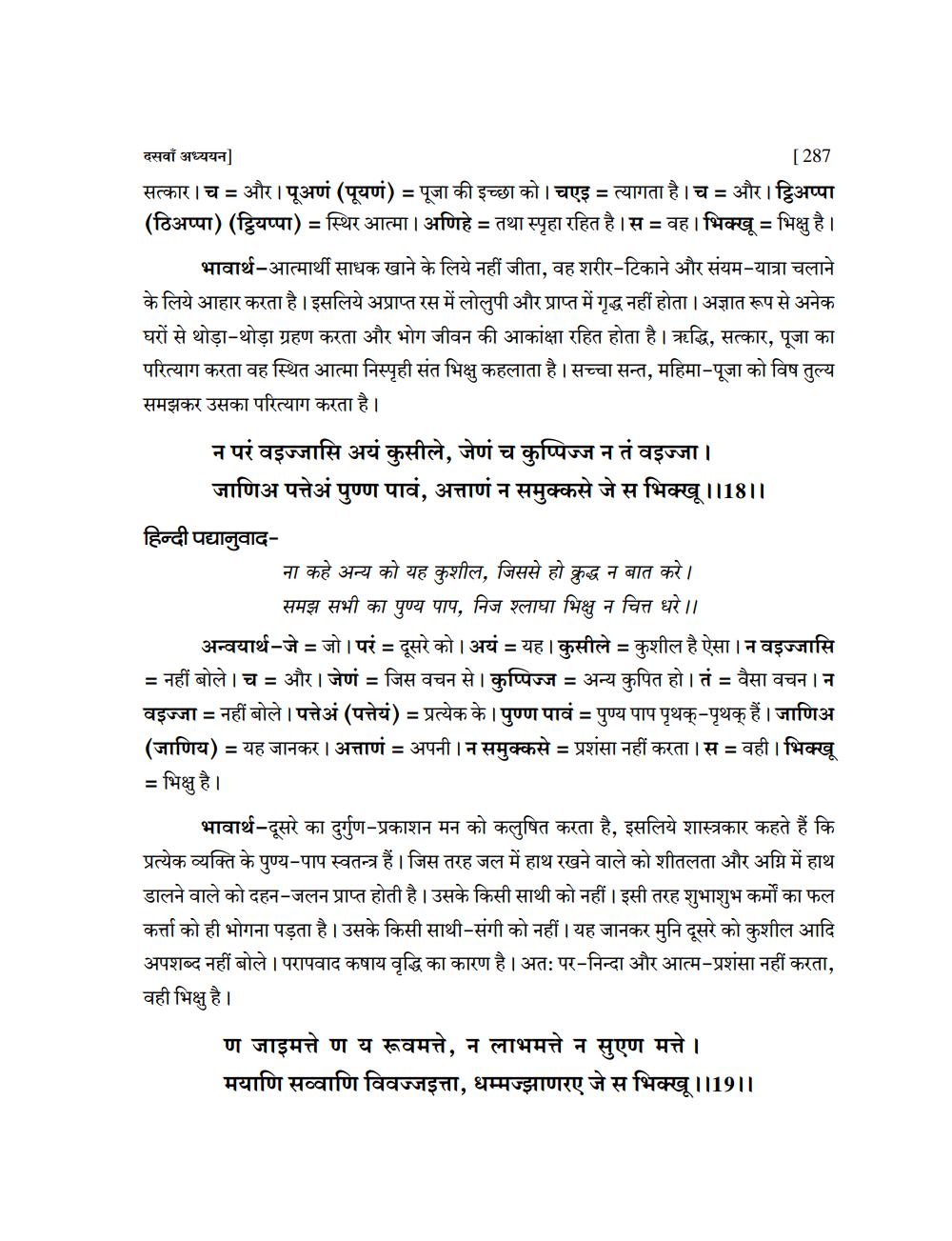________________
[287
दसवाँ अध्ययन] सत्कार । च = और । पूअणं (पूयणं) = पूजा की इच्छा को । चएइ = त्यागता है। च = और । ट्ठिअप्पा (ठिअप्पा) (ट्ठियप्पा) = स्थिर आत्मा। अणिहे = तथा स्पृहा रहित है। स = वह । भिक्खू = भिक्षु है।
भावार्थ-आत्मार्थी साधक खाने के लिये नहीं जीता, वह शरीर-टिकाने और संयम-यात्रा चलाने के लिये आहार करता है। इसलिये अप्राप्त रस में लोलुपी और प्राप्त में गृद्ध नहीं होता । अज्ञात रूप से अनेक घरों से थोड़ा-थोड़ा ग्रहण करता और भोग जीवन की आकांक्षा रहित होता है। ऋद्धि, सत्कार, पूजा का परित्याग करता वह स्थित आत्मा निस्पृही संत भिक्षु कहलाता है। सच्चा सन्त, महिमा-पूजा को विष तुल्य समझकर उसका परित्याग करता है।
न परं वइज्जासि अयं कुसीले, जेणं च कुप्पिज्ज न तं वइज्जा।
जाणिअ पत्तेअं पुण्ण पावं, अत्ताणं न समुक्कसे जे स भिक्खू॥18।। हिन्दी पद्यानुवाद
ना कहे अन्य को यह कुशील, जिससे हो क्रुद्ध न बात करे।
समझ सभी का पुण्य पाप, निज श्लाघा भिक्षु न चित्त धरे ।। अन्वयार्थ-जे = जो । परं = दूसरे को । अयं = यह । कुसीले = कुशील है ऐसा । न वइज्जासि = नहीं बोले । च = और । जेणं = जिस वचन से । कुप्पिज्ज = अन्य कुपित हो । तं = वैसा वचन । न वइज्जा = नहीं बोले । पत्तेअं (पत्तेयं) = प्रत्येक के । पुण्ण पावं = पुण्य पाप पृथक्-पृथक् हैं । जाणिअ (जाणिय) = यह जानकर । अत्ताणं = अपनी । न समुक्कसे = प्रशंसा नहीं करता । स = वही । भिक्खू = भिक्षु है।
भावार्थ-दूसरे का दुर्गुण-प्रकाशन मन को कलुषित करता है, इसलिये शास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप स्वतन्त्र हैं। जिस तरह जल में हाथ रखने वाले को शीतलता और अग्नि में हाथ डालने वाले को दहन-जलन प्राप्त होती है। उसके किसी साथी को नहीं। इसी तरह शुभाशुभ कर्मों का फल कर्ता को ही भोगना पड़ता है। उसके किसी साथी-संगी को नहीं । यह जानकर मुनि दूसरे को कुशील आदि अपशब्द नहीं बोले । परापवाद कषाय वृद्धि का कारण है। अत: पर-निन्दा और आत्म-प्रशंसा नहीं करता, वही भिक्षु है।
ण जाइमत्ते ण य रूवमत्ते, न लाभमत्ते न सुएण मत्ते । मयाणि सव्वाणि विवज्जइत्ता, धम्मज्झाणरए जे स भिक्खू।।1।।