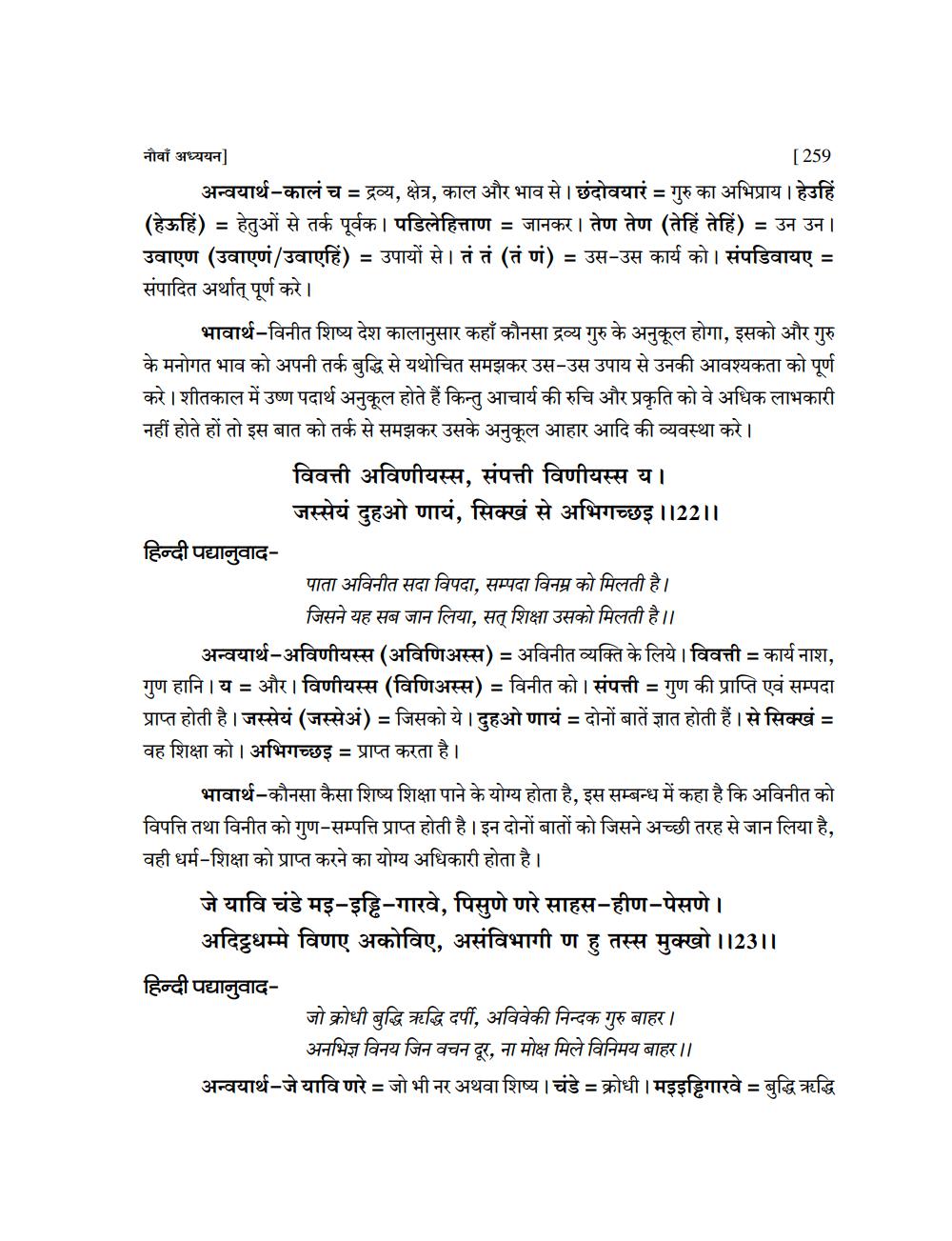________________
नौवाँ अध्ययन]
[259 अन्वयार्थ-कालं च = द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से । छंदोवयारं = गुरु का अभिप्राय । हेउहिं (हेऊहिं) = हेतुओं से तर्क पूर्वक । पडिलेहित्ताण = जानकर । तेण तेण (तेहिं तेहिं) = उन उन । उवाएण (उवाएणं/उवाएहिं) = उपायों से। तं तं (तं णं) = उस-उस कार्य को। संपडिवायए = संपादित अर्थात् पूर्ण करे।
भावार्थ-विनीत शिष्य देश कालानुसार कहाँ कौनसा द्रव्य गुरु के अनुकूल होगा, इसको और गुरु के मनोगत भाव को अपनी तर्क बुद्धि से यथोचित समझकर उस-उस उपाय से उनकी आवश्यकता को पूर्ण करे । शीतकाल में उष्ण पदार्थ अनुकूल होते हैं किन्तु आचार्य की रुचि और प्रकृति को वे अधिक लाभकारी नहीं होते हों तो इस बात को तर्क से समझकर उसके अनुकूल आहार आदि की व्यवस्था करे।
विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स य।
जस्सेयं दुहओ णायं, सिक्खं से अभिगच्छइ ।।22।। हिन्दी पद्यानुवाद
पाता अविनीत सदा विपदा, सम्पदा विनम्र को मिलती है।
जिसने यह सब जान लिया, सत् शिक्षा उसको मिलती है।। अन्वयार्थ-अविणीयस्स (अविणिअस्स) = अविनीत व्यक्ति के लिये। विवत्ती = कार्य नाश, गुण हानि । य = और । विणीयस्स (विणिअस्स) = विनीत को । संपत्ती = गुण की प्राप्ति एवं सम्पदा प्राप्त होती है । जस्सेयं (जस्सेअं) = जिसको ये । दुहओ णायं = दोनों बातें ज्ञात होती हैं । से सिक्खं = वह शिक्षा को । अभिगच्छइ = प्राप्त करता है।
भावार्थ-कौनसा कैसा शिष्य शिक्षा पाने के योग्य होता है, इस सम्बन्ध में कहा है कि अविनीत को विपत्ति तथा विनीत को गुण-सम्पत्ति प्राप्त होती है। इन दोनों बातों को जिसने अच्छी तरह से जान लिया है, वही धर्म-शिक्षा को प्राप्त करने का योग्य अधिकारी होता है।
जे यावि चंडे मइ-इडि-गारवे, पिसुणे णरे साहस-हीण-पेसणे।
अदिट्ठधम्मे विणए अकोविए, असंविभागी ण हु तस्स मुक्खो।।23।। हिन्दी पद्यानुवाद
जो क्रोधी बुद्धि ऋद्धि दपी, अविवेकी निन्दक गुरु बाहर।
अनभिज्ञ विनय जिन वचन दूर, ना मोक्ष मिले विनिमय बाहर।। अन्वयार्थ-जे याविणरे = जो भी नर अथवा शिष्य । चंडे = क्रोधी । मइइड्डिगारवे = बुद्धि ऋद्धि