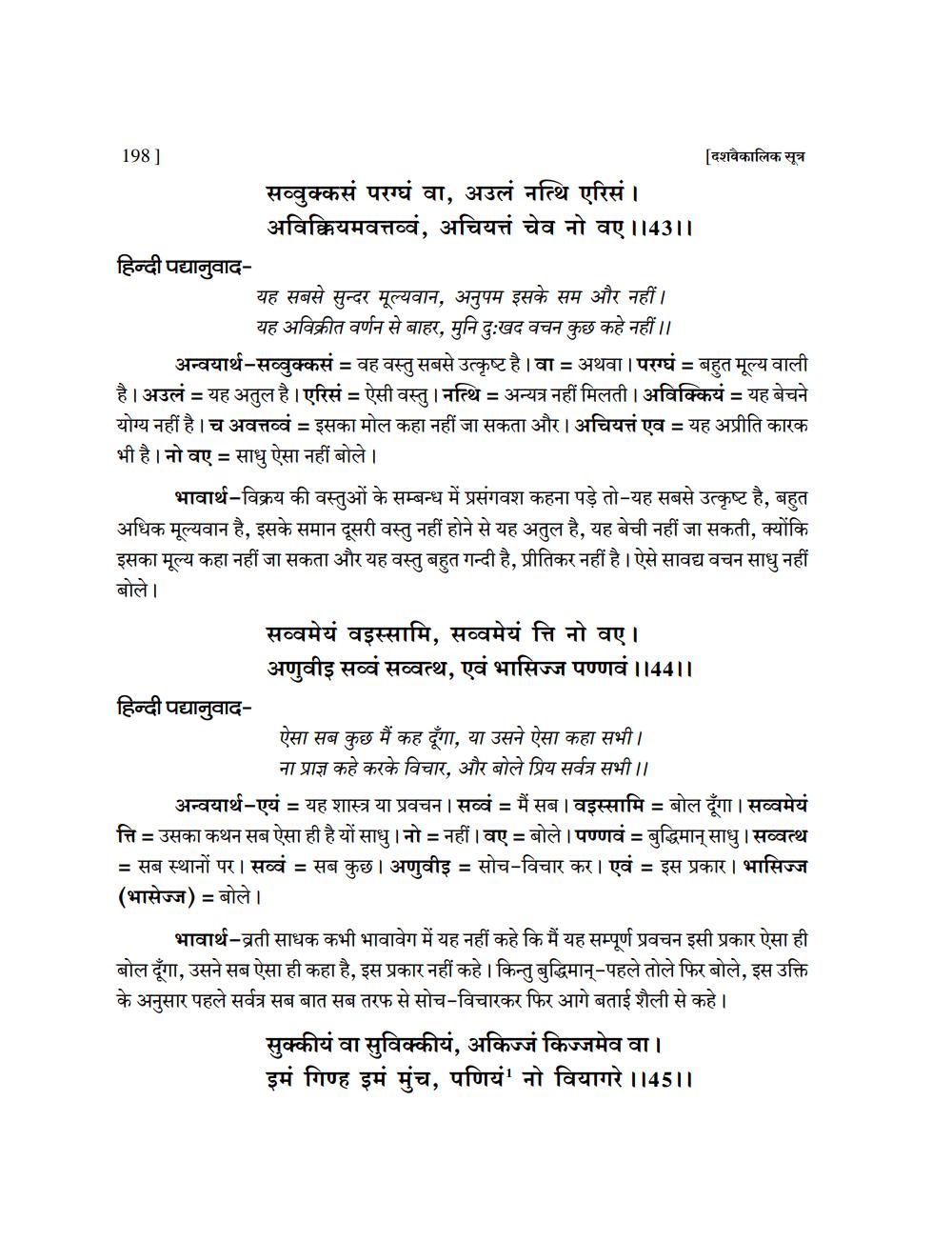________________
1981
[दशवैकालिक सूत्र सव्वुक्कसं परग्धं वा, अउलं नत्थि एरिसं।
अविक्कियमवत्तव्वं, अचियत्तं चेव नो वए।।43।। हिन्दी पद्यानुवाद
यह सबसे सुन्दर मूल्यवान, अनुपम इसके सम और नहीं।
यह अविक्रीत वर्णन से बाहर, मुनि दुःखद वचन कुछ कहे नहीं।। अन्वयार्थ-सव्वुक्कसं = वह वस्तु सबसे उत्कृष्ट है । वा = अथवा । परग्यं = बहुत मूल्य वाली है। अउलं = यह अतुल है। एरिसं = ऐसी वस्तु । नत्थि = अन्यत्र नहीं मिलती। अविक्कियं = यह बेचने योग्य नहीं है । च अवत्तव्वं = इसका मोल कहा नहीं जा सकता और । अचियत्तं एव = यह अप्रीति कारक भी है। नो वए = साधु ऐसा नहीं बोले।
भावार्थ-विक्रय की वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रसंगवश कहना पड़े तो-यह सबसे उत्कृष्ट है, बहुत अधिक मूल्यवान है, इसके समान दूसरी वस्तु नहीं होने से यह अतुल है, यह बेची नहीं जा सकती, क्योंकि इसका मूल्य कहा नहीं जा सकता और यह वस्तु बहुत गन्दी है, प्रीतिकर नहीं है। ऐसे सावध वचन साधु नहीं बोले।
सव्वमेयं वइस्सामि, सव्वमेयं त्ति नो वए।
अणुवीइ सव्वं सव्वत्थ, एवं भासिज्ज पण्णवं ।।44।। हिन्दी पद्यानुवाद
ऐसा सब कुछ मैं कह दूंगा, या उसने ऐसा कहा सभी।
ना प्राज्ञ कहे करके विचार, और बोले प्रिय सर्वत्र सभी।। अन्वयार्थ-एयं = यह शास्त्र या प्रवचन । सव्वं = मैं सब । वइस्सामि = बोल दूंगा । सव्वमेयं त्ति = उसका कथन सब ऐसा ही है यों साधु । नो = नहीं। वए = बोले । पण्णवं = बुद्धिमान् साधु । सव्वत्थ = सब स्थानों पर । सव्वं = सब कुछ। अणुवीइ = सोच-विचार कर । एवं = इस प्रकार । भासिज्ज (भासेज्ज) = बोले।
भावार्थ-व्रती साधक कभी भावावेग में यह नहीं कहे कि मैं यह सम्पूर्ण प्रवचन इसी प्रकार ऐसा ही बोल दूंगा, उसने सब ऐसा ही कहा है, इस प्रकार नहीं कहे । किन्तु बुद्धिमान्-पहले तोले फिर बोले, इस उक्ति के अनुसार पहले सर्वत्र सब बात सब तरफ से सोच-विचारकर फिर आगे बताई शैली से कहे।
सुक्कीयं वा सुविक्कीयं, अकिज्जं किज्जमेव वा। इमं गिण्ह इमं मुंच, पणियं नो वियागरे ।।45।।