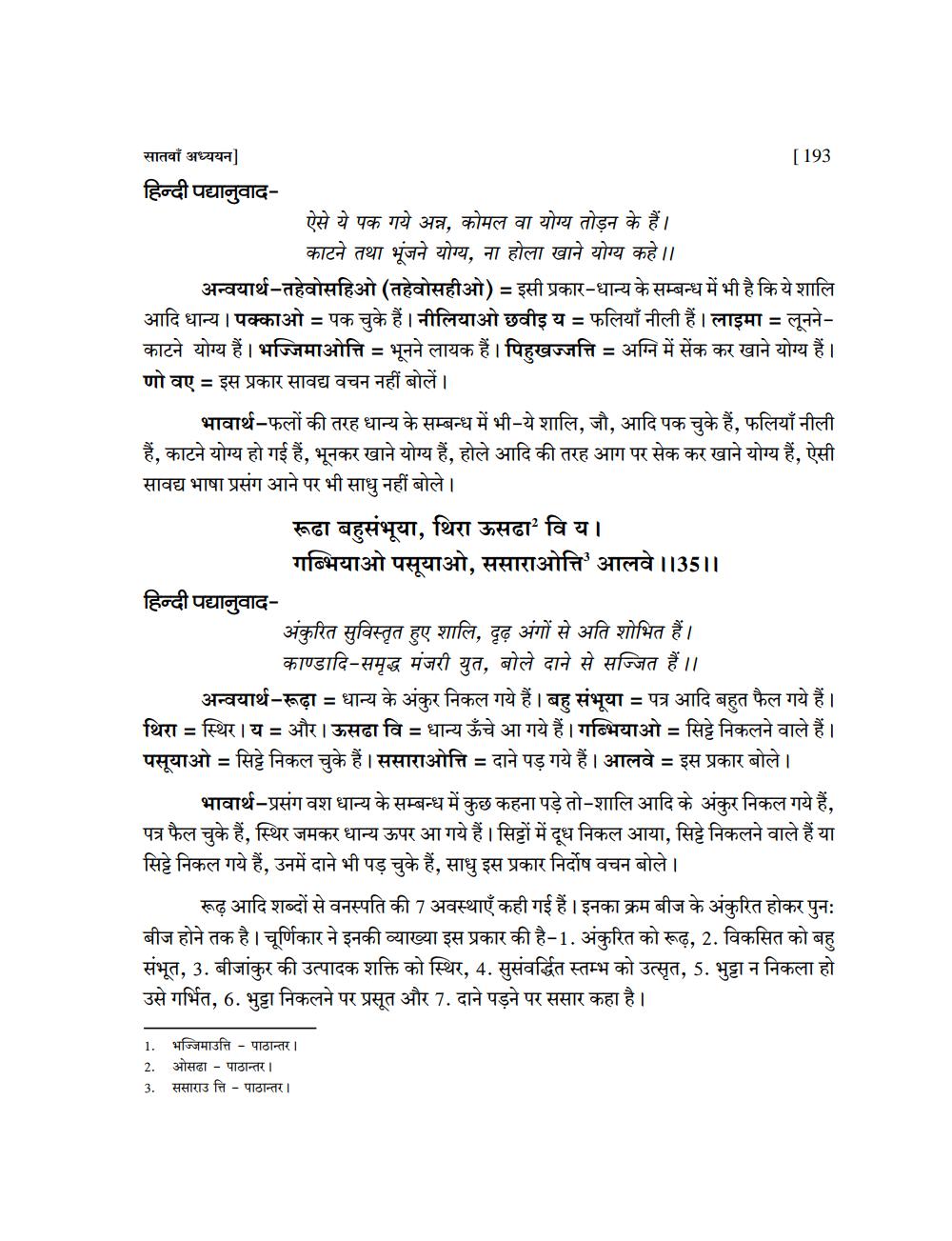________________
सातवाँ अध्ययन
[193 हिन्दी पद्यानुवाद
ऐसे ये पक गये अन्न, कोमल वा योग्य तोड़न के हैं।
काटने तथा मूंजने योग्य, ना होला खाने योग्य कहे ।। अन्वयार्थ-तहेवोसहिओ (तहेवोसहीओ) = इसी प्रकार-धान्य के सम्बन्ध में भी है कि ये शालि आदि धान्य । पक्काओ = पक चुके हैं। नीलियाओ छवीइ य = फलियाँ नीली हैं। लाइमा = लूननेकाटने योग्य हैं। भज्जिमाओत्ति = भूनने लायक हैं। पिहुखज्जत्ति = अग्नि में सेंक कर खाने योग्य हैं। णो वए = इस प्रकार सावद्य वचन नहीं बोलें।
भावार्थ-फलों की तरह धान्य के सम्बन्ध में भी-ये शालि, जौ, आदि पक चुके हैं, फलियाँ नीली हैं, काटने योग्य हो गई हैं, भूनकर खाने योग्य हैं, होले आदि की तरह आग पर सेक कर खाने योग्य हैं, ऐसी सावध भाषा प्रसंग आने पर भी साधु नहीं बोले।
रूढा बहुसंभूया, थिरा ऊसढा वि य ।
गब्भियाओ पसूयाओ, ससाराओत्ति' आलवे ।।35।। हिन्दी पद्यानुवाद
अंकुरित सुविस्तृत हुए शालि, दृढ़ अंगों से अति शोभित हैं।
काण्डादि-समृद्ध मंजरी युत, बोले दाने से सज्जित हैं ।। अन्वयार्थ-रूढ़ा = धान्य के अंकुर निकल गये हैं। बहु संभूया = पत्र आदि बहुत फैल गये हैं। थिरा = स्थिर । य = और । ऊसढा वि = धान्य ऊँचे आ गये हैं। गब्भियाओ = सिट्टे निकलने वाले हैं। पसूयाओ = सिट्टे निकल चुके हैं। ससाराओत्ति = दाने पड़ गये हैं। आलवे = इस प्रकार बोले।
भावार्थ-प्रसंग वश धान्य के सम्बन्ध में कुछ कहना पड़े तो-शालि आदि के अंकुर निकल गये हैं, पत्र फैल चुके हैं, स्थिर जमकर धान्य ऊपर आ गये हैं। सिट्टों में दूध निकल आया, सिट्टे निकलने वाले हैं या सिट्टे निकल गये हैं, उनमें दाने भी पड़ चुके हैं, साधु इस प्रकार निर्दोष वचन बोले।
रूढ़ आदि शब्दों से वनस्पति की 7 अवस्थाएँ कही गई हैं। इनका क्रम बीज के अंकुरित होकर पुनः बीज होने तक है। चूर्णिकार ने इनकी व्याख्या इस प्रकार की है-1. अंकुरित को रूढ़, 2. विकसित को बहु संभूत, 3. बीजांकुर की उत्पादक शक्ति को स्थिर, 4. सुसंवर्द्धित स्तम्भ को उत्सृत, 5. भुट्टा न निकला हो उसे गर्भित, 6. भुट्टा निकलने पर प्रसूत और 7. दाने पड़ने पर ससार कहा है।
1. भज्जिमाउत्ति - पाठान्तर । 2. ओसढा - पाठान्तर । 3. ससाराउ त्ति - पाठान्तर।