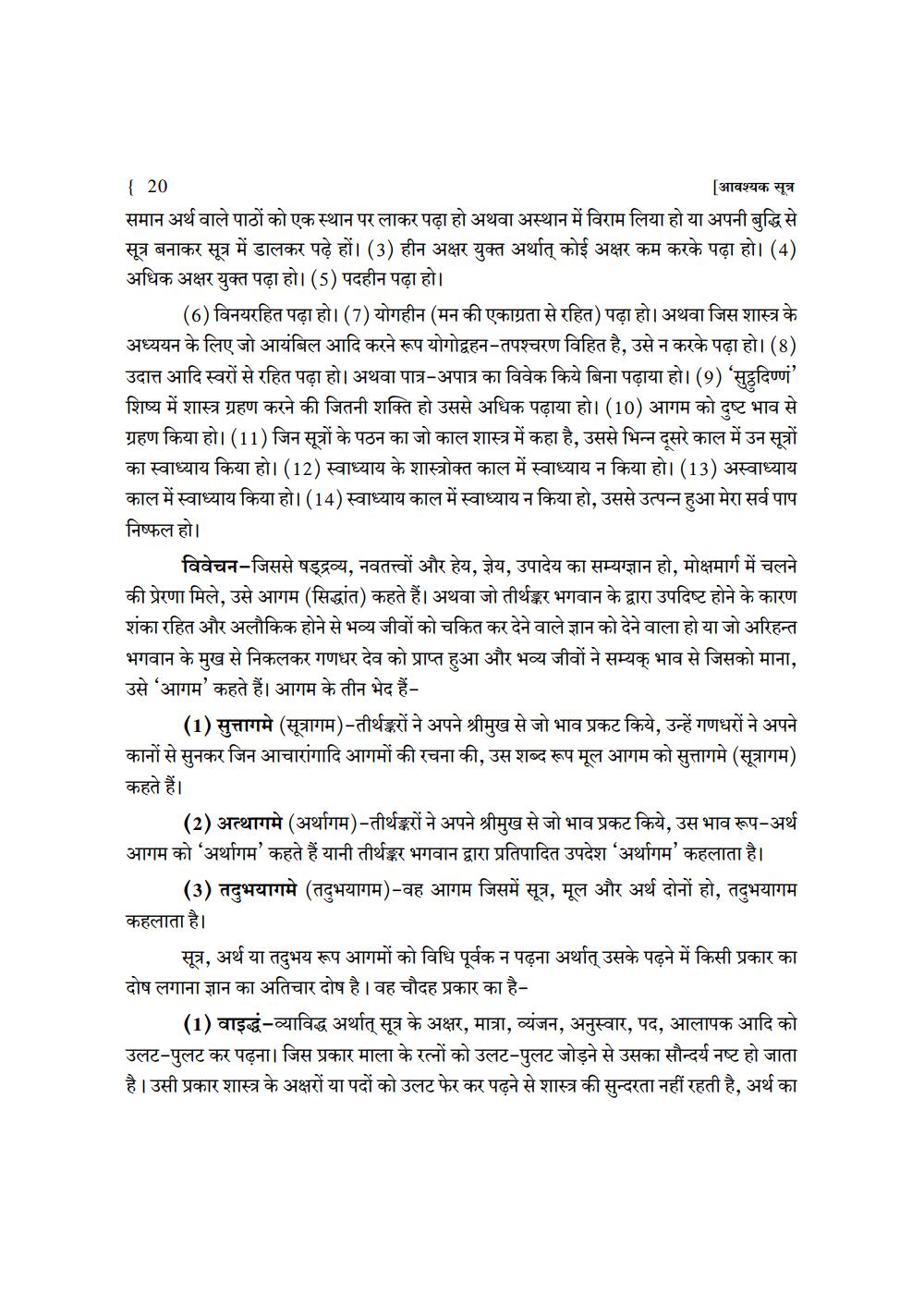________________
{ 20
[आवश्यक सूत्र समान अर्थ वाले पाठों को एक स्थान पर लाकर पढ़ा हो अथवा अस्थान में विराम लिया हो या अपनी बुद्धि से सूत्र बनाकर सूत्र में डालकर पढ़े हों। (3) हीन अक्षर युक्त अर्थात् कोई अक्षर कम करके पढ़ा हो। (4) अधिक अक्षर युक्त पढ़ा हो। (5) पदहीन पढ़ा हो।
(6) विनयरहित पढ़ा हो। (7) योगहीन (मन की एकाग्रता से रहित) पढ़ा हो। अथवा जिस शास्त्र के अध्ययन के लिए जो आयंबिल आदि करने रूप योगोद्वहन-तपश्चरण विहित है, उसे न करके पढ़ा हो। (8) उदात्त आदि स्वरों से रहित पढ़ा हो। अथवा पात्र-अपात्र का विवेक किये बिना पढ़ाया हो। (9) 'सुट्टदिण्णं' शिष्य में शास्त्र ग्रहण करने की जितनी शक्ति हो उससे अधिक पढ़ाया हो। (10) आगम को दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो। (11) जिन सूत्रों के पठन का जो काल शास्त्र में कहा है, उससे भिन्न दूसरे काल में उन सूत्रों का स्वाध्याय किया हो। (12) स्वाध्याय के शास्त्रोक्त काल में स्वाध्याय न किया हो। (13) अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय किया हो। (14) स्वाध्याय काल में स्वाध्याय न किया हो, उससे उत्पन्न हुआ मेरा सर्व पाप निष्फल हो।
विवेचन-जिससे षड्द्रव्य, नवतत्त्वों और हेय, ज्ञेय, उपादेय का सम्यग्ज्ञान हो, मोक्षमार्ग में चलने की प्रेरणा मिले, उसे आगम (सिद्धांत) कहते हैं। अथवा जो तीर्थङ्कर भगवान के द्वारा उपदिष्ट होने के कारण शंका रहित और अलौकिक होने से भव्य जीवों को चकित कर देने वाले ज्ञान को देने वाला हो या जो अरिहन्त भगवान के मुख से निकलकर गणधर देव को प्राप्त हुआ और भव्य जीवों ने सम्यक् भाव से जिसको माना, उसे आगम' कहते हैं। आगम के तीन भेद हैं
(1) सुत्तागमे (सूत्रागम)-तीर्थङ्करों ने अपने श्रीमुख से जो भाव प्रकट किये, उन्हें गणधरों ने अपने कानों से सुनकर जिन आचारांगादि आगमों की रचना की, उस शब्द रूप मूल आगम को सुत्तागमे (सूत्रागम) कहते हैं।
(2) अत्थागमे (अर्थागम)-तीर्थङ्करों ने अपने श्रीमुख से जो भाव प्रकट किये, उस भाव रूप-अर्थ आगम को ‘अर्थागम' कहते हैं यानी तीर्थङ्कर भगवान द्वारा प्रतिपादित उपदेश ‘अर्थागम' कहलाता है।
(3) तदुभयागमे (तदुभयागम)-वह आगम जिसमें सूत्र, मूल और अर्थ दोनों हो, तदुभयागम कहलाता है।
सूत्र, अर्थ या तदुभय रूप आगमों को विधि पूर्वक न पढ़ना अर्थात् उसके पढ़ने में किसी प्रकार का दोष लगाना ज्ञान का अतिचार दोष है । वह चौदह प्रकार का है
(1) वाइद्धं-व्याविद्ध अर्थात् सूत्र के अक्षर, मात्रा, व्यंजन, अनुस्वार, पद, आलापक आदि को उलट-पुलट कर पढ़ना। जिस प्रकार माला के रत्नों को उलट-पुलट जोड़ने से उसका सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार शास्त्र के अक्षरों या पदों को उलट फेर कर पढ़ने से शास्त्र की सुन्दरता नहीं रहती है, अर्थका